B.Com 1st Year Business Communication Hindi Long Notes
B.Com 1st Year Business Communication Hindi Long Notes :- hii friends this site is a very useful for all the student B.Com, M.com. B.Sc. M.A, BA Here you will find All the Question With Answer Study Material Notes Question Sample Model Practice Papers Mock test Paper All the content Unit wise chapter wise available .
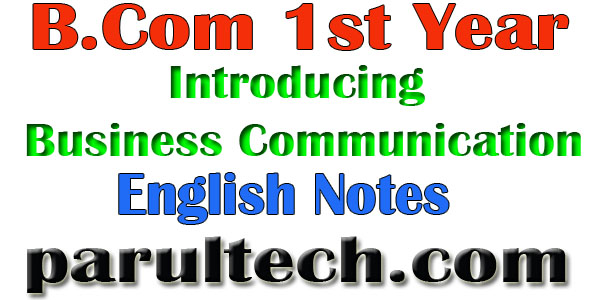
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न – व्यावसायिक सम्प्रेषण से आप क्या समझत हा सम्प्रेषण के सिन्हा
What do you mean by Business Communication? Discuss the theories of communication.
अथवा व्यावसायिक सम्प्रेषणा सै व्या आशय है। सम्प्रेषण की प्रकृति एवं प्रमुख तत्त द्वार बताइए। इसके महत्व व उद्देश्यों को समझाइए।
What do you mean by Business Communication ? Discuss natur and main elements of communication. Explain its importance ani objectives.
अथवा व्यावसायिक सम्प्रेषण को परिभाषित कीजिए एवं प्रबन्धकों के लिए इसके महत्त्व – की विवेचना कीजिए।
Define Business Communication and discuss its importance for for managers,
सम्प्रेषण सिद्धान्त
(Communication Theory)
सन्देश के माध्यम से सम्प्रेषण मनुष्यों को एक-दूसरे से जोड़ता है। सम्प्रेषण को किसी सीम मैं बाँधना प्रायः असम्भव ही है, बल्कि इसे कुछ मापदण्डों के आधार पर पूरा किया जाता है।
सहित में सम्प्रेषण को जिन मान्यताओं, सीमाओं व परिवेश में सम्पन्न किया जाता है उनै सम्प्रेषण सिद्धान्त कहते हैं, अर्थात् सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में आदर्श मूल्यों उक्षा व स्थापना हेतु सार्वभौमिक समुदाय के लिए निर्धारित सीमा में किया गया सम्प्रेषण सम्प्रेषण सिद्धान्त है।
सम्प्रेषण के सिद्धान्त
(Theories of Communication)
विश्व में सम्प्रेषण के निम्नलिखित सात सिद्धान्त हैं
वैद्रिक सम्प्रेषण सिद्धान्त (Vedic Theory of Communication)
कढ़िवादी सम्प्रेषण सिद्धान्त (Conservative Theory of Communications
इस्लामिक सम्प्रेषण सिद्धान्त (Islamie Theory of Communication)
साम्यवादी सम्प्रेषण सिद्धान्त (Communist Theory of Communication)
चीनी सम्प्रेषण सिद्धान्त (Chinese Theory of Communication)
उदारवादी सम्प्रेषण सिद्धान्त (Liberal Theory of Communication)
मसीही सम्प्रेषण सिद्धान्त (Christian Theory of Communication)
व्यावसायिक सम्प्रेषण व्यावसायिक सम्प्रेषण का आशय एवं परिभाषा
(Meaning and Definitions of Business Communication)
जन्म के साथ ही मनुष्य की सम्प्रेषण या संचार क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में ‘सम्प्रेषण’ से आशय उस वार्तालाप से है, जो किन्हीं दो प्राणियों के मध्य किसी विशिष्ट बिन्दु, सूचना या जानकारी के लिए होता है। किसी भी भाषा का अन्तिम लक्ष्य सम्प्रेषण ही होता है। ‘सम्प्रेषण’ का अंग्रेजी समानार्थी शब्द Communication’ है। यह लैटिन शब्द communico’ से बना है जिसका अर्थ होता है-‘आपस में बाँटना’ या ‘किसी वस्तु के सम्पूर्ण नियोजन में हिस्सा बाँटना’।
विश्व में निरन्तर प्रगतिशील आधुनिक व्यावसायिक परिवेश में सम्प्रेषण को कुछ विद्वानों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है-
कीथ डेविस के अनुसार, “सम्प्रेषण एक से दूसरे व्यक्ति के बीच सूचना प्रदान करने व 1 समझने की प्रक्रिया है।”
जॉर्ज आर० टेरी के अनुसार, “सम्प्रेषण के अन्तर्गत एक या उससे अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का आदान-प्रदान होता है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, or जिसमें सम्प्रेषक और संग्राहक के बीच सामंजस्य स्थापित हो, उनमें जागरूकता उत्पन्न हो।
सम्प्रेषण एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा जनता के ज्ञान, विचार और अभिवृत्ति का । निर्माण किया जाता है या उन्हें परिवर्तित किया जाता है।
सम्प्रेषण की प्रकृति
(Nature of Communication)
सम्प्रेषण की प्रकृति के नाना रूप दृष्टिगत होते हैं। इनको प्रमुख बिन्दुओं के रूप में अग्रवत् उद्घाटित किया जा सकता है
1. उचित माध्यम का चयन (Selection of Proper Media)-सम्प्रेषण के लिए किसी माध्यम का होना अत्यन्त आवश्यक है। सम्बन्धित सन्देश हेतु प्रयुक्त उचित माध्यम, सन्देश की विषय-वस्तु से भी मेल खा जाता है। सन्देश के प्रसारण के लिए उचित माध्यम हो, जिससे सन्देश को स्पष्ट रूप से सम्प्रेषित किया जा सके।
2. तथ्यों व अनुभवों से सम्बद्ध (Related to Facts and Experience)सम्प्रेषण की प्रकृति तथ्यपरक तथा अनुभवों के हस्तान्तरण के रूप में होती है। निश्चित तथ्यों का सम्प्रेषण किया जाता है।
3 . सतत प्रक्रिया (Regular Process)-सम्प्रेषण की क्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात् सतत रूप से तब तक चलती रहती है जब तक कि सम्बन्धित विषय पूर्ण न हो जाए। उसकी an) बारम्बारता में विघ्न उत्पन्न नहीं होता है, अन्यथा सम्प्रेषण का उद्देश्य खण्डित हो जाएगा।4. कला का विकसित रूप (Developed form of Art)-सम्प्रेषण द्वारा कार्य को सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जो कला का मूल तत्त्व है। कला व विज्ञान दोनों के सही मिश्रण से ही सम्प्रेषण को प्रभावशाली बनाया जाता है।
जन्मजात प्रकति (Nature by Birth)-सम्प्रेषण एक जन्मजात प्रकति है। सम्प्रेषण के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से भिन्न लेकिन श्रेष्ठ है। सम्प्रेषण उसका तथा प्राकृतिक गुण है।
सम्प्रेषण के प्रमुख तत्त्व
(Main Elements of Communication)
सम्प्रेषण के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं-
(1) सम्प्रेषण मानवीय विचारों एवं तथ्यों के कारण विस्तृत क्षेत्र वाला होता है।
(2) सम्प्रेषण का अस्तित्व उसके प्रवाह, क्रम एवं अनुक्रम की श्रृंखला पर निर्भर करता है। सम्प्रेषण प्रक्रिया के अन्तर्गत विचारों को जन्म से लेकर उन्हें उचित माध्यम द्वारा उचित व्यक्ति तक पहुँचाने की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है ताकि सूचनाग्राही इस प्राप्त सूचना का अनुकूल एवं प्रभावी प्रयोग कर सके।
(3) सम्प्रेषण के अन्तर्गत सूचनाओं का संचरण एवं बोधगम्यता होती है। इसका अभिप्राय है कि प्रभावी सम्प्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है।
(4) सम्प्रेषण में तीन आन्तरिक परिपथ-आरोही, अवरोही व पाश्वीय होते हैं, जिनमें आपस में अन्तर्सम्बद्धता व क्रॉस होते हैं।
(5) सम्प्रेषण का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विचारों एवं सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना होता है, चाहे वह मौखिक रूप से है या लिखित रूप से, चित्र द्वारा अथवा शारीरिक यात्रा द्वारा पहुँचाया जाए।
सम्प्रेषण के उद्देश्य
(Objectives of Communication)
सही व्यक्ति को सही तरीके से, सही जगह पर, सही सूचना पहँचाना ही सम्प्रेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है। संक्षेप में सम्प्रेषण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं
1, कार्यों में समन्वय (Coordination in Works)-सम्प्रेषण का प्रमुख उद्देश्य । संवेगों को निश्चित व्यक्ति तक सही रूप में पहुँचाना होता है। इसमें सूचना, आदेश, तथ्य, संलाह आदि को प्रेषित किया जाता है। इसके लिए समस्त कार्य-कलापों में समन्वय होना आवश्यक होता है।
2.जातिया का क्रियान्वयन (Application of Policies)-क्रियान्वयन की नीतिया का को इस प्रकार से गठित किया जाता है कि सम्प्रेषण के उद्देश्य का क्षय न हो पाए। शीघ्र निणय लेने के लिए समंकों का संकलन आवश्यक क्रिया है। अत: सम्बन्धित सूचनाओं का पाच संकलन किया जाता है।
3. प्रबन्धन कौशल में वृद्धि (Increase in Management Skill)-सम्प्रेषण का मुख्य उद्देश्य मानव-व्यवहार को सही समय पर सही रूप में समझना भी है। सम्प्रेषण क सीखने की क्रिया पूर्णत्व को प्राप्त करती है।
4. सही सूचनाओं का प्रेषण (Communication of Correct Infornation)सही सूचना का प्रेषण करना ही सम्प्रेषण का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। उचित व्यक्ति तक समुचित सन्देश पहुँचाना इसका परम लक्ष्य है। यदि सम्प्रेषण की सामग्री प्राप्तकत्ता तक उचित रूप में नहीं पहुँच पाती है तो सम्प्रेषण का मूल उद्देश्य ही खण्डित हो जाएगा। अधिकारियों व कर्मचारियों के मध्य सुझावों का आदान-प्रदान सम्प्रेषण के द्वारा निश्चयात्मकता को प्राप्त करता है और लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ता जाता है।
सम्प्रेषण का महत्त्व
(Importance of Communication)
वर्तमान समय में व्यावसायिक क्षेत्र में सम्प्रेषण का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। उपयोगिता के साथ-साथ इसके महत्त्व में भी आशातीत वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाना एक अनिवार्यता बन चुकी है। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति अपनी हर प्रकार की भावनाओं तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है। संगठनों के लगातार बढ़ते आकार के कारण वर्तमान समय में सम्प्रेषण का महत्त्व नित्यप्रति बढ़ता जा रहा है। सम्प्रेषण की कला में जो व्यक्ति दक्षता प्राप्त कर लेता है, वह विभिन्न क्षेत्रों में लाभदायक स्थिति को प्राप्त होता है।
-मानव की विकास यात्रा के साथ-साथ सम्प्रेषण का स्वरूप व आकार भी बदलता गया है और आज इसका अत्यन्त परिष्कृत रूप हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। वास्तव में, व्यक्ति की आवश्यकताओं ने ही सम्प्रेषण की माँग को जन्म दिया है। प्राचीन सूचना-सम्प्रेषण के माध्यमों-लकड़ी व पत्तों के प्रयोग से लेकर भाषा, लिपि, प्रिण्टिग प्रेस, रेडियो, फिल्म, दूरभाष, टेलीविजन, सेटेलाइट या उपग्रह एवं मोबाइल की यात्रा आदि मनुष्य की सम्प्रेषण से सम्बन्धित असीमित आवश्यकताओं का ही परिणाम है, जिसमें जिजीविषा के उत्कर्ष का भी प्रकटन होता है।
सम्प्रेषण के तौर-तरीकों के अच्छे या बुरे होने का व्यक्ति की व्यावसायिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सम्प्रेषण की क्रिया ही किसी व्यक्ति को उच्च आयामों का स्पर्श करा सकती है तथा यही व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अवनति की ओर भी धकेल सकती है।
निम्नलिखित तथ्यों से सम्प्रेषण के महत्त्व का यथेष्ट ज्ञान हो जाता है-
1. क्रियाशीलता एवं समन्वय-क्षमता का विकास (Development of Effectiveness and Coordination Skill)-सम्प्रेषण के बिना एकता व क्रियाशीलता का आना असम्भव है। सम्प्रेषण व्यक्तियों में सहयोग व समन्वय-क्षमता का विकास करता है। आपस में सूचनाओं व विचारों का आदान-प्रदान व्यक्तियों की एकता व क्रियाशीलता को बढ़ाता है।
2 .जेतृत्व गण के विकास हेतु आवश्यक (Necessary for Leadership Qualities)-सम्प्रेषण-कुशलता नेतृत्व शक्ति की पूर्व अनिवार्य शर्त है। यह प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। सम्प्रेषण में दक्ष एक प्रबन्धक अपने कर्मचारियों का वास्तविक नेता होता है। एक अच्छे सम्प्रेषण निकाय में व्यक्ति एक-दूसरे के निकट आते हैं और उनके आपसी विरोधाभास दूर हो जाते हैं।
3. प्रबन्धन-क्षमता बढ़ाने में सहायक (Helpfudio increasing Management Skill) -समुचित प्रबन्धन के लिए त्वरित सम्रोषण तथा व्यक्तिगत निष्पादन अनिवादा है। क्योंकि सम्प्रेषण के द्वारा ही प्रबन्धक आपने लक्ष्यों, उद्देश्यों व दिशा-निर्देशा तथा राजापार जर उत्तरदायित्वों के निर्वहन की व्यावस्था के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के व्यवहार का निरीक्षण – व मूल्यांकन करता है। अतः आज साम्प्रेषण प्रबन्धान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4 जनसम्पर्क में साहायक (Helpful in Public-relation)-साज प्रत्यक व्यावसायिक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज में अपना स्थान बनाए इसके लिए जनसम्पर्क एक आवश्यक शर्त है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सत्रोषणा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
5. योजना-निर्माण में सहायक (Helpful in Planning) सम्प्रेषण सदैव संगठन की योजना के निर्माण व क्रियाशीलता में सहायक होता है। किसी योजना को क्रियाशील करने तथा योजना के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने में सभीषणा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सम्प्रेषण का प्रबन्धकों के लिए महत्त्व
(Importance of Communication for Managers)
आज व्यावसायिक पर्यावरण बदल चुका है। प्रबन्धन की अवधारणा भी बदलाती जा – रही है, इसमें नित नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। चूंकि सम्प्रेषण में किसी व्यक्ति वा समूह के प्रति विचारों एवं भावनाओं को अन्य व्यक्तियों या समूहों में पहुंचाने की क्षमता होती है. आर. प्रबन्धक के लिए यह अनिवार्य है कि वह समय पर उचित सूचनाओं (जैसे-नए उत्पाद केबाजार में आने से पूर्व वर्तमान बाजार व आवश्यक पूंजी की जानकारी को मनाहीत को तथा अपने उद्देश्यों में सफल हो। एक प्रबन्धक के लिए वह भी आवश्यक है कि वह नियन्त्रण द्वारा अपने व्यवसाय को भली-भांति संचालित करे। उत्पादन लक्ष्यों को प्राथमिकता के आप पर निचले व्यावसायिक खण्डों में सम्प्राषित किया जाए और उनके परिणामों की प्रवकतन पहुंचाया जाए। एक अच्छे प्रबन्धक का गुण होता है कि वह सम्प्रेषण के माध्यम सेबाचन अधिकाधिक जनसम्पर्क बनाए क्योंकि उचित जनसम्पर्क एक उपक्रम के तर आवश्यक है। वास्तव में, एक प्रबन्धक द्वारा समस्त प्रबन्धकीय कार्य सम्प्रेषण के नाम सम्पन्न किए जाते हैं।
प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्यरत प्रबन्धक की निम्नलिखित पाँच मुख्य क्रिया हो सकती हैं-
(1) प्रोत्साहन व सम्प्रेषण करना।
(2) संगठित करना।
(3) कार्य की माप
(4) विदिश्य को प्राप्त करना।
(5) व्यक्ति का विकासा
उपर्यवत पाँचौ क्रियाएँ प्रत्येक प्रबन्धक द्वारा सम्पन्न की जाती हैं। इन क्रियाओं को सम्पन्न करने में सम्प्रेषण एक मुख्य भूमिका निभाता है। अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रबन्धक जो भी बोलता है, लिखता है, अर्थात् वह जो भी सूचना या सन्देश देता है, वह केवल सम्प्रेषण क्रिया पर ही निर्भर करता है। उसकी सफलता का पैमाना उसके द्वारा सम्प्रेषित वार्तालाप में ही निहित होता है। एक प्रबन्धक के पढ़ने, लिखने, सोचने की दक्षता उसे एक प्रभावी प्रबन्धक के रूप में स्थापित करती है। सम्प्रेषण जितना सुनियोजित ढंग से तथा कुशलता के साथ किया जाएगा, प्रबन्धक की उपलब्धि उतनी ही अधिक विकसित व मुखरित होती जाएगी।
प्रश्न – प्रभावी सम्प्रेषण के सिद्धान्तों को समझाइए।
Describe the principles of effective communication.
अथवा “एक प्रभावपूर्ण संचार में संक्षिप्तता तथा पूर्णता जितनी महत्त्वपूर्ण है उतनी ही महत्त्वपूर्ण शिष्टता एवं स्पष्टता है।” व्याख्या कीजिए।
“In an effective communication, coneiseness and completeness are as important as courtesy and clarity” Discuss.
उत्तर-सम्प्रेषण प्रक्रिया में, सन्देश सदैव स्पष्ट होना चाहिए ताकि प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता को आपसी समझ तथा वांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त हो सके। सम्प्रेषण की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि सूचना का सामान्य शब्दों एवं प्रभावी वाक्यों में आदान-प्रदान किया जाए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सम्प्रेषण के कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार, सम्प्रेषण के सिद्धान्तों से आशय उन मार्गदर्शक नियमों से है, जिनके पालन करने पर सम्प्रेषण प्रक्रिया अपने निहित उद्देश्यों को प्राप्त कर लेती है।
प्रभावी सम्प्रेषण के मुख्य सिद्धान्त
(Main Principles of Effective Communication)
व्यावसायिक सूचनाओं एवं सन्देशों के आदान-प्रदान में जिन महत्त्वपूर्ण नियमों या सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, वे निम्नवत् हैं
1. स्पष्टता (Clarity)-प्रभावशाली सम्प्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि सन्देश एवं उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, जिससे सम्बन्धित व्यक्ति सन्देश को उसी रूप व अर्थ में समझ, जिस रूप व अर्थ में सन्देश को प्रसारित किया गया है। स्पष्टता के अन्तर्गत सम्प्रेषण व्यवस्था में निम्नलिखित बाते आवश्यक होती हैं
(i) अभिव्यक्ति की स्पष्टता – सन्देशग्राही को यह स्पष्ट होना चाहिए कि सन्देश-प्रेषक पाकिम प्रकार सन्देश लिया जाए। सेना में ‘कोड’ शब्द प्रचलित हैं, अत: दोनों पक्षों के मध्य कोड पष्ट हान चाहिए। शब्दों के चयन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए
(a) निश्चित एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए।
(b) सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
(c) निवारक रूपों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
(ii) विचारों की स्पष्टता – सन्देश देने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में जैसे ही विन आता है तभी सन्देशकर्ता को स्वयं सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
(a) सम्प्रेषण की सामग्री क्या है,
(b) सम्प्रेषण का उद्देश्य क्या है,
(c) सम्प्रेषण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संचार का कौन-सा माध्यम उपयुक्त होगा।
(iii) अपरिमित रूप का प्रयोग न करना – अपरिमित रूप का प्रयोग सन्देश के औपचारिक बना देता है; जैसे
कैशियर का कर्त्तव्य है कि वेतन का भुगतान करे।
कैशियर वेतन का भुगतान करता है।
(iv) सन्देहात्मक शब्दों का प्रयोग न करना – यदि किसी सन्देश का अर्थ स्पष्ट नहीं व्य है तो सन्देश का प्रयोग करना उचित न होगा; जैसे
“गाड़ी रोको मत जाने दो” इसके दो अर्थ निकलते हैं
(a) गाड़ी रोको, मत जाने दो।
अथवा
(b) गाड़ी रोको मत, जाने दो।
(v) निरर्थक शब्दों का प्रयोग न करना – निरर्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट न होने के ध्या कारण इनका प्रयोग उचित नहीं है; जैसे
We beg to, this is to acknowledge, at all time, at the presest time. जात
2. पूर्णता (Completeness)-यह सम्प्रेषण का दूसरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है व्यावसायिक सम्प्रेषण सदैव अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पूर्णता में निम्नलिखित बातों प भाषा ध्यान देना आवश्यक है
(i) सन्देश भेजने का कारण क्या है,
(ii) सन्देश क्या है,
(iii) सन्देश किसको भेजा जा रहा है,
(iv) सन्देश किस स्थान पर भेजा जा रहा है,
(v) सन्देश कब तक पहुँचना है और कब भेजा गया।
3. संक्षिप्तता (Conciseness)-सन्देश में निरर्थक एवं अनावश्यक शब्दों का प्रया उपमह न किया जाए। इससे सन्देश प्रेषक व सन्देशग्राही दोनों का समय बचता है। प्रेषक का यह प्रया महान होना चाहिए कि सन्देश छोटा हो और उसमें सभी बातों का समावेश हो. अर्थात् सन्देश कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक बातों का समावेश हो; जैसे-
प्रश्न – सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता से किस प्रकार प्रभावित होती है? उदाहरण सहित समझाइए।
How is eultural consciousness influenced by cultural diversity Explain it with examples.
अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संवाद हेतु आवश्यक अन्तसांस्कृतिक बातों को स्पष्ट कीजिए।
Explain intercultural factors necessary for international communication.
उत्तर – सांस्कृतिक विविधता समाज को एक स्वाभाविक स्थिति है। प्रत्येक राष्ट्र को एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। जब विभिन्न सांस्कृतियाँ एक-दूसरे के निकट आती हैं तो स्वाभाविक रूप से वे एक-दूसरे को प्रभावित करती है। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो जाती है। विभिन्न अनुसन्धानों से यह विदित हुआ है कि संस्कृति को अनेक परिभाषाएँ हैं, परन् अध्ययन के दृष्टिकोण से संस्कृति को कम से कम 6 वर्ग या श्रेणियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ हमारा अभिप्राय संस्कृति के व्यावहारिक लक्षणों से है। व्यावहारिक लक्षण से आशय है-एक समूह में सप्रेम को यौगिक या अशाब्दिक प्रकृति, जो अपने आप में विशिष्ट एवं अद्वितीय है। संस्कृति से अभिप्राय किसी समाज या राष्ट्र को सामूहिक चेतना से है। आधुनिक व्यावसायिक र युग में विभिन्न राष्ट्रों के भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अपने-अपने व्यावयायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शाब्दिक या अशाब्दिक, मौखिक या लिखित सम्प्रेषण प्रक्रिया क अनुसरण करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सम्प्रेषण को भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को आशाओं के अनरूप औचित्यपूर्ण व प्रभावी कैसे बनाए जाए।
सांस्कृतिक चेतना
(Cultural Consciousness)
विश्व-गांव (Global Village) की अवधारणा के द्वारा विभिन्न संस्कतियों के प्रति वैचारिक व व्यावहारिक जागरूकता एवं आदर-सम्मान की भावनाओं का प्रादुर्भाव है सास्कृतिक चेतना का प्रमाण है। आधुनिक विश्व में इन अन्तर्राष्ट्रीय, सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद उनकी व्यावसायिक कार्यशैली, व्यवस्थाओं व आर्थिक नीतियों में अनेकता में एक होती अयात व्यावसायिक विभिन्नताओं में एकरूपता की एक नई सोच का प्रादुर्भाव हुआ। सांस्कृतिक चेतना विभिन्न व्यक्तियों के मूल्यों तथा विश्वास पर निर्भर करती है।
व्यावसायिक सम्प्रेषण पर सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव
(Impact of Cultural Consciousness on Business Communication)
सास्कृतिक चेतना व्यावसायिक सम्प्रेषण के प्रत्येक चहल को प्रभावित करता जैस-आदर, शिष्टता या विनम्रता का प्रदर्शन प्रेषित सचना की मात्रा.बात करने कास्ट आवाज तथा लिखित सम्प्रेषण में प्रयुक्त पृष्ठ का आकार। उक्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सस्ता अतिरिक्त व्यावसायिक सम्प्रेषण व्यक्तिगत संस्कृति अथवा एक संगठन की संस्कृति जल जाति, वर्ग व राष्ट्रीयता, सामाजिक स्थिति व अन्य बातों से प्रभावित होता है।

द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि राष्ट्रीय संस्कृति, संगठन संस्कृति व व्यक्तिगत संस्कृति के अतिव्यापन की स्थिति में किस प्रकार का सम्प्रेषण आवश्यक होगा। कुछ स्थितियों में एक प्रकार की संस्कृति अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।
अन्तर्रास्कृतिक सम्प्रेषण
(Inter-cultural Communication)
सम्प्रेषण को संस्कृति एवं उपसंस्कृति पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करती है। सांस्कृतिक विविधताएँ सूचनाओं को अलग-अलग अर्थ प्रदान करती है, जैसे-उत्तरी अमेरिका के लोग शब्दो द्वारा स्पष्ट संकेत देते हैं, जबकि जापान के लोग सूचनाओं को गर्मजोशी, दैहिक भाषा, व्यक्तिगत मिलन आदि में व्यक्त करते है। इसी प्रकार, सांस्कृतिक विविधता के कारण ही विभिन्न राष्ट्रों के लोग अजनबी एवं अतिथियों के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं।
अशाब्दिक सम्प्रेषण – भी सांस्कृतिक विविधता के प्रभाव से सर्वथा अछूता नहीं है क्योंकि सांस्कृतिक विविधता के माध्यम से शारीरिक भाषा, रंग एवं कपड़े, आभूषण, अभिवादन का तरीका. हर्षोल्लास या द:ख को अभिव्यक्ति के तरीकों में वैश्विक स्तर पर अत्यधिक भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती है।
शाब्दिक सम्प्रेषण – व्यक्ति को मनोदशा, परम्परा व संस्कृति के अनुसार अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। अन्तसास्कृतिक विविधता के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक सम्प्रेषण के मौखिक एवं लिखित सम्प्रेषण में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है; उदाहरण के लिए, अमेरिका में अपने सहकर्मियों को उनके नाम के पहले शब्द द्वारा औपचारिक सम्बोधन दिया जाता है, जबकि इटली में अपने सहयोगियों को उनके पद या उपनाम द्वारा औपचारिक सम्बोधन दिया जाता है।
सांस्कृतिक चेतना को सीखना
(Learning of Cultural Consciousness)
किसी भी राष्ट्र या संस्कृति के लोगों के साथ व्यापार करने अथवा सम्बन्ध बनाने से पहले यह आवश्यक है कि उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन कर लिया जाए तथा
स्वयं को उस संस्कृति के अनुसार ढाल लिया जाए। साथ ही उस संस्कृति के अनुरूप स्वयं । ढालना व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम रहता है। इस हेतु निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रख कर चाहिए-
(1) सम्बन्धित राष्ट की संस्कृति से सम्बन्धित लेखों व पुस्तकों का अध्ययन किया जा चाहिए, ताकि आप उनके इतिहास, रीति-रिवाज, धर्म, जाति व राजनीति से परिचित हो सर्व सम्म इसके अतिरिक्त, इस अध्ययन के माध्यम से हम वहाँ के मौसम, स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा कर मुद्रा, परिवहन सुविधाओं तथा सम्प्रेषण के साधनों से भी परिचित हो जाते हैं।
(2) सम्बन्धित देश की व्यावसायिक संस्कृति के बारे में जानकारी अर्जित कर सह व्यावसायिक दृष्टि से अति आवश्यक है। विशेष तौर पर उनकी उपसंस्कृति व व्यावसायि उपसंस्कृति के सम्बन्ध में क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी व्यावसायिक नीतियाँ, नियम सद संलेख होते हैं। कौन निर्णय लेता है, क्या उपहार स्वीकार्य है, पोशाक क्या है, इत्यादि। जानकारी होना भी अति आवश्यक है।
(3) सर्वप्रथम सम्बन्धित राष्ट्र की भाषा का अध्ययन करना चाहिए, इससे उन संस्कृति को सीखने के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इससे हम उनके रीति-रिवाजों व परम्पराओं प्रात परिचित हो जाएंगे, इसके फलस्वरूप सम्बन्धित राष्ट्र के व्यक्तियों से हमारी अन्तरंगता बढ़ेगी
अन्तसस्कृितिक सम्प्रेषण के लिए ध्यान रखने योग्य बातें
(Points to be kept in Mind for Inter-cultural Communication)
जब हम किसी अन्य राष्ट्र की संस्कृति को सीखने की इच्छा या आवश्यकता महसा सम करते हैं तो हमारे पास दो सरल मार्ग होते हैं
(1) किसी संस्कृति को स्वीकार करने में सहायक सामान्य कशलताओं को विकसि कर करना।
(2) अधिकाधिक रूप से सम्बन्धित संस्कृति की भाषा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व इतिहास वेश सामाजिक नियम व अन्य विशिष्ट संस्कृति, जिसकी आप व्यवसाय में आवश्यकता महसूर सो करते हैं, को सीखना।
प्रथम मार्ग-एक विशिष्ट संस्कृति का गहन अध्ययन बहुत सरल है, परन्तु इसमें द कमियाँ होती हैं
(1) प्रथम मार्ग की एक कमी यह है कि किसी विशिष्ट संस्कृति में लीन होना अति सामान्यीकरण के जाल की स्थिति है। किसी भी व्यक्ति को सांस्कृतिक दृष्टि से देखना होगा। प्रभ कि उसके अद्वितीय लक्षणों को व्यक्तिगत रूप में देखना।
(2) आप कभी भी किसी संस्कृति को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। उदाहरणार्थ पृष् बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने जर्मन संस्कृति का कितना अध्यय किया है। आप न कभी जर्मन थे और न ही आपने जर्मनी के अनुभवों को कभी जानने कचा कोशिश की है। यदि आप जर्मन संस्कृति को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो भी कोई जर्मन आपर्व इस विचार से सहमत नहीं होगा कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते और समझते हा मानद्वितीय मार्ग-संस्कृति को सीखने हेतु सामान्य अन्तसांस्कृतिक कशलताओं के सीखना बहुत उपयोगी होता है, जब आप एक संस्कृति या उपसंस्कृति से यक्त व्यक्ति से संवाद
करते हैं। अत: अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्सास्कृतिक सम्प्रेषण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है-
1. सम्प्रेषण दायित्व स्वीकार करना हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हमारे साथ सम्प्रेषण करना किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी है बल्कि इसका दायित्व स्वयं को स्वीकार करना चाहिए।
2. निर्णय स्थान – सम्पूर्ण सन्देश को सुनना तथा अन्य सन्देशों में अन्तर करने को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। यिक
3. लचीलापन हमें अपने स्वभाव, रुचि, आदतों व नजरिए में परिवर्तन के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।
4. संवेदनशीलता को बढ़ाना – सम्प्रेषण के भौतिक चलन के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता का होना अति आवश्यक है। दोषयुक्त सम्प्रेषण से सदैव बचना चाहिए। इनकी
5. आदर प्रदर्शन – सम्प्रेषण के प्रति भावों व आँखों के द्वारा तथा अन्य संस्कृतियों के , आद प्रों से प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए।
6. दोहरापन छोड़ना – विपरीत परिस्थितियों में अपनी कुण्ठाओं पर नियन्त्रण रखकर दोहरापन रोकना चाहिए।
7. धैर्य रखना – किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए धैर्य रखना अति आवश्यक है।
8. अन्य के दृष्टिकोणों व विचारों को समझना – सन्देश को ध्यानपूर्वक सुनकर हसूस सम्प्रेषण के भावों व दृष्टिकोणों को समझना चाहिए।
9. स्पष्ट सन्देश – हमें लिखित अथवा मौखिक सन्देश के द्वारा स्पष्ट सन्देश प्रदान कसित करना चाहिए।
10. बाह्य अवसरों के अतिरिक्त सोचना – हमें अपनी विचार श्रृंखला को मात्र हास वेशभूषा तथा पर्यावरणीय असुविधाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इससे भी आगे हसूस सोचना चाहिए।
एक प्रभावशाली अन्तर्सास्कृतिक सम्प्रेषण के तत्त्व
(Elements of an Effective Inter-cultural Communication)
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक तत्त्वों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए
(1) अन्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों से सम्प्रेषण करते समय उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व संस्कृति को अपने दृष्टिकोण से देखना-परखना उचित होता है।
(2) सम्प्रेषण सम्बन्धी अपनी कमियों को चिह्नित करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
(3) किसी व्यक्ति की भाषा या संस्कृति के सम्बन्ध में बातचीत करते समय आप ही मानसिक स्तर पर उससे जुड़कर लाभ अर्जित कर सकते हैं। –
(4) यदि आप अन्य संस्कृति के प्रति आदर-सम्मान रखेंगे तो आप स्वयं भी सम्मान के संवा पात्र होंगे।
प्रश्न – प्रस्तुतीकरण क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतीकरण को समझाइए।
What is Presentation? Discuss various types of presentation.
अथवा प्रस्तुतीकरण पर एक लेख लिखिए।
Write a detail note on Presentation.
अथवा सार्वजनिक प्रस्तुति से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्यों की सविस्तार व्याख्या कीजिए।
What do you understand by Public speaking? Explain the purpose of public presentation.
अथवा सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण को सफल बनाने के लिए आवश्यक पगों की व्याख्या
कीजिए।
Explain the essential steps to make effective public presentation, an
उत्तर – सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण को उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जगत् में सार्वजनिक का मौखिक अभिव्यक्ति अथवा सार्वजनिक वाक्शक्ति के सन्दर्भ में प्रयोग किया गया है। उसे व्यावसायिक जगत में अनेकों ऐसे अवसर आते हैं जिनमें सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण किया जाता वा है। प्रमुख अवसर निम्न प्रकार हैं
(i) नवीन उत्पाद अथवा सेवा के प्रारम्भ करने पर
(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर
(iii) नवीन व्यावसायिक रूपरेखा की व्याख्या
(iv) विपणन अथवा विक्रय लक्ष्यों के प्रस्ताव
(v) व्यवसाय क्रियाओं के परिवर्तन की जानकारी
(vi) विचारगोष्ठी, सेमिनार अथवा कॉन्फ्रेंस
प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य
(Purpose of Public Presentation)
1. निर्देश एवं तकनीकी ज्ञान (Direction and Technical Knowledge)- प्र प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य संस्था के कर्मचारियों के कार्यक्रमों को सामूहिक रूप से निर्देश एवं अ प्रशिक्षण प्रदान करना भी होता है। नवीन तकनीकी का ज्ञान भी प्रस्तुतीकरण द्वारा ही दिया जाता दि है। प्रस्तुतीकरण द्वारा ही नए व्यक्तियों एवं नए कर्मचारियों को सामहिक रूप से संगठनात्मक कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति से परिचित कराया जाता है एवं आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं।
2. सूचना देना (To give Information)-व्यावसायिक संगठन के लक्ष्यों, सन्देशों विचारधारा, नवीन तथ्यों एवं महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की व्याख्या प्रभावी सार्वजनिक अभिव्यक्ति करती है। नवीन उत्पादों, अनुसन्धानों, सुधारों प्रयोग के ढंग, उपभोक्ताओं के हितों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को इसके द्वारा ही प्रकट किया जाता है।3. औपचारिक कार्यक्रम (Formal Programme)-संगठन में उदघाटन सम्पादन, अभिनन्दन, प्रेरणा, सम्मान, विदाई, शपथ समारोह या अन्य औपचारिक कार्यक्रमों के आयोजन होते रहते हैं। इन समारोहों एवं कार्यक्रमों में सहभागिता तथा कार्यक्रम को सार्थक र स्वरूप प्रदान करने के लिए भी सार्वजनिक भौतिक प्रस्तुतीकरण किया जाता है।
4. प्रभावित करना (Persuasion)–-सार्वजनिक प्रस्ततीकरण का मूल उद्देश्य श्रोताओं एवं दर्शकों को विचारों, सन्देशों एवं दृष्टिकोणों द्वारा प्रभावित करना होता है। प्रभावी वाक्शक्ति दर्शकों को निश्चित परिणामों एवं वांछित प्रतिक्रियाओं के लिए प्रेरित करती है जिसमें संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की सफलता निहित होती है।
5. मूल्यांकन (Evaluation) – अधिकृत सार्वजनिक वाक्शक्ति का सम्बन्धित श्रोताओं, दर्शकों या व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन, विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है।
प्रस्तुतीकरण को सफल बनाने के आवश्यक पग
(Steps to make a successful Presentation)
1. प्रस्तुति के अवसर व उद्देश्य का स्पष्ट होना (Be clean about the Occasion and Object of Presentation)—प्रस्तुतकर्ता को प्रस्तुति के सन्दर्भ, कारणों तथा लक्ष्य क का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। प्रस्तुति के समय घटित होने वाली घटनाओं की सम्पूर्ण रूपरेखा है। उसे बिन्दुवार मालूम होनी चाहिए। प्रस्तुतकर्ता का दायित्व है कि वह प्रस्तुति में प्रयोग किए जाने ता वाले तथ्यों, सांख्यिकी का व्यवस्थित क्रम से संग्रह, अवलोकन एवं अध्ययन कर ले तभी प्रस्तुति प्रभावशाली हो सकती है। नवीन उत्पाद को बाजार में उतारते समय प्रस्तुतकर्ता को उत्पाद के समस्त गुणों, कमियों, तकनीकों, प्रयोग करने के ढंग, मूल्य, उपयोगिता एवं प्रतियोगी उत्पादों से अपने उत्पाद की गुणवत्ता आदि की जानकारी होना आवश्यक है।
2. वैयक्तिक गुण (Personal Qualities)-एक सफल प्रस्तुति के प्रस्तुतकर्ता में आत्मविश्वास, आकर्षक व्यक्तित्व, सहजता, सकारात्मक दृष्टिकोण, विनम्रता, उदारता, तीव्र स्मरण शक्ति, निर्णयन क्षमता, वाक्पटुता एवं प्रभावी सम्प्रेषण कौशल का होना अति आवश्यक है।
3. श्रोता विश्लेषण (Audience Analysis)-प्रस्तुति से पूर्व वक्ता को यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि प्रस्तुति किस वर्ग एवं प्रकार के श्रोताओं के मध्य की जानी है। श्रोता केवल एक स्थान विशेष पर एकत्रित व्यक्तियों की भीड़ नहीं होती बल्कि उनका एक मिश्रित एवं सामूहिक व्यक्तित्व होता है। श्रोताओं की संख्या एवं प्रस्तुति का औपचारिक अथवा अनौपचारिक स्वरूप ही – प्रस्तुति को प्रभावित करता है। श्रोताओं का आयु वर्ग, लिंग, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव, राष्ट्रीयता एवं आदि का प्रस्तुतकर्ता को पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि तदनुरूप शब्दों का चयन, वाक्य जात विन्यास स्तर, उदाहरण, प्रसंग, व्याख्या आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। मन यदि वक्ता अधिकांश श्रोताओं से पूर्व परिचित है, तो प्रस्तुति अधिक प्रभावी होती है। हैं। इसीलिए अपरिचित प्रस्तुतिकर्ता कभी-कभी प्रस्तुति से पूर्व श्रोताओं से मिलता है। देशा श्रोताओं के विश्लेषण की प्रक्रिया प्रस्तुतिकर्ता द्वारा प्रस्तुतिकाल में भी सतत रूप से की कि जानी चाहिए। वक्ता को सदैव अपने आँख और कान श्रोताओं पर केन्द्रित रखने चाहिए। वक्ता अद्वारा श्रोताओं की प्रतिक्रिया अविलम्ब महसूस की जानी चाहिए। श्रोताओं की दैहिक भाषा,
मुखाभिव्यक्ति वक्ता को तुरन्त पर्याप्त फीडबैक प्रदान करती है। श्रोताओं की उत्तेजना, जाटन कानाफूसी, खामोशी आदि भी वक्ता को भाव सम्प्रेषित करती है।
4. प्रस्तुति की विधि का निर्धारण (Decision of Method of Presentation)नार्थ यद्यपि प्रस्तुति का ढंग, प्रस्तुत किए जाने वाले कथनों की प्रकृति एवं प्रस्तुति अवसर पर निर्भर करता है, लेकिन एक सफल प्रस्तुति के लिए प्रस्तुति करने का ढंग पूर्व-निर्धारित होना चाहिए। सामान्यत: सार्वजनिक प्रस्तुति की तीन प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं
(i) तात्कालिक प्रस्तुति (Extempore Presentation)-तात्कालिक प्रस्तुति सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें पूर्व संचित ज्ञान, अनुभव एवं वाक्पटुता की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें वक्ता दृष्टिकोण एवं चिन्तन द्वारा अपनी प्रस्तुति की कच्ची रूपरेखा नोट कर लेता है एवं प्रस्तुति के समय उसके मस्तिष्क में विचारों का आगमन स्वाभाविक रूप से होता है जिसमें से वह प्रस्तुति योग्य विचारों का चयन कर लेता है। यह मानसिक क्रिया तथा प्रस्तुति समानान्तर प्रक्रिया है। विशेष परिस्थितियों में किसी अवरोध के कारण यदि प्रस्तुति का क्रम टूटता है तो वह कच्ची रूपरेखा को देख लेता है। तात्कालिक प्रस्तुति द्वारा वक्ता मानसिक विचारों, दृष्टिकोणों एवं कल्पनाओं का स्वाभाविक रूप से प्रस्तुतीकरण करता है। तात्कालिक प्रस्तुति में मानसिक विचारों तथा प्रस्तुति से तादात्म्य स्थापित करना आवश्यक होता है। सामूहिक परिचर्चा, सम्मेलन आदि में प्रस्तुति विधि का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी प्रस्तुतीकर्ता की एकाग्रता भंग होने पर विचारों की श्रृंखला टूट जाती है जिसका प्रस्तुति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा विषय से हटकर अभिव्यक्ति हो जाती है।
(ii) पढ़कर प्रस्तुति (Reading Presentation)-बहुत से वक्ता अपने विचारों तथा सन्देशों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से लिख लेते हैं तथा श्रोताओं के सम्मुख उसको पढ़कर प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में क्रमबद्धता एवं शुद्धता दोनों होती हैं। शोधपत्रों, वैज्ञानिक महत्त्व के समझौतों, महत्त्वपूर्ण सूचनाओं, कार्य-सूची, पारित अथवा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव, सूक्ष्म तकनीकी ज्ञान, मार्गदर्शक सन्देशों, नीतिगत विचारों एवं तथ्यों की प्रस्तुति प्राय: लिखित रूप में पढ़कर की जाती है। पढ़ते समय वक्ता को उच्चारण तथा व्याकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
(iii) स्मृति आधारित प्रस्तुति (Memorised Presentation)-इस विधि का प्रयोग तीव्र स्मरण शक्ति वाले वक्ता करते हैं। वक्ता सम्पूर्ण प्रस्तुति को प्रारम्भ में ही व्यवस्थित क्रम वक में लिखकर स्मरण कर लेता है फिर उसकी प्रस्तुति करता है, लेकिन यदि किसी कारणवश उसके मुख विचारों का क्रम टूट जाता है या प्रस्तुति के महत्त्वपूर्ण बिन्दु उसके ध्यान में नहीं आते हैं तो प्रस्तुति कर अर्थहीन हो जाती है। इस विधि के सफल प्रस्तुतिकर्ता महत्त्वपूर्ण विचारों को स्मरण करने के प्रभ साथ-साथ बिन्दुवार नोट भी कर लेते हैं एवं इसी कारण से वे सार्थक प्रस्तुति करने में सफल भी होते हैं। अधिकांश वक्ता विचारगोष्ठियों तथा सेमिनार में प्रस्तुति की इसी विधि का प्रयोग करते हैं।
5. प्रस्तुति स्थल पर विचार (Have an Idea of the Location)-एक सफल एक प्रस्तुति के लिए स्थल एक महत्त्वपूर्ण घटक होता है। प्रस्तुति में श्रोताओं की संख्या के अनुरूप विर आरामपूर्वक बैठने की पर्याप्त जगह, अनुकूल वातावरण एवं तापमान, ध्वनि व प्रकाश क का सन्तोषजनक व्यवस्था, श्रव्य-दृश्य यन्त्रों एवं अन्य सहायक सामग्री का व्यवस्थित संचालन पर्याप्त रूप से प्रस्तुति को प्रभावित करते हैं। अत: आयोजकों एवं वक्ता को प्रस्तुति से पूर्व ही आयोजन का निरीक्षण कर आवश्यक पूर्वानुमान लगा लेने चाहिए अन्यथा प्रस्तुतिका चार जितना भी सार्थक प्रयास करले प्रस्तुति सफल नहीं हो पाती: जैसे-आयोजन स्थल पर ध्वान कर पुनरावृत्ति करती है तो श्रोताओं को सन्तोषजनक ढंग से सुनायी नहीं देगा और यदि स्थल क तापमान काफी गर्म है, तो लोग घुटन महसूस करेंगे। इस परिस्थिति में वक्ता द्वारा प्रभावी प्रस्तु को श्रोता नीरस एवं बकवास समझेंगे।
6. प्रस्तुति की रूपरेखा तैयार करना (Plan out the Presentation)-प्रस्तुति विधि का चयन करने के पश्चात् वक्ता या प्रस्तुतिकर्ता को प्रस्तुति की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। एक सफल प्रस्तुति के लिए यह आवश्यक है कि आयोजक अथवा प्रायोजक श्रव्य-दृश्य यन्त्रों को संचालित करने वाले सहयोगी तथा सह प्रस्तुतिकर्ता (यदि कोई है) के साथ इस पर विचार-विमर्श कर लेना चाहिए। कच्ची रूपरेखा निम्न प्रकार तैयार की जा सकती है
प्रारम्भिक (Beginning)
(i) प्रारम्भिक कथन – अभिवादन, सम्बोधन एवं प्राक्कथन (Introductory Remark)
(ii) उद्देश्यात्मक कथन — प्रस्तुति करने के कारण एवं अवसर के सम्बन्ध में
(iii) प्रस्तुति का स्थूल वर्णन (Draw the outlines of Presentation)
मध्य (Middle)
(i) प्रस्तुति के कथनों का बिन्दुवार संक्षिप्त विभाजन
(ii) प्रत्येक बिन्दु की समय सीमा का निर्धारण
(iii) सम्बन्धित उदाहरणों की प्रसंग सहित बिन्दुवार व्याख्या
समापन (End)
() सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का सार कथन
(ii) महत्त्वपूर्ण उद्देश्यपरक बिन्दुओं की विभिन्नता सहित पुन: संक्षिप्त सन्दर्भ
(iii) अन्तिम टिप्पणी
(iv) सकारात्मक भावनाओं सहित धन्यवाद
7. दैहिक एवं पार्श्व भाषा (Effective use of Body and Para Language)वक्ता को प्रस्तुति करते समय, प्रस्तुति के अनुरूप शारीरिक संचालन, भावभंगिमा, मुद्रा, मुखाभिव्यक्ति आदि का प्रयोग करना चाहिए। भावशून्य प्रस्तुति नीरस होती है। विचारों को व्यक्त करते समय भाषा एवं पार्श्व भाषा का उचित मिश्रण करना चाहिए। इससे कथनों में प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है।
8. घबराहट से उबलना (Overcoming Nervousness)-कोई भी व्यक्ति जन्म से प्रभावी वक्ता नहीं होता। प्रबुद्ध श्रोताओं के मध्य प्रस्तुति करते समय घबराहट उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किन्तु प्रस्तुतिकर्ता इस क्षणिक अवस्था से उबर सकता है तथा विश्वासपूर्वक प्रस्तुति देने में सक्षम हो जाता है। घबराहट से उबरने के लिए निम्नलिखित तत्त्वों को ध्यान में रखना चाहिए
(i) पूर्व अभ्यास बार-बार करना चाहिए। ___
(ii) प्रस्तुति पर विचार केन्द्रित करना चाहिए।
(iii) प्रस्तुति से पूर्व स्वयं को तरोताजा बनाना चाहिए और मानसिक दबाव को भी कम करना चाहिए।
(iv) प्रस्तुति के समय सभी श्रोताओं की ओर नजर घुमानी चाहिए।
(v) सामान्य स्वर में कम गति से बोलना चाहिए।
(vi) क्षणिक विराम पर आवाजरहित गहरी सांस लेनी चाहिए।
9. पूर्व प्रयोग (Rehearsal)- त्रुटिरहित प्रस्तुति के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक प्रस्तुति से पहले उसका अभ्यास कर लिया जाए। पूर्व अभ्यास से वक्ता में आत्मविश्वास आता है और उसमें आत्मसुधार होता है। प्रस्तुति की टीम द्वारा पूर्व अभ्यास किए जाने से सहयोगियों से परस्पर सकारात्मक व आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की जाती है जिनको सुधार कर प्रस्तुति को सफल बनाया जा सकता है। प्रस्तुति पूर्व अभ्यास के द्वारा सभी वक्ताओं एवं दृश्य-श्रव्य, ध्वनि व प्रकाश सहायकों के बीच सुन्दर समन्वय स्थापित होने के साथ-साथ अवरोधकों का भी पर्याप्त उपचार हो जाता है।
10. सहायक दृश्य सामग्री का प्रयोग (Use of Visual Aids)-प्रस्तुति की सूचनाओं, कथनों, विचारों के प्रभावी सम्प्रेषण के लिए दृश्य सहायक सामग्री; जैसे–चार्ट, ब्लैकबोर्ड, चित्र, नक्शा, पिक्चर, स्लाइड, पारदर्शी स्लाइड, कम्पैक्ट डिस्क (C.D.) आदि का उपयोग होता है। प्रस्तुति में प्रयोग की जा सकने वाली दृश्य सामग्री की एक लम्बी श्रृंखला होती है, लेकिन वक्ता की प्रस्तुति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व उपलब्ध सामग्री का पूर्व चयन कर लेना चाहिए। प्रस्तुति के समय दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग भी एक कौशल है। अतः इसको प्रयोग करते समय निम्नलिखित तत्त्वों को ध्यान में रखना चाहिए
(i) दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग कथन/सन्देश की मुख्य विषय-वस्तु के लिए किया जाना चाहिए।
(ii) सम्पूर्ण प्रस्तुति काल में नवीन उत्पाद पर नवीन शोध वस्तु को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिसे दर्शक सुविधापूर्वक देख सकें।
(iii) दृश्य सहायक सामग्री ऐसे स्थान पर लगायी जानी चाहिए जिसे सभी श्रोता सुविधापूर्वक देख सकें तथा बिना अवरोध के वक्ता भी प्रस्तुति करते समय उस दृश्य सामग्री तक पहुँच सके।
(iv) छड़ी अथवा स्टीकर के माध्यम से पिक्चर को समझाते समय वक्ता की नजर श्रोताओं पर होनी चाहिए।
(v) लम्बे समय तक कोई भी दृश्य सामग्री श्रोताओं के बीच न रहे। इससे श्रोताओं का ध्यान भंग होता है।
(vi) स्लाइड्स तथा पारदर्शी स्लाइड के प्रदर्शन को ठीक ढंग से पूर्व नियोजित कर लेना चाहिए।
(vii) दृश्य सहायक सामग्री इतनी ऊँचाई अथवा कार्नर पर होनी चाहिए जिससे दृश्य सामग्री की व्यवस्था करते समय प्रस्तुतिकर्ता, श्रोताओं के लिए स्वयं बाधा न बन सके। दृश्य सामग्री का स्थान लगभग इस प्रकार होना चाहिए
11. प्रश्नोत्तर काल (Question-Answer Session)-आवश्यकतानुसार प्रस्तुति के उपरान्त प्रश्नोत्तर काल का भी महत्त्व है। प्रश्नोत्तर काल में प्रस्तुतिकर्ता का दायित्व है कि वह श्रोताओं की जिज्ञासाओं को शान्त करे एवं उनके प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर अवश्य दे। प्रश्नों की पुनरावृत्ति पर उत्तेजित होने के बजाय विनम्रतापूर्वक उस बिन्दु की प्रश्न के सन्दर्भ में सभी व्याख्या करे। अग्रिम व अन्तिम पंक्ति के मध्य सभी श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। यदि वक्ता प्रस्तुति के कारण थका हुआ होता है प्रतिपुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्दबाजी में प्रश्नोत्तरकाल को निबटाने का प्रयास करता है। वक्ता को ऐसा न करके धैर्य रखना चाहिए क्योंकि प्रस्तुति का समापन वास्तव में प्रश्नोत्तरकाल के बाद ही होता है।
प्रश्न – अंगूरीलता सम्प्रेषण का आशय स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं एवं | प्रकार बताइए।
Explain the meaning of grapevine communication and describe कर its characteristics and types.
उत्तर- अंगूरीलता सम्प्रेषण का आशय सको
(Meaning of Grapevine Communication)
अंगूरीलता सम्प्रेषण अनौपचारिक सम्प्रेषण का ही एक रूप है। सामाजिक मनोविज्ञान के लिए अनुसार व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति सामाजिक ही होती है। अधिकांश व्यक्ति सामूहिक रूप से
मिलने एवं बातचीत करने के अवसरों को नहीं खोना चाहते। किसी व्यवसाय एवं संगठन में । पर साथ-साथ कार्य करने वाले व्यक्ति शनैः शनैः अनौपचारिक ढंग से आपस में मिल-बैठकर
व्यवसाय के सम्बन्ध में संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं। यह सम्प्रेषण अवकाश के क्षणों में श्रोता अथवा भोजनावकाश में, सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में, क्लबों एवं पार्टियों में अथवा मग्री जब कभी भी उसे अवसर प्राप्त होता है, सम्प्रेषण करते हैं। इस सम्प्रेषण में जहाँ एक ओर तथ्यपूर्ण एवं सार्थक विषयों पर चर्चाएँ होती हैं, वहीं दूसरी ओर गप्पबाजी तथा अफवाहों का नजर बाजार भी गर्म होता है।
अंगूरीलता सम्प्रेषण की विशेषताएँ
(Characteristics of Grapevine Communication)
(1) अंगूरीलता सम्प्रेषण की स्थायी रूपरेखा नहीं होती।
(2) अंगूरीलता सम्प्रेषण सत्य के निकट हो भी सकता है और नहीं भी क्योंकि इसमें सुनी-सुनाई सूचनाओं का प्रसारण होता है।
(3) अंगूरीलता सम्प्रेषण में कुछ-न-कुछ मिलावट अवश्य ही होती है। जितने अधिक व्यक्तियों के मध्य से होकर यह सन्देश गुजरता है, उतना ही अधिक यह विकृत हो जाता है।
(4) अंगूरीलता सम्प्रेषण प्राचीनतम प्रणालियों में से एक है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अधिक महत्त्व भी है।
(5) अंगूरीलता सम्प्रेषण में सामान्य, गोपनीय, मूल्यवान एवं व्यर्थ सभी प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण होता है।
(6) अंगूरीलता सम्प्रेषण लम्बवत्, क्षैतिज, कर्णीय (आड़ी-तिरछी) आदि सभी दिशाओं में हो सकता हैं।


अवरोही सम्प्रेषण के उद्देश्य
(Objectives of Downward Communication)
अवरोही सम्प्रेषण द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ण किए जा सकते हैं
(1) अवरोही सम्प्रेषण का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को प्रभावकारी तरीके से सम्पन्न करे। .
(2) यह कर्मचारियों के कार्य सम्पादन में सुधार के लिए प्रेरित करता है।
(3) एक विशिष्ट कार्य के लिए अपने अधीनस्थ कर्मियों को शिक्षित करता है।
(4) यह एक संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।
(5) यह इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देता है कि क्या और कैसे करें।
अवरोही सम्प्रेषण के लाभ
(Advantages of Downward Communication)
अवरोही सम्प्रेषण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं
(1) अवरोही सम्प्रेषण अधीनस्थ कर्मियों के संगठन की योजनाओं, नीतियों कार्यक्रमों ५ प्रक्रियाओं, कार्यविधि व अन्य आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराकर कार्य सम्पादन में सहायक होता है।
(2) प्रभावी प्रतिपुष्टि के लिए अधीनस्थों के क्रिया-कलापों पर नियन्त्रण रखता है।
(3) यह कर्मचारियों के कार्य निष्पादन को गति देने को प्रेरित करता है।
(4) यह अधीनस्थों से प्रबन्धन को जो उम्मीद रहती है उसे प्राप्त करने में सहायक होता है।
अवरोही सम्प्रेषण की सीमाएँ
(Limitations of Downward Communication)
संगठनात्मक स्वरों के माध्यम से सम्प्रेषण का नीचे की ओर प्रवाह की प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं
1. अल्प या अधि-सम्प्रेषण (Under or Over Communication)-अवरोही सम्प्रेषण में सूचनाओं के संकुचन या अनावश्यक विस्तार की सम्भावना बनी रहती है। कभी-कभी मा उच्चाधिकारी केवल सूचना के महत्त्वपूर्ण अंश का ही सम्प्रेषण करते हैं और यह मान लेते हैं कि जि सूचना की पृष्ठभूमि लोगों को स्वाभाविक रूप से ज्ञात है। परिणामस्वरूप लोगों को अधूरा सम्प्रेषण की ही हो पाता है एवं कार्य का परिणाम असन्तोषप्रद होता है तथा अधिसम्प्रेषण में गोपनीयता भंग होने मौ तथा अनावश्यक विवरण से सन्देश का वास्तविक अर्थ खो जाने का भय रहता है।
2. विलम्ब (Delay)—संगठनात्मक स्तरों के माध्यम से सम्प्रेषण का नीचे की आर. प्रवाह समय लेने वाली प्रक्रिया है। विलम्ब से सूचनाओं का सम्प्रेषण संगठन की गतिविधियों का सर हतोत्साहित कर देता है।
3.प्रतिरोध (Resistance)-अवरोही सम्प्रेषण की नीतियों एवं अधीनस्थों का सहभागिता नहीं होती। अधीनस्थों में असन्तोष उत्पन्न होता है। कार्यों के सम्पादन क व्यावहारिक कठिनाइयों की बिना जानकारी के ऊपर से आदेश प्राप्त हो जाते हैं, जिससे
नियोक्ता-कर्मचारी अथवा पर्यवेक्षक-अधीनस्थ सम्बन्धों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं अधीनस्थों द्वारा ऐसे सम्प्रेषणों का प्रतिरोध किया जाता है!
4. मिश्रण (Mixing)-अवरोही सम्प्रेषण विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। इसमें किसी भी स्तर पर निहित कारणों से सन्देश में संशोधन, परिवर्तन, अनावश्यक मिश्रण किया जा सकता है, जिससे सन्देश का अर्थ, स्वरूप व भाव बदल सकता है।
अवरोही सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने के उपाय
(Essentials of Effective Downward Communication)
अवरोही सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं
(1) एक संगठन में अनुकूल सम्प्रेषण का पर्यावरण होना चाहिए। सन्देश सम्प्रेषित होने से पूर्व उससे उत्पन्न होने वाले सभी विभ्रमों को दूर कर लेना चाहिए। एक प्रबन्धक को सदैव अनुकूल सम्प्रेषण पर्यावरण के निर्माण के लिए सहयोग व निश्चितता का वातावरण निर्मित करना चाहिए।
(2) संगठन के उच्च व निम्न सभी प्रकार के कर्मचारियों को संगठन के समस्त उद्देश्यों एवं उसकी गतिविधियों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी होनी अनिवार्य है, जिससे कि सम्प्रेषित सन्देश विभ्रम में किसी प्रकार के प्रश्न व जाँच का उत्तर दे सकें।
(3) अवरोही सम्प्रेषण में सम्प्रेषण को सदैव साफ और सम्पूर्ण सन्देश सरल व सीधी भाषा में प्रेषित करना चाहिए।
(4) किसी अधिकारी को जारी आदेश या निर्देशों पर अतिकेन्द्रित व्यवहार को अनदेखा करना चाहिए क्योंकि इस सम्प्रेषण प्रक्रिया में उसके अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं।
(5) एक संगठन में अवरोही सम्प्रेषण उचित माध्यमों से होना चाहिए।
प्रश्न –सामूहिक सम्प्रेषण तन्त्र से आप क्या समझते हैं? सामूहिक सम्प्रेषण तन्त्र को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
What do you mean by Symbiotic Interactionism ? Describe the affecting factors of Symbiotic Interactionism.
उत्तर- सामूहिक (सहजीवी) सम्प्रेषण तन्त्र
(Symbiotic Interactionism) एक ‘सम्प्रेषण तन्त्र’ का अभिप्राय, एक संगठन में विभिन्न छोटे-छोटे समूह-तन्त्रों के भी माध्यम से अन्तर्सम्बन्धित सम्प्रेषण से है। इस तन्त्र में छोटे-छोटे अनेक सम्प्रेषण जाल होते हैं, के जिनके आधार पर एक सम्पूर्ण तन्त्र विकसित होता है, इसे सम्प्रेषण तन्त्र कहते हैं। व्यक्ति ण की मूल प्रवृत्ति ‘समूह’ में रहने की होती है क्योंकि वह समूह में रहकर ही अपनी आधारभूत ने मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सफल हो सकता है। यह समूह मौलिक रूप में दो प्रकार का हो सकता है
1. औपचारिक (Formal)-औपचारिक समूह का अभिप्राय एक संगठन की कार्य को संरचना से है, अर्थात् कार्य संरचना के आधार पर निर्मित समूह औपचारिक होता है। इसका प्रत्येक सदस्य संगठन के लक्ष्यों के प्रति क्रियाशील रहता है।
2. अनौपचारिक (Informal)-अनौपचारिक समूह से अभिप्राय सामाजिक व वयक्तिक कारणों के स्वाभाविक रूप से निर्मित समूह से है। इसमें व्यक्ति अपने हितो, रुचि, सआदत, क्षेत्र, भाषा व आयु के आधार पर एकत्रित होता है।



2. सम्प्रेषण की प्रकृति (Nature of Communication)-सम्प्रेषण की प्रकृति भी उनको प्रभावित करती है क्योंकि सम्प्रेषण कई तरह का होता है; यथा-अर्थपूर्ण, परम्परागत, परस्पर, सम्पर्क नियोजित, संगठित, वार्तालाप आदि।
3. सूचना स्वामित्व (Information Ownership)—यद्यपि सूचना का स्वामित्व एक विशिष्ट व्यक्ति के हाथ में होता है, तथापि किसी महत्त्वपूर्ण सूचना के सम्प्रेषण में अन्य की हिस्सेदारी होने, न होने का निर्णय वह अपने विवेक के आधार पर लेता है।
4. सम्प्रेषण की औपचारिक श्रृंखला (Formal Channel of Communication)-चूँकि औपचारिक सम्प्रेषण शृंखला संरचना पूर्णत: उच्चाधिकारियों द्वारा नियन्त्रित होती है, अत: सम्प्रेषण की प्रकृति निर्देशात्मक व प्रतिसंघात्मक होगी।
5. अधिकार संरचना (Authority Structure)-विभिन्न पदों द्वारा सम्प्रेषण की दशाओं/ क्रियाओं का निर्धारण होता है, जैसे—सम्प्रेषण कैसे व किससे होगा। सम्प्रेषण के लिए स्थानापद भी महत्त्वपूर्ण होता है, अर्थात् सम्प्रेषण का तरीका पद व स्थिति पर निर्भर होता है।
6. कार्य विशिष्टीकरण (Job Specialization)-कार्य की विशिष्टता व दक्षता/ कुशलता सम्प्रेषण को प्रभावित करती है। अत्यधिक विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों में सम्प्रेषण की कमी व विशिष्ट व्यक्तियों में सम्प्रेषण/विचारों, भावनाओं, तकनीकों, उद्देश्यों व शैलियों का होना पाया जाता है। ____
प्रश्न -सम्प्रेषण की प्रमुख बाधाओं को समझाइए तथा उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए।
Explain main barriers of communication and give suggestions to remove them.
उत्तर – संसार में प्राणी के जन्म से ही सम्प्रेषण क्रिया प्रभावी हो जाती है, अर्थात् पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी सम्प्रेषण प्रक्रिया का प्रयोग करता है। परन्तु मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, जो अच्छे व प्रभावी ढंग से अपनी किसी भी बात को सम्प्रेषित कर पाने में सक्षम है। सम्प्रेषण को सम्प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुँचाने में कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं में आने वाली बाधाओं को ही ‘सम्प्रेषण की बाधाएँ’ कहते हैं।
सम्प्रेषण की बाधाएँ
(Barriers of Communication)
सम्प्रेषण को प्रभावित करने वाली बाधाओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है1. धन/वित्त सम्बन्धी बाधा (Money related Barrier)-धन की सीमितता के कारण भी सम्प्रेषण क्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। वित्तीय साधनों की अल्पता के कारण सन्देश सम्प्रेषणग्राही की पहुंच से दूर ही रह जाता है। वैज्ञानिक व शोधकर्ता विभिन्न स्थानों पर आयोजित संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, सम्मेलनों, कार्यशालाओं में हिस्सा लेने से वंचित रह जाते हैं। आधुनिक तकनीक महँगी होने के कारण इनके द्वारा सन्देश प्राप्त होने में व्यवधान आते हैं।
2. समय सम्बन्धी बाधा (Time related Barrier)-सन्देश के सम्प्रेषण के समय यदि औपचारिक माध्यमों का उपयोग किया जाता है तो वे अधिक समय लेते हैं। इन माध्यो द्वारा सन्देश के प्रकाशन में अधिक समय लगता है तथा सन्देश के सरल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।
3. साहित्यिक विस्फोट सम्बन्धी बाधा (Literature Explosion related Barrier)-ज्ञान के विस्फोट के कारण सम्पूर्ण साहित्य एक ही सम्प्रेषण केन्द्र से प्राप्त करना असम्भव है। स्वतन्त्र सम्प्रेषण में यह भी एक बाधक तत्त्व है।
4. आधुनिक तकनीक सम्बन्धी बाधा (Modern Technique related । Barrier)-वर्तमान समय में कम्प्यूटर के माध्यम से सम्प्रेषण प्रक्रिया को पूरा करना प्रत्येक के वश की बात नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस तकनीक का अभ्यस्त नहीं होता। साथ ही जिन स्थानों पर सन्देश कम्प्यूटर के माध्यम से सम्प्रेषित किए जाते हैं, वहाँ पर प्राप्तकर्ता उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है।
5. भाषा सम्बन्धी बाधा (Language related Barrier)-सम्प्रेषण के लिए भाषा अनिवार्य माध्यम है। शाब्दिक अथवा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार की भाषाओं का सम्प्रेषण में प्रयोग किया जाता है। अधूरी, अस्पष्ट भाषा तथा असामयिक विविध अर्थों वाले शब्दों या संकेतों का चयन-सम्प्रेषण में प्रमुख बाधा है।
6. माध्यम सम्बन्धी बाधा (Medium related Barrier)-सन्देश के सम्प्रेषण के सम्बन्ध में माध्यम अव्यवस्थित होते हैं। अधिकांश माध्यम सन्देश का सम्प्रेषण एक ओर ही करते हैं। इस कारण एक सूचनाग्राही किसी प्रकार की अधिक व स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में है असमर्थ होता है।
7. शासकीय प्रकाशन सम्बन्धी बाधा (Government Publication related Barrier)-अधिकांश शासकीय प्रकाशन इस प्रकार के होते हैं कि उनका सम्पूर्ण रूप से ह प्रकाशन असम्भव होता है, अत: इनका सम्प्रेषण अत्यधिक सीमित हो जाता है।
8. बोलचाल की भाषा सम्बन्धी बाधा (Speaking Language related Barrier)-अधिकांश सन्देश-सम्प्रेषक, सन्देश को सम्प्रेषित करते समय अपनी स्थानीय ए बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, अत: इस व्यवस्था में सन्देश का कुछ अंश प्राप्तकत्ता समझने में चूक जाता है। इससे सम्पूर्ण सन्देश सम्प्रेषित नहीं हो पाता है। यह सूचना-सम्प्रेषण वि की प्रमुख बाधा है।
9. आत्मनिर्भरता की कमी सम्बन्धी बाधा (Lack of Self-dependence अ related Barrier)-यदि सम्प्रेषक में आत्मनिर्भरता की कमी होती है तो सन्देश का सम्प्रेषण उचित ढंग से नहीं हो पाता क्योंकि वह किसी भी सन्देश को सम्प्रेषित करने के उत्कृष्टता या निकृष्टता का अहसास रखता है। ऐसी स्थिति में सम्प्रेषक अपने सन्देश का प्राप्तकर्ता तक उचित रूप में सम्प्रेषित कर पाने में असमर्थ होता है।
10. व्यवहार व धारणा सम्बन्धी बाधा (Behaviour and Concept relate Barrier)-कभी कभी व्यक्तिगत व्यवहार व धारणाएँ सम्प्रेषण की मुख्य बाधा बन जाता गलत धारणाएँ व व्यवहार सूचनाग्राही तक सन्देश को सही रूप में पहँचाने में बाधा उत्तपन्न करते हैं।
11.संगठन में एक से अधिक प्रबन्धन स्तरों की उपस्थिति (Presence of more One Management Stages in Organization)-जब संगठन में प्रबन्धन क स्तर होते हैं तो प्रेषित सन्देश में देरी अथवा सम्प्रेषण प्रक्रिया के असफल होने का सम्भावना बढ़ जाती है। यह भी सम्भव है कि दिए गए सन्देश का स्वरूप, सन्देशग्राही तक पहुँचने में बदल जाए।
12. अत्यधिक सूचनाओं का दबाव होना (Stress of Extra Informations)-जब सम्प्रेषण माध्यम पर अधिक सूचनाओं का दबाव होता है तब या तो जटिल सचनाएँ प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगी या प्राप्तकर्ता तक पहुँचने वाली सूचनाएं अप्रभावी रहेगी।
सम्प्रेषण की बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव
(Suggestions to remove the Barriers of Communication)
सम्प्रेषण किसी भी व्यवसाय का जीवन है। सम्प्रेषण किसी भी व्यक्ति को किसी भी संगठन में बनाए रख सकता है अथवा बाहर कर सकता है क्योंकि वह किसी भी संगठन की उन आन्तरिक व बाह्य गतिविधियों की सूचना देता है, जो उस संगठन के हित या अहित में होती हैं। । किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य को संगठन के सामूहिक प्रयासों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आज हर तरह की सूचनाएँ अत्यधिक मात्रा में सृजित हो रही हैं। इन सूचनाओं के सम्प्रेषण में तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित होती हैं। इन बाधाओं के निराकरण हेतु सुझाव निम्नलिखित “
(1) सम्प्रेषक को सम्प्रेषण में सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
(2) सम्प्रेषक द्वारा प्रसारित किए जाने वाले सम्प्रेषण का समय उचित रूप से निर्धारित होना चाहिए।
(3) परिस्थितियों के अनुगामी सम्प्रेषण के दिशा-निर्देश तय कर लेने चाहिए।
(4) सम्प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच सही अनुकूलन होना आवश्यक है। दोनों के मध्य एकरूपता का होना भी अति महत्त्वपूर्ण है।
(5) यदि सम्प्रेषण की क्रिया आमने-सामने हो रही है तो आशंका का निवारण तत्काल किया जाना सम्प्रेषण की बाधा को विकसित होने से रोक देता है।
(6) सम्प्रेषण की अभिव्यक्ति तथा भाषा सम्प्रेषणग्राही के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अपनायी जानी चाहिए।
(7) सन्देश के पश्चात् यदि आवश्यकतानुसार उसकी परिपुष्टि की जा सके तो सम्प्रेषण की बाधा का सम्यक् निराकरण हो सकता है।
(8) सम्प्रेषण की सम्पूर्ण क्रिया में श्रवणता का अति महत्त्वपूर्ण अवदान होता है, अत: सम्प्रेषण की बाधा से बचने के लिए श्रवणता के तत्त्व का उचित पालन किया जाना चाहिए।
(9) प्रत्यक्ष सम्प्रेषण किए जाते समय अन्य पक्ष के शारीरिक हाव-भाव का महत्त्व बढ़ जाता है। ऐसा करने से सम्प्रेषण में आने वाली बाधा को दूर किया जा सकता है अथवा बाधा के विकसित होने से पूर्व ही उसका निराकरण हो सकता है।
प्रश्न – ”होठों की आवाज की तुलना में मुस्कराहट अधिक प्रभावी है।” दैहिक भाषा सम्प्रेषण के सन्दर्भ में इसे स्पष्ट कीजिए।
“Sound of smile is more louder than voice of lips.” Explain it as resources to body language communication.
अथवा दैहिक भाषा सम्प्रेषण से आपका क्या अर्थ है? इसके गुण व दोषों को समझाड़ा।
What do you mean by Body Language ? Explain its merits and demerits.
उत्तर – शारीरिक भाषा
(Body Language)
शारीरिक भाषा से आशय शरीर के विभिन्न हिस्सों की गतिशीलता के द्वारा अपनी भावनाओं/संवेदनाओं के माध्यम से सन्देश/सूचना के सम्प्रेषण से है। शारीरिक भाषा के अन्तर्गत
आँखों को घुमाना/चलाना, होंठों को चबाना/चलाना, ताली बजाना इत्यादि सम्मिलित हैं। इसे ‘KINESICS’ भी कहा जाता है। इससे व्यक्ति अपने सन्देश को अन्तर्वैयक्तिक क्रियाकलापों/ २ गतिविधियों द्वारा अन्य व्यक्तियों या समूहों तक पहुँचाता है। यद्यपि शारीरिक भाषा भाषिक।
शाब्दिक सम्प्रेषण की पूरक कहलाती है क्योंकि जब यह शाब्दिक भाषा के पूरक का कार्य करती है, तब ही सम्प्रेषक के सन्देश का अर्थ स्पष्ट होता है और वह शाब्दिक भाषा के साथ • जुड़ जाती है।
जे० फास्ट के शब्दों में—“अविश्वास के लिए हमारे द्वारा अपनी भौंहों को ऊपर चढ़ाना, घबराहट, परेशानी के लिए नाक को रगड़ना/मलना, स्वयं को संरक्षित करने के लिए अपने हाथों को बाँधना, स्वयं को पृथक् बताने के लिए कन्धों को उचकाना, घनिष्ठता बताने के लिए आँख मारना/पलक झपकाना, घबराहट के लिए उँगलियों को थपथपाना, विस्मरण के लिए स्वयं के माथे को थप्पड़/चाँटा मारना इत्यादि क्रियाएँ शारीरिक भाषा के अन्तर्गत आती हैं।
” शारीरिक भाषा-एक प्राकृतिक प्रक्रिया
(Body language : A Natural Phenomenon)
शारीरिक भाषा सम्प्रेषण की सम्पूर्ण प्रक्रिया है जिसका स्वरूप प्राकृतिक है। इसमें भाषा के स्थान पर शारीरिक अंगों के हाव-भाव से विचारों का उचित सम्प्रेषण किया जाता है। इसका किसी प्रकार का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता है, लेकिन सतत अभ्यास के द्वारा इसका विकसित किया जा सकता है। वास्तव में शाब्दिक सम्प्रेषण के सापेक्ष शारीरिक भाषा के प्राकृतिक संवेग अधिक प्रभावशाली होते हैं। जितना सम्प्रेषणकर्ता शारीरिक भाषा में दक्ष होगा सम्प्रेषण की क्रिया उतनी ही सुगठित अवस्था को प्राप्त होगी। इसके कुछ उपादानों का विवरण निम्नलिखित है
1. आँखों का सम्पर्क (Eyes Contact)-आँखों द्वारा किसी विचार का सम्प्रेषण – शारीरिक भाषा का सबसे मुखर बिन्दु है। चेहरे को दिल का आइना कहा गया है और चेहरे क आइना आँखें होती हैं। इनके द्वारा प्रेषित सन्देश, ग्राही व्यक्ति द्वारा सहजरूपेण ही ग्रहण कर लिए जाते हैं।
2. चेहरे एवं ललाट की अभिव्यक्ति (Expression of Pace and Forehead) हदय के गानों को खरित करने तथा अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला सर्वाधिक सशक्त माध्यम हमारा चेहरा ही होता है। चेहरा व्यक्ति की मनोदशा को स्पष्ट रूप से शब्दों के बिना ही सम्प्रेषित करने की पूर्ण सामथ्य रखता है। दुख, विवाद, प्रसन्नता तथा साम्यावस्या का दिग्दर्शन किसी के चेहरे को पढ़कर किया जा सकता है। चेहरे व ललाट की विभिन्न प्रतिकृतिया। द्वारा अनुभूति, विचार तथा गुण, स्वभाव का सही सूचना के आप में सम्प्रेषण हो जाता है।
शारीरिक भाषा के लाभ
(Advantages of Body Language)
शारीरिक भाषा अशाब्दिक सम्प्रेषण की सहायक भाषा है। शारीरिक भाषा के लाभ निम्नलिखित है___
(1) शारीरिक भाषा का समयानुकूल उपयोग कार्य सम्पादन को अत्यन्त सरल बना देता है। इसकी परिणति व्यवसाय के हित में ही होती है।
(2) शारीरिक भाषा प्राय: शाब्दिक सम्प्रेषण की सहायक अथवा पूरक होती है। यदाकदा इसको विपरीत स्थिति भी हो जाती है। जब अशाब्दिक सम्प्रेषण अति महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक हा ती शारीरिक भाषा की प्रासंगिकता और भी उपयोगी हो जाती है। ___
(3) सम्प्रेषण के क्षेत्र में शारीरिक भाषा, व्यावसायिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रतिविम्वों को ताबाम्बत करती है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी अशाब्दिक भाषा के अनेक लाभ हैं।
(4) शारीरिक भाषा सम्प्रेषण प्रक्रिया को अधिक भावप्रवण बनाती है। हाव-भाव, “मा, आँखों के उचित व प्रभावी प्रयोग या सम्पर्क के अभाव में आमने-सामने का सम्प्रेषण अप्रभावी रहता है।
(5) शारीरिक सम्प्रेषण को ग्राही व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित सम्प्रेषण की अपेक्षा स समझ लेता है। शारीरिक सम्प्रेषण की यह सर्वसुलभता इसके लाभ का एक महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।
शारीरिक भाषा की सीमाएँ
(Limitations of Body Language)
शारीरिक भाषा जब अनेक पहलुओं की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हो जाती है, तब शाब्दिक सम्प्रेषण की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। अनेक अवसरों पर ऐसा भी होता है कि भावभंगिमाओं का वास्तविक सन्देश उसी रूप में ग्राही व्यक्ति तक नहीं पहुँचता, जिस रूप में उसको सम्प्रेषित करने वाला व्यक्ति पहुंचाना चाहता है। कई बार संस्कृति व समाज का प्रभाव भी पड़ता है, अर्थात् एक समाज में किसी शारीरिक क्रिया का अर्थ कुछ होता है तो दूसरे समाज में कुछ और तो ऐसी अवस्था में शारीरिक भाषा द्वारा सम्प्रेषण का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है।
शारीरिक भाषा को प्रभावी बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण बातें
(Important Factors in making Body Language Effective)
शारीरिक भाषा को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बाते निम्नलिखित है
(1) हमें प्रतिदिन की सम्प्रेषण प्रक्रिया में बोलने के लहजे, भावभंगिमा इत्यादि – गतिविधियों पर ध्यान देना होता है। हम जब खड़े रहते हैं तो कन्धों को सीधा, शरीर स्वतन्त्र तथा अपने शरीर के वजन को दोनों पैरों पर सन्तुलित करना हमारे विचारों में दृढ़ता को दर्शाता है।
(2) व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए आँखे महत्त्वपूर्ण व
शक्तिशाली तत्त्व है। यदि आप किसी व्यक्ति की बातो को गम्भीरता से सुन रहे है तो सामने वाले व्यक्ति की आँखों से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।
(3) आधुनिक व्यावसायिक जगत में हाथ मिलाना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यह मिलने वाले व्यक्ति की शक्ति, ऊर्जा व स्थिति को दर्शाता है। कलाई को मोड़कर केवल अंगुलियों को पकड़कर हाथ मिलाना एक गलत संकेत देता है।
(4) अशाब्दिक सन्देश आपके अभ्यन्तर अर्थात् आपकी चेतना व आत्मबल से उठता है। यदि आपको अपनी शारीरिक भाषा को बेहतर व प्रभावी बनाना है तो कार्य को अपने अभ्यन्तर से प्रारम्भ करना चाहिए।
(5) शालीन व विश्वासपूर्ण मुद्रा हमारे व्यवसाय व संगठन के माहौल को बेहतर बनाती है।
(6) शारीरिक भाषा का स्वरूप बहुत कुछ इस बात पर आधारित होता है कि हमारा सम्प्रेषण किस प्रकार के व्यक्ति से हो रहा है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति तथा आयु का शारीरिक भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, अतः सम्प्रेषण किए जाने वाले व्यक्ति की विभिन्न अवस्था का सम्यक् रूप से ध्यान रखते हुए ही हमारा शारीरिक भाषा का सम्प्रेषण होना। चाहिए।
प्रश्न – एक व्यवसाय में पूछताछ के पत्र से क्या आशय है? इसे लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूछताछ प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
What is meant by a Letter of Enquiry in a Business? What point should be kept in mind while writing an enquiry letter ? Discus various steps of enquiry process.
उत्तर – पूछताछ के पार से आशय
(Meaning of an Enquiry Letter)
एक व्यवसाय में पूरता करने से मना । हो सका है। ले। लावतात भारना टेलीफोन द्वारा जानकारी लेना तार जवार जाना हो। आगला ।।।। कतार करना आदि। आजकाल त्यावसायिक ।। ।। द्वारा पत्ता नाराका सा बहत लोकपिय है।
जब किसी व्यापारी को कोई रजाकारी होती है तो खरीद।।। पहले वह विपिन व्यापारियो से उस वस्तु के विषय में पूछताछ रकता है। इस सम्बन्ध में वह जो पत्र भेजता हैं, वह जो पत्र भेजता है, उन पत्रों को ही पूछताछ का पत्र (Enquiry letter ) कहते हैं।
पूछताछ के पत्र का उत्तर जन विक्रेता के पास इस तरह का पहलाता है तो वह पूछतार करने वाले को इतित वस्तु के पूर्ण वितरण का के गाँ।। ((CATopi() जाता है। इसे “पूछताह के पत्र का उत्तर” कहते हैं। परता के उत्तर ।। लिखा जाने वाला यह पत्र अत्यन्त विनस भाषा में होना चाहिए। पर वर्तमान साहको को बनाए रख। एन। पाहक, बनाने में विकय प्रतिनिधि की पमिका निभाते है, अतः विकास की रात के आकर्षक हो। क साथ साथ इस पत्र का उत्तर भी आकर्षक होना चाहिए। क्रेता द्वारा जिवाला के विषय ।। पुलतान की गई है, उनके पूर्ण तथा स्पा’ विवरण दिए जाने चाहिए।
पूछताछ का पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें
(Points to be kept in Mind whilo writing an Enquiry Lotter)
पूछताछ का पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए
1. पूछताछ विशेष होनी चाहिए (Cquiry should be Spacific) पूछताछ करने वाले को अपने पत्र में उन सभी बातों को स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए, जिनके विषय में वह पूछताछ करना चाहता है। उसे अपनी शतों को भी स्पष्ट कर देना चाहिए जैसे यदि कोई ग्राहक बैंक से ऋण लेना चाहता है तो उसे ऋण की राशि तथा ऋण के लिए आवश्यक जमानत इत्यादि के विषय में स्पष्ट रूप से पूछताछ करनी चाहिए।
पूछताछ सम्बन्धी पत्र की शुरुआत प्रत्यक्ष प्रश्न से की जानी चाहिए जैसे “कृपया हमें सूचित कीजिए कि आप निम्नलिखित माल की पूर्ति कर सकेंगे या नहीं।”कि इस रूप में- “हमें निम्नलिखित माल की आवश्यकता है तथा हमने सोचा कि हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप माल की पूर्ति कर सकते हैं अथवा नहीं।” इस प्रकार घुमा फिराकर पूछताछ करने से आपके पत्र का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। . 2. पिछले व्यवहारों का विवरण (Details of Post.transactions)- यदि पूछताछ करने वाली संस्था को किसी बैंक से पूछताछ करनी है और उसके बैंक के साथ पुराने लेन-देन हों तो उसे इनका भी विवरण दे देना चाहिए। इससे बैंक को पिछले रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। उदाहरणार्थ-यदि पूछताछ करने वाले के पास पहले से ही १ 50 लाख का अधिविकर्ष है तथा वह उसे बढ़वाकर ₹ 80 लाख कराना चाहता है तो उसे पतमान अधिविकर्ष के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देते हुए आगे के लिए अधिविकर्ष बढ़ाने के सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाहिए।
3. पूछताछ स्पष्ट होनी चाहिए (Enquiry should be Clear)–यदि पूछताछ स्पष्ट नहीं है तो दूसरा पक्ष इसे महत्त्व न देकर भुला सकता है अथवा उसे स्पष्टीकरण हेत दुबारा लिखना होगा। पूछताछ के पत्र की शैली सरल होनी चाहिए तथा पूछताछ करने वाले व्यक्ति को अपनी सभी आवश्यकताओं को स्पष्ट कर देना चाहिए। उदाहरणार्थ-यदि कोई व्यक्ति लघु उद्योग प्रारम्भ करने हेतु बैंक से ऋण चाहता है तो उसे पूर्ण विवरण बनाकर देना होगा कि वह ऋण की राशि को कहाँ-कहाँ और कैसे प्रयोग करेगा इत्यादि।
4. प्रारम्भिक पूछताछ को विशेष रूप से स्पष्ट करना (Preliminary Enquiry should be Specifically disclosed)-कभी-कभी ग्राहक प्रारम्भिक पूछताछ भी कर सकता है। इस पूछताछ का उत्तर पाने के बाद वह निर्णय ले सकता है कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। यदि वह केवल प्रारम्भिक पूछताछ ही कर रहा है तो उसे ऐसा लिख देना चाहिए कि पूर्ण विवरण वह बाद में देगा। उदाहरणार्थ-यदि कोई कृषक ट्रैक्टर खरीदने हेतु किसी व्यावसायिक बैंक से ऋण लेना चाहता है, परन्तु उसे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है तो वह बैंक से प्रारम्भिक जानकारी इस प्रकार कर सकता है-आप किस प्रकार कृषि ऋण प्रदान करते हैं? हम ₹ 3,00,000 का ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक हैं। यदि यह आपकी बैंक ऋण योजना के अन्तर्गत आता है तो हमें जानकारी दें। हम अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण आपका उत्तर प्राप्त होने के बाद भेज देंगे।
5. यदि संस्था आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती तो उससे विकल्पों के विषय में पूछिए (Ask for alternatives if the firm cannot meet your requirements)–यदि आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज के विषय में आप पूछताछ कर रहे हैं, संस्था उसकी पूर्ति नहीं कर सकती तो आप संस्था से पूछ सकते हैं कि फिर इसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ-एक ग्राहक अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलना चाहता है। कुछ विदेशी बैंक मुद्रा विनिमय का व्यवसाय करते हैं और कुछ नहीं करते। यदि वह बैंक, जिससे पूछताछ की जा रही है, इस स्थिति में नहीं है कि वह इस कार्य को कर । सके तो वह यह बता सकता है कि ग्राहक विदेशी मुद्रा कहाँ से प्राप्त करे।
6. विनम्र भाषा (Humble Language)-पूछताछ के पत्र में विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
7. दोहराव न हो (No Repetition)-एक ही बात को बार-बार नहीं दोहराना – चाहिए।
8. पूर्ण विश्वास (Full Confidence)—पूछताछ के पत्र को पूर्ण विश्वास के साथ। लिखना चाहिए।
पूछताछ प्रक्रिया
(Enquiry Process)
पूछताछ प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं-1. योजना – विशेष के सम्बन्ध में पूछताछ (Enquiry regarding the Specifics Scheme)-बैंकों द्वारा समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों के लाभार्थ विभिन्न योजना चलाई जाती हैं; जैसे- “Own your House Scheme” अथवा “Retirement Benefit Scheme” आदि। बैंक अपनी योजनाओं का विज्ञापन समाचार-पत्रों या पोस्टरों के माध्यम से
करते है। पूछताछ करने वाले व्यक्ति को उस योजना-विशेष के सम्बन्ध में स्पष्ट कर देना चाहिए, जिसके विषय में वह जानना चाहता है।
उदाहरण – मैंने आज के ‘नवभारत टाइम्स’ समाचार-पत्र में पढ़ा कि आपने एक नई योजना “Own Your House Scheme” प्रारम्भ की है। मैं इस योजना में सम्मिलित होने में रुचि रखता हूँ; अत: आपसे निवेदन है कि आप सभी आवश्यक सूचनाएँ भेजें।
2. प्रारम्भिक परिचय (Introduction)-पत्र के प्रारम्भिक अनुच्छेद में पूछताछ करने वाले को अपना परिचय देते हुए यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह फर्म है या व्यक्ति।
उदाहरण“हमारी फर्म इस कस्बे में साड़ियों का व्यवसाय करने वाली अकेली फर्म है। हमारा वार्षिक व्यवसाय ₹ 30 लाख का है।” अथवा “मैं एक स्नातक बेरोजगार व्यक्ति हूँ तथा मैं अपना उद्योग प्रारम्भ करना चाहता हूँ।”
3. यदि कोई अन्य सन्दर्भ हों तो उनका भी वर्णन करना चाहिए (If there are any other references, mention them)—यदि आप देख रहे हैं कि बैंक की स्कीम से कुछ लोग लाभ उठा रहे हैं और आप बैंक से जानना चाहते हैं कि क्या बैंक के पास ऐसी कोई योजना है, जिससे आप भी अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें तो आपको अपनी पूछताछ में उन । व्यक्तियों का वर्णन कर देना चाहिए, जो बैंक की इस प्रकार की योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं।
उदाहरण– “मेरे चचेरे भाई ने हाल ही में काफी मात्रा में घरेलू सामान खरीदा है तथा उसका कहना है कि इस प्रकार का सामान क्रय करने हेतु बैंक ने ऋण योजना प्रारम्भ की हई है। क्या आप कृपा करके इस स्कीम की पर्याप्त सूचना हमें देंगे?’
4. सूची-पत्र, विवरणी पुस्तिका आदि के विषय में पूछना (Asking for Catalogue, Brochure etc.)-जब आपको बैंक से सूची-पत्र या बुकलेट लेनी हो तो उस समय अपने विषय में पूर्ण सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सबके विषय में तो आप पोस्टकार्ड से भी पूछ सकते हैं। इस स्थिति में आपको अपना पूरा पता, फोन नम्बर या टेलेक्स नम्बर, यदि कोई हो तो देना चाहिए। ___अधिक अच्छा होगा यदि आप पत्र में उस स्कीम का नाम भी लिख दें जिसमें आपकी रुचि हो।
उदाहरण—“कृपया क्या आप लघु उद्योगों पर कोई बुकलेट हमें भेजने का कष्ट करेंगे? मैं ₹ 10 की पूँजी से बियरिंग (Bearing) निर्माण की इकाई प्रारम्भ करने में रुचि रखता हूँ।”
5. विवरणों के लिए पूछना (Asking for Details)-आप जिस योजना के विषय म पूछना चाहते हैं, उसके विषय में आपको अपना परिचय देकर योजना के विवरणों के विषय में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ___उदाहरण-“आज के ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ समाचार-पत्र से पता चला है कि आपने उच्च शिक्षा ऋण योजना’ निकाली है। मैं राँची यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूं। मैं इसमें परास्नातक करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बताएँगे कि मेरे लिए कितनी सश स्वीकृत हो सकती है? ब्याज की दर, पून: भुगतान का माध्यम तथा जमानत की राशि
क्या होगी?”
6. अन्तिम (Closing)-पूछताछ को बन्द करने के लिए केवल धन्यवाद काफी है। हम यह भी प्रयोग कर सकते हैं
(1) “आपका शीघ्र उत्तर प्रशंसनीय होगा।”
(ii) “हम दीपावली पर पर्याप्त मात्रा में माल रखना चाहते हैं, यह हमारे लिए अत्यन प्रशंसनीय बात होगी यदि आप शीघ्र उत्तर दें।”
(ii) “आपको ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे निकट भविष्य में उत्तर की आशा है।”
प्रश्न – साक्षात्कार क्या है? इसे प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?
What is Interview ? How can it be made effective ?
अथवा साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार के गुण व प्रकार लिखिए। इसे कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है?
उत्तर –
What is Interview? Wat down the merits and types of Interview. How can it bepade e Nective ?
साक्षात्कार से आशय
Meaning of Interview
वी० एम० पामर के शब्दों में, “दो व्यक्तियों के बीच पायी जाने वाली वह विशा सामाजिक स्थिति. जिसमें दोनों व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत परस्पर उत्तर-प्रत्युत्तर करते हैं, ‘साक्षात्कार’ कहलाती है।”
एच० पी० यंग के शब्दों में, “क्षेत्रीय कार्य की वह विशेष तकनीक, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, उनके कथन को लिखने व सामाजिक य समुदाय को अन्तक्रिया के स्पष्ट परिणामों के अध्ययन हेतु किया जाता है, ‘साक्षात्कार कहलाती है।”
वास्तव में साक्षात्कार सम्प्रेषण की एक अति विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें साक्षात्कार के तथ्यों का संकलन होता है। इसमें दो व्यक्ति अथवा पक्ष आमने-सामने की स्थिति में होक निश्चित विषय पर बातचीत करते हैं। इसमें लम्बी प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर-प्रत्युत्तर की क्रिया चलती रहती है।
साक्षात्कार के गुण
(Merits of Interview)
साक्षात्कार विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आयोजित किए जाते हैं, परन्तु विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार के लिए विभिन्न गुण होते हैं, जो निम्नलिखित हैं
(1) साक्षात्कार की प्रक्रिया में सदैव दो पक्षों का होना आवश्यक है। इनके मध्य विचार का आदान-प्रदान होता है।
(2) साक्षात्कार पूर्व नियोजित होता है, अत: दोनों पक्ष इसके लिए मानसिक व भौति रूप से तैयार होते है।
(3) साक्षात्कार का विशिष्ट गुण है कि उसमें अवलोकन की क्रिया अति विशिष्ट रूप की जा सकती है।
(4) सभी साक्षात्कार पूर्व विधारित होते हैं तथा इनका उद्देश्यपरक होना नितान्त आवश्यक होता है।
(5) दोनों पक्षों के लिए सम्प्रेषण पटना की तैयारी या पूर्व अभ्यास आवश्यक होता है। यह औपचारिक सम्प्रेषण का एक हिस्सा होता है।
साक्षात्कार के प्रकार
(Kinds of Interview)
साक्षात्कार को निम्नलिखित जात श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है
(i) रोजगार सम्बन्धी साक्षात्कार, (ii) उन्मुखीकरण, (iii) काउन्सिलिंग साक्षात्कार, (iv) शिकायत सम्बन्धी साक्षात्कार, (v) अर्थ निष्पादन सम्बन्धी साक्षात्कार, (vi) संशोधन सम्बन्धी साक्षात्कार, (vii) निर्गग सम्बन्धी साक्षात्कार, (viii) सूचना-संग्रह सम्बन्धी साक्षात्कार।
साक्षात्कार को प्रभावी बनाने हेतु दिशा-निर्देश
(Guidelines for an Impressive Interview)
साक्षात्काररूपी परीक्षा, परीक्षार्थियों तथा परीक्षक के मध्य वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करती है। परीक्षक साक्षात्कार के माध्यम से यह जानने का प्रयास करता है कि आवेदक की विषय के प्रति समझ, आधिकारिकता एवं जानकारी क्या है। वास्तव में साक्षात्कार देना एक कला है, अत: साक्षात्कार परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर परीक्षार्थियों को साक्षात्कार परीक्षा सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं। साक्षात्कार देते समय परीक्षार्थियों को इन महत्त्वपूर्ण सुझावों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए
(1) परीक्षार्थी को अपने मन में परेशानी, चिन्ता एवं घबराहट की भावना नहीं पनपने देनी चाहिए।
(2) साक्षात्कार परीक्षा देते समय मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होनी चाहिए। ऐसे समय नकारात्मक सोच हानिकारक हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि साक्षात्कार से ठीक पहले तक पढ़ते न रहें बल्कि अपने साथियों से सामान्य बातें भी विषय को छोड़कर करते रहें। ऐसी कोई भी क्रिया न करें जिससे मन में तनाव की अवस्था उत्पन्न होती हो।
(3) साक्षात्कार देने जाते समय अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य ढंग से पहने गए कपड़ों का विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। ऐसे मौके पर भड़कीले वस्त्रों के मोह से बचना चाहिए।
(4) साक्षात्कार-कक्ष में प्रवेश करते समय “May I come in Sir/Madam” का सम्बोधन करना चाहिए तथा जब सकारात्मक उत्तर मिले, तब ही कक्ष में प्रविष्ट होना चाहिए और परीक्षक या परीक्षकों का उचित अभिवादन; जैसे-नमस्ते, Good Morning या Good Afternoon Sir/Madam (समय के अनुसार) आदि करना चाहिए तथा आवेदक को आभवादन थोड़ा झुककर सादगीपूर्ण मुस्कराहट के साथ करना चाहिए।
(5) साक्षात्कार समिति के किसी सदस्य द्वारा बहने के लिए कहे जाने पर ही अपवा ज्ञापित करते हुए जैतमा उचित रहता है। यदि परीक्षक का ध्यान कहीं और है और वह भापकी बैठने के लिए नहीं कहता है तो समता से परीक्षक को सबोधित करते हुए कहा चाहिए- “Sir Madanक्या मैं बता सकता हूँ?’ उनके, “हाँ” कह । पर “धन्यवाद” कहते हुए सादगीसेट जाइए।
(6) साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अपनी जानकारी के अनुसार सही उत्तर देना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर दात न हो तो झुट का सहारा कदापि न ले।
(7) साक्षात्कार समिति के समक्षा पहुंचने से पूर्व, परीक्षार्थी को आत्मविश्वास नहीं खोला चाहिए। कक्ष में पहुँचने के बाद तथा पश्नों के उत्तर देते समय परीक्षार्थी को इस आत्मविश्वास को पूरी तरह बनाए रखना चाहिए। साक्षात्कार परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास परमावश्यक है, इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। परीक्षार्थीको कभी भी अपने मन में शंका नहीं रखनी चाहिए।
(8) सौम्य व आदरपूर्ण व्यवहार किए जाने पर सभी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही बात चयन समिति के समक्ष भी खरी उतरती है।
(9) प्रश्नों का उत्तर न जानने की अवस्था में निराश नहीं होना चाहिए अपित सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुकूल करने की चेष्टा करते रहना चाहिए।
(10) प्रश्नोत्तर काल में प्रश्नोत्तरों की भाषा सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होनी चाहिए। अच्छा तो यह होता है कि परीक्षक आपसे जिस भाषा में प्रश्न पूछे उसका उत्तर उसी भाषा में दें किन्तु यदि ऐसा आपके लिए सम्भव नहीं है तो आप किसी भी भाषा में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उत्तर धाराप्रवाह होना चाहिए।
(11) परीक्षार्थी को साक्षात्कार देते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भली-भाँति सुने और उनका समुचित उत्तर दे। परीक्षार्थी यदि प्रश्न को ठीक प्रकार से सुन व समझ नहीं पा रहा है तो परीक्षार्थी को-“क्षमा कीजिए श्रीमान, प्रश्न को दोबारा बोलने की कृपा करें”-कहना चाहिए।
(12) परीक्षार्थी को प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देना चाहिए कि परीक्षक उसकी जानकारी वाले विषय से सम्बन्धित प्रश्नों पर ही आ जाए। इसको अपने अनुकूल करने की अवस्था कहा जाता है। कई बार साक्षात्कार देने का अनुभव होने पर इस अवस्था की स्वयमेव ही प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार परीक्षक उसी विषय पर प्रश्न पूछेगा, जिसमें परीक्षार्थी की रुचि है, अर्थात् परीक्षार्थी को अपनी रुचि के प्रश्न पूछने के लिए परीक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए।
(13) प्रश्न का उत्तर आवश्यक, अनुकूल, संक्षिप्त, तर्कपूर्ण एवं प्रभावशाली हान चाहिए। प्रश्न का उत्तर अनावश्यक रूप से बढ़ाने का प्रयास कदापि न करें, अन्यथा आपक उत्तर में से अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
(14) जब आपका साक्षात्कार समाप्त हो और परीक्षक आपसे कहे.-“अच्छा, अब आप जा सकते हैं, धन्यवाद”, तब आप सादगी से उठकर तथा थोड़ा झककर समस्त उपस्थितगणों का अभिवादन करते हुए, Thank you Sir/Madam का सम्बोधन करते
कक्षा से बाहर जाएँ। ध्यान रहे कि स्थान छोड़ते समय अपनी पीठ तुरन्त परीक्षक की ओर न करें तीन कदम पीछे हटकर बिना किसी प्रकार की आवाज किए बाहर आएँ।
प्रश्न – लेखन कुशलता से क्या अभिप्राय है? एक लेखन को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है?
What is meant by Writing Skill ? Discuss how writing can be made effective?
उत्तर – लेखन कुशलता/दक्षता
(Writing Skill/Ability)
प्राचीनकाल से ही लेखन कला का मानवीय जीवन में विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीनतम लेखन के प्रमाण आर्य मनीषियों की रचनाओं में परिलक्षित होते हैं। वर्तमान समय में यूरोपियनों ने इस विधा को पुष्पित व पल्लवित किया तथा इसको ऊर्ध्वगामी बनाया। आज के वैज्ञानिक युग में लेखन शैली तथा इसकी उपादेयता दिनोदिन बढ़ती जा रही है। कम्प्यूटर के इस युग में भी लेखन दक्षता को समाज तथा व्यवसाय जगत में विशिष्टता प्राप्त है। लेखन के द्वारा हम किसी कथन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्रमाण के रूप में भी लिखित सामग्री को स्वीकार किया जाता है।
लेखन कुशलता के निम्नलिखित चार चरण होते हैं
(1) नियोजन, (2) प्रथम प्रारूप लेखन, व्यावसायिक सम्प्रेषण-लेखन कुशलता/दक्षता एवं आवेदन-पत्र, (3) संशोधन तथा (1) सम्पादन।।
लेखन कुशलता के प्रथम चरण अर्थात् नियोजन के अन्तर्गत निम्नलिखित पाँच बातें समाहित होती हैं-(i) उद्देश्य, (ii) श्रोता विश्लेषण, (iii) विचारों का चयन, (iv) विचारों के अनुकूल आँकड़ो व तथ्यों का एकत्रीकरण तथा (v) सन्देश को व्यवस्थित क्रम प्रदान करना।
नयोजन के पश्चात् द्वितीय चरण के रूप में लेखन का ‘ड्राफ्ट’ (प्रथम प्रारूप) तैयार किया जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विचारों को स्थान दिया जाता है। इसमें विभिन्न पहलुओं का समाहार होता है। मुख्य विचार के समर्थन व उससे सम्बन्धित अनुकूल तथ्यों व उदाहरणों का चयन किया जाता है। प्रथम प्रारूप लेखन की निम्नलिखित दो शैलियाँ होती हैं-(i) रेखीय एवं (ii) चक्रीय।
रेखीय शैली में एक तथ्य के पश्चात् दूसरा तथ्य क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है, जबकि चक्रीय शैली में विचारों की प्रस्तुति व व्यवस्था अत्यधिक लचीली होती है। प्रथम ड्राफ्टिग में सर्वप्रथम मुख्य सूचना को प्रथमत: कागज पर लिखा जाता है, जो कि सम्पूर्ण सन्देश का एक प्रमुख अंश होता है।
तृतीय चरण में बनाए गए ड्राफ्ट (प्रथम प्रारूप) में आवश्यक संशोधन किया जाता है तथा लेखन की सुविधा के अनुसार विषयगत तत्वों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रारूप में उचित परिवर्तन हो जाता है। इसी चरण में व्याकरणसम्मत त्रुटियों का भी निराकरण कर दिया जाता है तथा भाषा को गति व प्रवाह प्रदान किया जाता है।चतुर्थ चरण में लेख को सावधानीपूर्वक पढ़ा जाता है तथा शेष रह गई त्रुटियों को भी लेख से निकाल दिया जाता है। इसी चरण में लेख को प्रभावी स्वरूप प्राप्त होता है। सम्पादन के
द्वारा समस्त नया का लारण हो जाता है और इस रूप में तैयार लेख अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफलीभूत होता है।
प्रभावशाली लेखन के आवश्यक तत्व
(Essentials for Effective Writing)
(1) एक प्रभावशाली लेखा के लिए, लिखने से पूर्व निम्नलिखित कुछ बिन्दुओं पर मनन किया जाना आवश्यक होता है…
(i) बयों लिखें,
(ii) किसके लिए लिखें,
(iii) क्या लिखें,
(iv) कैसे लिखे।
(2) लेखन में सदैव सारगर्भित शब्दों व वाक्यों का ही प्रयोग उचित रहता है। ऐसा करने से लेखन को स्पष्टता तो झलकती ही है, विचारों का प्रस्फुटन भी ओजस्वी रूप से पाठक के हृदय में होता है।
(3) विषय वस्तु के अनुरूप ही लेखन का प्रणयन किया जाना चाहिए। ___(1) लेखन वास्तविक जगत से सम्बन्धित होना चाहिए तथा उसकी विश्वसनीयता
असंदिग्ध होनी चाहिए।
(5) लेखन व्यावहारिक हो। कोई भी श्रोता या व्यक्ति आदेश या उपदेश को पसन्द नहीं करता, अत: लेखन में मानवीयता का समावेश होना चाहिए।
(6) व्यावसायिक लेखन में यह ध्यान दिया जाना परमावश्यक है कि तथ्य वस्तुगत हों, न कि विषयगत। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योकि व्यावसायिक सम्प्रेषण में वस्तुगत लेखन की ही विशिष्टता होती है।
(7) लेखन में अप्रचलित शब्दाडम्बर व अत्यधिक उत्साही भाषा का प्रयोग न करें।
प्रश्न – निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-
(I) समूह चर्चा,
(II) संगोष्ठी।
Write short note on the following:
(I) Group Discussion,
(II) Seminar.
उत्तर – 1) समूह चर्चा
(Group Discussion)
प्रबन्धन संस्थान, नौकरियों की तलाश कर रहे विद्यार्थियों की सम्प्रेषणशीलता या कम्युनिकेटिव जाँच करने के लिए सामूहिक परिचर्चा के सशक्त माध्यम हैं। आज के प्रतियोगितात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक युग में विभिन्न सहयोगियों के बीच सम्प्रेषण के महत्त्व को समझते हुए विभिन्न प्रबन्धन संस्थान तथा प्रयत्नकर्ता लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के अलावा सामहिक परिचर्चा परीक्षण का सहारा लेकर योग्य आवेदनकर्ताओं का चयन
करते हैं। अतः स्पष्ट है कि समूह चर्चा में एक सपरया या नीतियों पर जोखिममा काम निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है।
समूह चर्चा के मूल उद्देश्य
(Fundamental Objectives of the Group Discussion)
दो व्यक्तियों के मध्य जो वार्तालाप का संचार होता है, उस विणि कोणाल का सरला का समावेश कर वार्ता को तर्कसंगत रूप प्रदान किया जा सकता है। एस) का सर कोपाल कहा गया है। आदिकाल से ही मानव का दूसरे मानव के साथ यह बातो कोणाला जारी है। सभ्यता के दौर में इस कौशल ने नए आयामों का स्पर्श किया है। शिHिI, यि , पति-पत्नी, मालिक-नौकर के बीच विचार विमर्श ही वातालाप है। यह साड़ी का जीना है, वक्ता-श्रोता के बीच सहमति है। वक्ता सदैव श्रोता की मन स्थिति, पिपति और छाया का अनुरूप ही अपनी बातें रखता है। श्रोता उठने लगे, कतराने लगे, अनायास नरकी ले। लाता वक्ता असफल है। श्रोता से तालमेल बैठाकर ही विचार विनिमय के गूल उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। अध्ययन की दृष्टि से समूह चर्चा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं
(1) समूह चर्चा का लक्ष्य विचारों/आदर्शों की प्रस्तुति व इस सालमा प्रतिक्रियामा का प्राप्त करना होता है जिससे आगे की जिज्ञासा प्रकट होती है, जो पुनः प्रश्न और प्रतिप्रश्न पूछ । का निमित्त बनती है।
(2) समूह चर्चा में विभिन्न रचनात्मक विचारों के द्वारा समस्या का सम्यक निदान केन्दा जाता है।
(3) निर्णय प्रक्रिया में विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, अतः सगृह चर्चा में इन विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। इस प्रकार की समूह चर्चा के लिए पटव रचनात्मक भाषा होती है।
समूह चर्चा के समय अपनाया जाने वाला आचारशास्त्र
(Behaviour to be Adopted at the Time of Group Discussion) __
मूह चर्चा श्रम की विशिष्टता को जन्म देती है क्योंकि इसमें एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विषयों में पारंगत व्यक्ति अपने अनुभवों, विचारों, आदर्शों के माध्यम से सहयोग देते हैं। समूह चर्चा में भाग लेने वाले व्यक्तियों का विशेष महत्त्व होता है, अत: इसके सहभागी सदस्यगणों की उपादेयता असंदिग्ध है। इनकी निश्चित सोच का अनुगामी होने से विश्वसनीयता को बढ़ाने में सफलता प्राप्त होती है। समूह चर्चा में प्राय: निम्नलिखित कार्य-व्यापार को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है
(1) कृत्यक आचरण (Task Behaviour)
(2) अनुरक्षण आचरण (Maintenance Behaviour)
(3) आत्मनिर्देशित आचरण (Self-directed Behaviour)1. कृत्यक आचरण (Task Behaviour) – इसमें उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण, ज्ञान-स्रोतों का विश्लेषण, समस्याओं को परिभाषित करना, प्रस्तावों का निर्माण, सफलता की कसौटियों की स्थापना, हल को परिभाषित करना, अच्छे हल के लिए स्वीकृति, प्रस्तुति, मूल्यांकन व संक्षिप्तीकरण सम्मिलित होता है।
2. अनुरक्षण आचरण (Maintenance Behaviour)-अनुरक्षण आचरण में भागी इस चर्चा में कैसा महसूस कर रहे हैं इस बात को जाना जाता है। इसमें बैठक को कैसे प्रबन्धित करना है, कौन किसको प्रभावित करता है, कौन किससे बात करता है, कोन हिस्सा ले रहा है, कौन और क्यों, एक-दूसरे के प्रस्ताव का समर्थन, सुरक्षा, प्रोत्साहन, तनाव को कम करना व प्रतिपुष्टि (Feedback) देना समाहित होते हैं।
3. आत्मनिर्देशित आचरण (Self-directed Behaviour)-चर्चा के दौरान उद्देश्यों की प्राप्ति के ढंग का इसके अन्तर्गत विवेचन किया जाता है; जैसे-वार/प्रतिवार सुरक्षात्मक व्यवहार, एक-दूसरे के प्रस्तावों पर असहमति, प्रतियोगिता की पहचान या स्वीकृति. सहभागिता की अस्वीकृति इत्यादि इसमें समाहित होते हैं।
एक सफल समूह चर्चा की अनिवार्य शर्ते
(Essential Conditions for a success Group-discussion) __
(1) समूह चर्चा में सम्मिलित व्यक्तियों को चर्चा के उद्देश्य/लक्ष्य के प्रति जागरूक रहकर उसके अनुकूल क्रियाशील रहना चाहिए।
(2) समूह चर्चा में इस प्रकार का वातावरण निर्मित होना चाहिए कि प्रत्येक विचार। आदर्श को अनुकूल व रचनात्मक आलोचनाओं के साथ सुना जाए व प्रोत्साहित किया जाए।
(3) एक समूह चर्चा विभिन्न रुचि व कुशलता वाले व्यक्तियों के विचारों/आदर्शों के संयोजन द्वारा होनी चाहिए।
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सामूहिक चर्चा का व्यावसायिक सम्प्रेषण के क्षेत्र में अति विशिष्ट स्थान निर्धारित हो चुका है। किसी भी व्यावसायिक संगठन की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपादेयता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
संगोष्ठी
(Seminar)
संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का वितरण एवं समान ज्ञानी सदस्यों के मध्य अपने-अपने विचारों के प्रस्तुतीकरण से है। सामान्यतः वक्ता एक विशिष्ट विषय पर अपने ज्ञान को विस्तारित कर अपने विचार प्रस्तुत करता है। अन्य सहभागी सदस्य वक्ता के वक्तव्य पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त वाद-विवाद भी करते हैं।
संगोष्ठी को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है—“संगोष्ठी चर्चा का एक छोटा समूह होता है, जिसके अन्तर्गत किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित शोध/अनुसन्धान या अन्य अध्ययन को मौखिक या लिखित रूप में प्रकट किया जाता है।”
सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री को यथास्वरूप ग्रहण करने में संगोष्ठी विशेष भूमिका का निर्वहन करती है। संगोष्ठी के द्वारा सरलीकरण की प्रक्रिया को मूर्तता प्रदान की जाती है। यह शोध-पत्रों, संक्षेपणों तथा सुझावों को व्यक्त व स्पष्ट करने में सहायक होती है। इसमें शोध-पत्रों, संक्षेपणों व सुझावों को एक प्रकाशित रिपोर्ट के स्वरूप में वृहत् रूप से वितरित किया जाता है। संगोष्ठी मौखिक सम्प्रेषण की एक प्रभावशाली प्रक्रिया या विधि है। इसका एक पहलू विचारों/अनुभवों का उचित आदान-प्रदान होता है।
संगोष्ठी के लक्षण
characteristics of Seminar)
संगोष्ठी के मूलभूत लक्षणों की चर्चा निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है(1) संगोष्ठी के लिए विषय का चयन अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाता है तथा य-विशेष की महत्ता को अक्षुण्ण रखा जाता है। संगोष्ठी की चर्चा में आने वाले बिन्दुओं का वर्धारण पूर्व में ही सुनियोजित ढंग से कर लिया जाता है।
(2) संगोष्ठी में प्रायः विचारों का आदान-प्रदान मौखिक रूप में ही फलदायी होता है, अत: संगोष्ठी एक मौखिक व्यावसायिक सम्प्रेषण है। ___
(3) संगोष्ठी में विषय-विशेषज्ञों का एकत्रित होना तथा उनके द्वारा सारभूत व्याख्यान से निकली विचारमाला सार्थक निष्कर्षों व सुझावों के रूप में परिलक्षित होती है।
(4) छोटे समूह में अनेक विशेषज्ञों का आमने-सामने वार्तालाप होता है, जिससे सारभूत निष्कर्ष की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। ____
प्रश्न -“एक व्यावसायिक पत्र इतना प्रभावी होना चाहिए कि जिस सीमा तक सम्भव हो, लेखक का भी स्थान ले सके।” वर्णन कीजिए।
“A business letter should be so effective that it can take the place of the writer as far as possible.” Discuss.
व्यावसायिक पत्र का आशय
(Meaning of Business Letter)
व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाने वाला पत्रों का आदान-प्रदान ‘व्यावसायिक पत्र व्यवहार’ कहलाता है और ऐसे पत्रों को व्यावसायिक पत्र’ कहते हैं। आधुनिक युग में व्यावसायिक पत्र निश्चित रूप से एक अपरिहार्य आवश्यकता का रूप ग्रहण कर चुके हैं। किसी-न-किसी रूप में तथा कभी-न-कभी व्यावसायिक पत्रों के आदान-प्रदान की आवश्यकता प्रत्येक व्यवसायी तथा उद्यमी को पड़ती है। अपने नियमित कार्य को करने हेतु व्यवसायी को विभिन्न पक्षों से सूचनाओं का आदान-प्रदान करना पड़ता है। पूछताछ करने के लिए, आदेश प्रेषित करने के लिए, आदेशों को पूरा करने के लिए, साख की अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, देनदारों को उनके खातों का विवरण भेजने के लिए, माल की पूर्ति में की गई कमी की शिकायत के लिए, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा फर्म की ख्याति में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक संस्था में सम्प्रेषण की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक पत्रों के उचित माध्यम व सम्प्रेषण के द्वारा ही उद्योग जगत में फैले विशाल जनसमुदाय से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। भौगोलिक दूरी की प्राकृतिक बाधा को व्यावसायिक पत्रों के द्वारा सहजरूपेण ही पार कर लिया जाता है।
व्यावसायिक पत्र का महत्त्व
(Importance of a Business Letter)
आधुनिक व्यापार की सफलता काफी सीमा तक व्यावसायिक पत्र-व्यवहार पर भी भर करती है। हरबर्ट एन० केसन के अनुसार, “एक श्रेष्ठ पत्र उस मास्टर-चाबी के समान
होता है जो ताला लगे दरवाजे को भी खोल देती है। यह बाजार का निर्माण करता है वस्तुओं व सेवाओं के विक्रय हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा पत्र फर्म का चित्र । करता है।”
व्यावसायिक पत्र अपने श्रेष्ठ रूप में व्यवसाय में अन्तर्निहित उद्देश्य को प्राप्तकर्ता पहुँचाने में कारगर सिद्ध होता है। सुदूर क्षेत्रों में स्थित लोगों तक इस पत्र के द्वारा ही प्रतिशत ख्याति पहुँचती है। अच्छे व्यावसायिक पत्रों के द्वारा फर्म की ख्याति स्थायित्व को करती है। वास्तव में एक व्यावसायिक पत्र इतना प्रभावी होना चाहिए कि जिस सीमा तक सार हो, लेखक का भी स्थान ले सके।
व्यावसायिक पत्र लिखने के कारण/आवश्यकता
(Reasons/Need to write a Business Letter)
एल० गार्टसाइड ने व्यावसायिक पत्रों को लिखने के चार मुख्य कारण बताए हैं । निम्नलिखित हैं-
(1) व्यक्तिगत सम्बन्ध के बिना सम्प्रेषण का सरल व आर्थिक साधन उपलब्ध कराना। (2) सूचना प्रदान करना। (3) व्यवहारों के प्रमाण प्रदान करना।
(4) भविष्य के सन्दर्भ हेतु रिकॉर्ड प्रदान करना।
व्यावसायिक पत्र के लाभ/कार्य
(Advantages/Functions of a Business Letter)
एक व्यावसायिक पत्र के लिखे जाने के अनेक दूरगामी लाभ (कार्य) होते हैं
1. रिकॉर्ड एवं सन्दर्भ (Record and Reference)–सम्प्रेषण को भविष्य में रिकॉर्ड में रखने के लिए इसका लिखित में होना अनिवार्य है। इसके लिए व्यावसायिक पत्र एक उत्तम माध्यम है। लिखित सम्प्रेषण को सम्बन्धित व्यक्तियों व विभागों तक सरलता से पहुँचाय जा सकता है। इसका प्रभाव स्थायी होता है। दूसरी ओर यदि मौखिक सम्प्रेषण को अपनाय जाता है तो लिखित सम्प्रेषण की भाँति इसके मूल रूप को एक-दूसरे तक नहीं पहुँचाया जा सकता। इसमें अनावश्यक रूप से समय की बरबादी होगी एवं कार्य में देरी होगी। व्यावसायिक सम्प्रेषण में केवल चालू सन्दर्भो की ही नहीं वरन् पिछले सन्दर्भो की भी आवश्यकता पड़ती है। और इस हेतु व्यावसायिक पत्रों का आदान-प्रदान उद्यम का लाभकारी पक्ष प्रस्तुत करता है। लिखित पत्र होने से पिछले व्यवहारों, अनुबन्धों का ज्ञान, ग्राहकों व विक्रेताओं से किए गएदपत्र-व्यवहारों की जानकारी सरलता, शीघ्रता व शुद्धता से हो जाती है।2. भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही हेतु ठोस आधार (An Authoritativek Proof for Future Reference)-लिखित पत्र हमारे भविष्य एवं वर्तमान के लिए विश्वसनीय प्रमाण होता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी तथ्य के सम्बन्ध में यह कहे व ऐसा नहीं है तो पत्र निकालकर प्रमाण दिया जा सकता है और यही व्यावसायिक पत्र का सर्वाधिक मुखर लाभ है। कानूनी दाँव-पेंचों में भी व्यावसायिक पत्रों को ‘प्राइमरी एवीडेन्स रूप में मान्यता प्राप्त है।
3. विस्तृत फलकों पर प्रभाव का लाभकारी पक्ष (Widening the approach) -किसी भी व्यवसाय के लिए यह बहुत कठिन होता है कि प्रत्येक स्थान पर वह प्रतिनिधि भेजे। विभिन्न स्थानों की दूरी अधिक होने के कारण यह सम्भव नहीं हो पाता है। थति में केवल पत्र ही एक ऐसा माध्यम है, जिसे जहाँ चाहे भेज सकते हैं। पत्रों के म से व्यवसाय के क्षेत्र का भी विस्तार होता है। इन पत्रों की पहुंच विश्व या समस्त डल पर होने के कारण इनकी उपादेयता स्वयंसिद्ध है।
4. व्यावसायिक पत्र मधुर व्यावसायिक सम्बन्धों का प्रणेता (Business Letters hingaSource of Good Relations)-व्यावसायिक पत्र का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अन्य स्याओं के साथ मित्रता बढ़ाना होता है। पत्र के माध्यम से हमेशा के लिए अच्छे सम्बन्ध बनाए जा सकते हैं। पत्राचार के मुख्य उद्देश्य हैं-कम्पनी व ग्राहकों के मध्य सम्बन्ध बनाना, विद्यमान ग्राहकों जबनाए रखना, नए ग्राहक बनाना तथा ग्राहकों को नए-नए उत्पाद अधिक मात्रा में खरीदने के लिए आमन्त्रित करना आदि। इसी से फर्म की ख्याति को बढ़ावा मिलता है। इनके सफल नियोजन से अवसायगत क्षेत्रों में नाना प्रकार के लाभों का आस्वादन किया जा सकता है। __
5. दीर्घकालीन प्रभाव (Making a Lasting Impression)-मुस्पष्ट एवं मधुर कलेवर में लिखे गए पत्रों का प्राप्तकर्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव निश्चित रूप से दीर्घकालीन प्रवृत्ति का होता है। किसी भी प्रसंग को पुन: ताजा करने के लिए पुराने पत्रों का अवलोकन कर विस्मृत स्मृति को सहज रूप में ही पुनर्जीवित किया जा सकता है।
प्रश्न -जीवनवृत्त सारांश क्या है? एक आदर्श जीवनवृत्त सारांश के तत्त्व बताइए।
What is Resume ? Explain the main elements of an ideal resume ?
अथवा “जीवनवृत्त सारांश का उद्देश्य यह दिखाना है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसकी नयोक्ता तलाश कर रहा है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।
“The objective of the resume is to show that you are the same Jerson which employer is searching.” Comment on the above =tatement.
उत्तर – जीवनवृत्त सारांश का आशय
(Concept of Resume)
करीकुलम विटे (सी० वी०) अर्थात् जीवनवृत्त-सारांश एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, यदि यह प्रभावशाली होगा तो आपको अवश्य ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और यदि यह प्रभावशाली नहीं हुआ तो आपको बिना साक्षात्कार के लिए बुलाए नौकरी veी पात्रता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तर विनवृत्त-सारांश के माध्यम से ही आप अपने को नौकरियों और रोजगार के बाजार में ठीक से पायपित कर सकते हैं। आपका जीवनवृत्त-सारांश एक ऐसा विजिटिंग कार्ड है जिसके द्वारा लात्कार लेने वाले को यह ज्ञात होता है कि आप कौन हैं। जीवनवृत्त-सारांश का उद्देश्य यह (खाना है कि नियोक्ता जिस तरह के आदमी की तलाश कर रहा है वह आप ही हैं और व बखूबी पद की जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं।
जीवनवृत्त सारांश को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि इसके माध्यम से आना नौकरी की तलाश के अभियान में आपको मदद मिले, अर्थात् नियोक्ताओं की आप में जाग्रत हो, वे आपको साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित करें, आप नियोक्ता के सामन बैठकर भी आपको प्रस्तुत कर सके और अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर आपके लिए रोजगार का संभावनाएं बढ़े। जीवनवृत्त सारांश ऐसा होना चाहिए कि किसी भी पद के लिए आवेदन कर वालों की भीड़ में आप अलग ही दिखाई दें। जीवनवृत्त सारांश सावधानी से तैयार किया गया विपणन का औजार है जिसके माध्यम से पूर्व निर्धारित समूह के समक्ष किसी व्यक्ति के किकामा रोजगार के लिए उपयुक्त होने का विवरण संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तैयार की जानक समय इसके दो पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए.-पहला विषयवस्तु और दूसरा प्रस्तुतीकरण जिस जीवनवृत्त सारांश कोई इकबालिया बयान नहीं है जिसमें आप प्रत्येक बात का यथातथ्य प्रस्त करें, आप अपनी कमजोरियों को थोड़ा कम करके अपनी खूबियों को बढ़ा-चढ़ाकर अपने शैक्षिक आपको प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा करना गलत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपके प्रतिद्वतील भी यही सब ही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर अन्तर्वस्तु कमजोर है, अर्थात् आपके पास प्रस्तनापी का करने के लिए कोई विशेष बात नहीं है तो आपका जीवनवृत्त-सारांश अच्छा नहीं बन पाएगा अपनी लेकिन यह भी सत्य है कि अगर जीवनवृत्त सारांश ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया तो आपकी या सारी उपलब्धियाँ धरी की धरी रह जाएंगी।
एक आदर्श जीवनवृत्त-सारांश के प्रमुख तत्त्व
(Main Elements of An Ideal Resume)
1. सज्जा-आपके जीवनवृत्त-सारांश की सज्जा स्पष्ट, युक्तिसंगत और ठीक से समझ द्वितीय में आने वाली होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त खाली स्थान होना चाहिए। इसमें पृष्ठ के चारों ओ विव एक-एक इंच का हाशिया छोड़ना चाहिए। यदि लिखने के लिए अधिक सामग्री हो और स्थान की कमी हो तो हाशिये की चौड़ाई आधा इंच कम भी की जा सकती है। लेकिन इससे और क हाता करने पर कागज लूंस-ठूस कर भरा गया प्रतीत होगा। हाशिये देने से आपके लिए हुए हिस्से के व्या चारों ओर का खाली स्थान नियोक्ता को पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। साथ ही यात नियोक्ता चाहे तो हाशिये की जगह पर अपनी टिप्पणियाँ भी लिख कर सकता है।
2. नाम – जीवनवृत्त-सारांश का प्रमुख और पहले आने वाला शीर्षक नाम ही होता है। 3 यदि इसे लाइन के बीचों-बीच या बाएँ हाशिये की ओर लिखा जाए तो यह सबसे अच्छा जिम्मे लगता है। इसे सामान्य से बड़े अक्षरों और बोल्ड टाइप में लिखा जाना चाहिए।
3. पता और फोन नम्बर – अपना पूरा पता और फोन नम्बर लिखना न भूलें। या माग आपके पास फैक्स नम्बर या ई-मेल का पता हो तो उसे भी जीवनवृत्त-सारांश में अवश्य ।। लिखें। अपने घर का या दफ्तर का फोन नम्बर दोनों ही लिखे जा सकते हैं। ऑफिस का नम्र
सबसे तभी लिखें जब इस बात की पक्की व्यवस्था हो कि भेजा गया संदेश आप तक पहुँच जाएगा।
4. विवरण – जीवनवृत्त सारांश का पढ़ने वाले पर अनुकूल प्रभाव पड़े इसके शरुआत से ही ऐसा सारांश तैयार कर लें जिससे शुरु के कुछ शब्द पढ़कर ही लोगों का आपकी ओर आकर्षित हो जाए। जिन लोगों को किसी कार्य का अनुभव है,
5. शिक्षा दम भाग का उपयोग यह बताने के लिए कोरापलिया लिखे। लेकिन यदि आपके पास कोई ज्यावायिक अनुभव को अनुभव बट ही बताया जाना चाहिण शिक्षा वाले भाग मया का नाममा कायम ने अपनी पढ़ाई पूर्ण की है। वह संध्या किम ज्यानक है, इसका भी उल्लेख को दिलमा या प्रमाणपत्र का नाम और उत्तीर्ण करने का लिखना लपलें। टमार की सम्बन्धित किसी क्षेत्र में नए स्नातक हैं, और परीक्षा आपने अच्छे अंक का माप अंकों का विवरण भी दे सकते हैं। यदि आपने प्रथम मनमाया दयाल की हो तो इसका भी उल्लेख अवश्य करें ताकि नियोक्ता का यान इस पानीजाप) लेकिन यदि आपन द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हो तो अंको का उल्लेख करने की कोई आवायकता नहीं है और इसका विवरण बाद में ही द।
6. अनुभव-जीवनवृत्त-सारांश के लिए अनुभव हृदय और आत्मा की तरह महलपन होता है। इस भाग में आप अपनी उपलब्धिया, अपने द्वारा निभाई जा चुकी जिम्मेदारिया, – व्यक्तिगत कौशल और पट पर कार्य करते हुए अर्जित जान का उल्लेख को अपने अनुभव को कार्य उल्टे क्रम में ही लिखें ताकि इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं और जो भी कार्य सबसे महत्त्वपूर्ण है, वह कार्य सबसे पहले आ जाए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई
अनुभव न हो तो आप इंटर्नशिप, स्वैच्छिक, कार्य, शिक्षणतर गतिविधियों और निभायी गई – जिम्मेदारियों का भी विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं।
7.अन्य गतिविधियाँ-पढ़ाई पूरी करके नए-नए निकले शिक्षार्थियों के लिए गतिविधि भाग अति आवश्यक है। विशेष रूप से उन्हीं गतिविधियों को बताएं जो पटसेसर्वान्चत हो। नियोक्ता के लिए विशेष कौशल का उल्लेख उनकी उपयता के कम ही लिखे। पाषा दक्षता, कण्यटा शॉर्ट हैंडाटाइपिंग और भाषा सम्बन्धी अपनी टपता के स्तर का भी उल्लेखं करें।
जीवनवृत्त-सारांश में अपनी रुचियों का उल्लेख करने का तभी फायदा है जब वे पट से सम्बन्धित हो अथवा अनोखी हो। विवादास्पद मुद्दों जैसे धर्म या राजनीति का उल्लेख कटापि न र यही आपके लिए अच्छा होगा।
सतत शिक्षा लाइसेंस प्रमाणपत्र/प्रकाशित सामग्री व्यावसायिक सदस्यता आणि उल्लेख उनको सार्थकता और कर्मचारी के रूप में आपकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही करें।।
9. प्रकाशित सामग्री-यदि आप किसी शैक्षणिक पद के लिए आवेदन कर रहे है। आपके पास नियोक्ता को बताने के लिए प्रकाशनों की सूची है तो पहले पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में उनका उल्लेख होना चाहिए। शैक्षणिक पद के लिए शेक्षणिक प्रकाशनों का विशेष से उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर-शैक्षणिक पद के लिए सामान्य जानकारी वाले लेखो। विशेष रूप से उल्लेख करके आप नियोक्ता को यह भी बता सकते हैं कि आप पठनीय तह से लिख सकते हैं और तकनीकी विषयों के बारे में सामान्य लोगों को बताने की क्षमता भी । में निहित है।
10. संदर्भ-यदि अपेक्षित हो तो संदर्भ के लिए माँगे गए व्यक्तियों के नाम और सब देना उचित होगा। ये ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपको भली-भाँति जानते हो और जो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने के स्थान पर उक्त पद के लिए आपकी उपयुक्तता के बारे में समुचित टिप्पणी कर सकें, आपके कॉलेज के प्रोफेसर, आपकी पिछली नौकरी के बॉस जी कि आपको भली-भांति जानते हों या कोई ऐसा जाना-माना व्यक्ति जिसे आपकी योग्यताओ और आपको उपलब्धियों की समुचित जानकारी हो, संदर्भ देने के लिए उपयुक्त है। लेकिन उनका नाम देने से पहले आप उनसे बात कर लें और उनकी सहमति प्राप्त कर लें, बेहतर यहा होगा कि आप अपना जीवनवृत्त-सारांश उन्हें भी दिखा दें और उनसे यह पता कर लें कि क्या वे नाम दे आपको सिफारिश करेंगे।
11. उपयोगी बातें-1) आदर्श जीवनवृत्त-सारांश दो-तीन पृष्ठ से अधिक लम्बा नहीं न दित होता। प्राय: नए लोगों का जीवनवृत्त अनुभवी लोगों के जीवनवृत्त से छोटा ही होता है।
(i) अपने व्यावसायिक जीवन के लक्ष्य का उल्लेख करे। इसमें शैक्षिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण अनुभव और उन कौशलों का उल्लेख करें जो उक्त नौकरी से सम्बन्धित होग हों
(iii) रोजगार के बाजार में अपनी योग्यताओं को भुनाएँ, बिना अतिशयोक्ति के अपन यह कौशल, उपलब्धियों और अपने द्वारा निभाए गए दायित्वों को प्रभावशाली तरीके से बताएं।
(iv) महत्त्वपूर्ण बातों को सर्वप्रथम लिखें फिर अपने व्यावसायिक जीवन के लक्ष्य के योग ध्यान में रखते हुए सूचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखें।
(v) सूचनाओं को उल्टे कालक्रम में लिखें, अर्थात् जो घटना सबसे ताजातरीन घटन.. हो उसे सबसे पहले लिखें और उसी क्रम से पहले घटित घटनाओं का उल्लेख करें।
(vi) प्रभावशाली तरीके से अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कार्य-सूचना क्रियाओं और कार्य-मूलक शैली का उपयोग करें।
(vii) संक्षिप्तता का ध्यान रखें और अनावश्यक विवरण कदापि न दें।
(vii) व्याकरण, वर्तनी और विराम चिह्न आदि का सही-सही व उचित ढंग से उपया। करें।
(ix) कर्मवाच्य की बजाय कर्तृवाच्य में लिखना सर्वदा अच्छा होता है।
(x) शब्दाडम्बर से बचते हुए सर्वदा सरल, सीधी-सादी व सामान्य भाषा का ही ही उपयोग करें।
(i) जीवनवृत्त-सारांश की विषयवस्तु पूर्णतया तथ्यपूर्ण, परिणामोन्मुखी, उचित, सही और ईमानदारी से लिखी गई होनी चाहिए, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व जैसी व्यक्तिनिष्ठ विशेषताओं के बजाय आपको कौशल तथा सत्यापित किए जा सकने वाली उपलब्धियों पर ही अपना ध्यान प केन्द्रित करना चाहिए। का
12. परिलब्धियाँ-आप उक्त नौकरी के लिए कितना वेतन चाहते हैं इसका ब्योरान क देकर आप अपना जरूरत से ज्यादा या बहुत कम मूल्यांकन करने के खतरे से बच सकते हैं। पि अगर इस बारे में विशेष रूप से जानकारी मांगी गई हो तो आप अलग पत्र में इसका उल्लेख कर सकते हैं।
13. पिछली नौकरी छोड़ने का कारण – यह सूचना आपके लिए अत्यन्त विस्फोटक मन हो सकती है, इसलिए साक्षात्कार तक इसे टालने की ही कोशिश करें। र जीवनवृत्त-सारांश तैयार करने के लिए साधारण कागज का उपयोग कदापि न करें, जा सर्वदा अच्छी किस्म के सफेद बॉण्ड पेपर पर इसे बनाएँ। औ
14. प्रस्तुतीकरण-आपका अन्तिम कार्य है-जीवनवृत्त-सारांश का उचित तरीके से न प्रस्तुतीकरण। बेहतर तो यही होगा कि आप इसे किसी वर्ड प्रोसेसर पर तैयार करके लेजर प्रिंटर . ही पर निकालें। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे पेशेवराना तरीके से तैयार किया गया होना चाहिए वे ताकि यह नियोक्ता को साफ-सुथरा और आकर्षक लगे। नियोक्ता को भेजी जाने वाली प्रति अच्छी किस्म के कागज पर छपी होनी चाहिए। सामान्य किस्म के कागज में फोटो कॉपी कदापि ही न भेजें। साफ-सुथरे जीवनवृत्त-सारांश से विशेष रूप से यह प्रभाव पड़ता है कि आप कार्य में
दिलचस्पी लेते हैं और आपके कार्य करने का तरीका इसी तरह का है। जोर भिन्न-भिन्न पदों के लिए जीवनवृत्त-सारांश भी अलग से ही तैयार किया जाए तो बेहतर चत होगा। ऐसा करने से आप उक्त पद से सम्बन्धित अपने कौशल और अनुभव पर विशेष रूप से जोर दे सकते हैं। आप अपना जीवनवृत्त-सारांश इस प्रकार से तैयार करें कि व्यस्त नियोक्ता को तुरन्त ने यह पता चल जाए कि आप उसके संगठन के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
15. संलग्न पत्र-जीवनवृत्त-सारांश के साथ संलग्न पत्र में पद से सम्बन्धित को योग्यताओं और अनुभवों को संक्षिप्त रूप में दिया जाना चाहिए। इसकी भाषा नपी-तुली, संक्षिप्त और गहन सूझ-बूझ वाली होनी चाहिए। ना 16. आवेदन पत्र/प्रारूप-सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी नौकरियों में कनिष्ठ पदों के लिए जीवनवृत्त-सारांश का प्रारूप प्राय: संलग्न रहता है और इसी पर आवेदन क करना आवश्यक होता है। इसे साफ-सुथरे तरीके से सही-सही भरना चाहिए और सन्दर्भ के लिए इसकी एक प्रति अपने पास रख लेनी चाहिए।
प्रश्न – परिपत्र क्या है? वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें परिपत्र की आवश्यकता होती है? परिपत्रों के क्या-क्या उद्देश्य हैं? इनके लाभ भी बताइए।
What is a Circular Letter ? Which are the situations that need rcular letter ? What are the objectives of circular letters ? Mention heir advantages too.
उत्तर – परिपत्र का अर्थ
(Meaning of Circular Letter)
जब किसी व्यापारी को कोई सूचना अनेक ग्राहकों व व्यापारियों के पास भेजनी होती है तो इस आशय से लिखे जाने वाले पत्र को ‘परिपत्र’ या ‘गश्ती पत्र’ कहते हैं। अन्य शब्द कह सकते हैं कि कुछ सूचनाएँ ऐसी भी होती हैं, जो जनसाधारण को देनी होती हैं, लेकिन जनसाधारण को ये सूचनाएँ व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से यथाशीघ्र एक साथ दे पाना सा नहीं होता तथा ऐसा करना अति व्ययपूर्ण भी होता है, अत: जनसाधारण को दी जाने वाली सूचनाएं, जिनकी विषय-सामग्री एक समान होती है, परिपत्रों या गश्ती पत्रों के माध्यम से ही जाती हैं।
परिपत्र वे पत्र होते हैं, जिनके माध्यम से एक ही समाचार सभी को दिया जाता है। परिपत्र सुन्दर शैली व आकर्षक रूप में लिखे जाने चाहिए। ये परिपत्र जितने अधिक प्रभावी होंगे, सूचना का उतना ही अधिक प्रभाव लोगों पर पड़ेगा।
परिपत्र को रुचिकर व प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी रखना आवश्यक है। परिपत्र को प्रभावी बनाने के लिए सुन्दर भाषा-शैली व भिन्न-भिन्न रंगों का प्रयोग किया जा सकता है।
परिपत्र की आवश्यकता की परिस्थितियाँ
(Situations that need Circular Letter)
परिपत्र या गश्ती पत्र की आवश्यकता समय-समय पर उत्पन्न होती रहती है क्योंकि जिस प्रकार बाजार में गश्त लगाने वाला चौकीदार अपने क्षेत्र की सभी दुकानों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके ताले खटखटाता हुआ गश्त लगाता रहता है, उसी प्रकार ‘गश्ती पत्र’ भी सभी नए-पुराने ग्राहकों को खटखटाता हुआ यह सुनिश्चित करता है कि कोई ग्राहक असन्तुष्ट ते नहीं है। जिन परिस्थितियों में गश्ती पत्र लिखे जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं
(1) व्यवसाय का पता या भवन परिवर्तन करने की स्थिति में।
(2) नई दुकान खोलने या नई शाखा खोलने अथवा व्यवसाय का विस्तार करने का स्थिति में
(3) किसी नए उत्पाद के बारे में जनसाधारण को सूचित करने के लिए।
(4) मूल्य में छूट प्रदान करने की सूचना देने के लिए ताकि विक्रय को बढ़ाया जा सके।
(5) नई एजेन्सी प्राप्त होने की सूचना देने हेतु। .
(6) किसी नए साझेदार के प्रवेश करने पर।
(7) फर्म की संरचना में परिवर्तन करने पर।
(8) किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर।
इसके अतिरिक्त एक कम्पनी में भी विभिन्न परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जिनकी सूच।। सभी कर्मचारियों तक पहुँचाना अनिवार्य होता है। इस कार्य के लिए भी परिपत्र का ही प्रया, किया जाता है। ये परिस्थितियाँ अग्रलिखित होती हैं
(1) कम्पनी की किसी नीति में परिवर्तन करने पर।
(2) महँगाई भत्ते की दर में वृद्धि या कमी होने पर।
(3) अवकाश की सूचना देने के लिए।
(4) कम्पनी के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए।
(5) किसी विशेष सुविधा में कटौती करने पर।
(6) कार, स्कूटर या अन्य किसी वाहन को एक निश्चित स्थान पर खड़ा करने के लिए।
परिपत्रों के मुख्य उद्देश्य
(Main Objectives of Circular Letters)
(1) सूचना का प्रचार करने के लिए या अपने भार से मुक्त होने के लिए।
(2) पाठकों को सभी तथ्यों के बारे में बताने के लिए।
(3) पाठकों को फर्म की सूचनाएँ व तथ्यों के सम्बन्ध में सूचित करने के लिए।
(4) प्रचार करने के लिए।
(5) पाठकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए।
परिपत्रों के लाभ
(Advantages of Circular Letters)
(1) परिपत्र भेजने के उपरान्त व्यवसायी अपने कर्त्तव्य से मुक्त हो जाता है।
(2) भविष्य में कोई ग्राहक या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनी के कर्मचारी यह स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें अमुक परिवर्तन या सुविधा या कटौती के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।
(3) परिपत्र व्यवसायी या कम्पनी के लिए भविष्य में सन्दर्भ के रूप में अत्यन्त सहायक सिद्ध होते हैं। .
प्रश्न -ई-कॉमर्स क्या है? इसकी कार्य-पद्धति, प्रकार, लाभ एवं भारत में इसके भविष्य की व्याख्या कीजिए।
What is e-commerce ? Explain its mechanism, types, advantages and its future in India.
उत्तर – ई-कॉमर्स से आशय
(Meaning of e-commerce)
आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना क्रान्ति की तीव्रता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रशासनिक तन्त्र तथा व्यापारी जगत पर इसका प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रौद्योगिकी ने व्यावसायिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियों में दखल देकर अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम ‘ई-कॉमर्स’ के रूप में दिया है।
‘ई-कॉमर्स’ में ‘ई’ से अभिप्राय ‘इलेक्ट्रॉनिक’ और ‘कॉमर्स’ से अभिप्राय ‘व्यापारिक लेन-देन’ से है।
‘ई-कॉमर्स’ के प्रयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी व उन्नत कम्प्यूटर नेटवर्क की सहायता से व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को अत्यन्त कार्यकुशल बनाया है। ‘ई-कॉमर्स ने कागजों पर आधारित पारस्परिक वाणिज्यिक पद्धतियों को अत्यन्त समर्थ व विश्वसनीय संचार माध्यमों से युक्त कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा विस्थापित करने का महत्त्वाकांक्षी प्रयास किया है।
ई-कॉमर्स की कार्य-पद्धति
(Mechanism of e-commerce)
ई-कॉमर्स प्रणाली का मुख्य आधार ‘इलेक्ट्रॉनिक डाटा-इण्टरचेंज’ है, जिसके अन्तर्गत आँकड़ों को परिवर्तित तथा स्थानान्तरित करने की सुविधा होती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत ग्राहक जब वेबसाइट पर उपलब्ध सामान को पसन्द करके क्रय करता है तो उसे भुगतान के लिए कम्प्यूटर पर उपलब्ध एक फार्म भरना होता है। इस फार्म पर वह अपना क्रेडिट कार्ड नं०, देय राशि व पाने वाले व्यक्ति का नाम आदि सूचनाओं को अंकित करता है। इस फार्म के भरते ही व्यक्ति/ग्राहक के खाते में से उचित धनराशि विक्रेता के खाते में स्थानान्तरित हो जाती है। E.D.C. के अन्तर्गत ही वर्तमान समय में एक नई प्रणाली विकसित की गई है. जिसमें क्रेता कम्प्यूटर पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर कर चैक काट सकने में भी सक्षम होता है। इसे ‘नेट चैक’ कहते हैं।
IA ई-कॉमर्स के प्रकार
(UNTypes of e-commerce)
ई-कॉमर्स के तीव्र प्रसार के कारण इसके प्रकारों को अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन प्रचार की तीव्रता के अनुसार इसके निम्नलिखित तीन प्रकारों को अधिक मान्यता प्राप्त हुई है
(1) बी-टू-बी (Business to Business),
(2) सी-टू-बी (Consumer to Business) तथा
(3) आन्तरिक खरीद (Internal Procurement)|
1. बी-टू-बी (Business to Business)-‘बिजनेस-टू-बिजनेस’ ई-कॉमर्स व्यापार की विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से एवं तीव्रता से निष्पादित करने हेतु उचित वातावरण तैयार करने में मदद करने के साथ-साथ खर्चों में भी कटौती हेतु काफी कारगर है। इण्टरनेट के आविष्कार से पूर्व भी इस प्रकार की गतिविधियाँ व्यापारिक जगत में प्रचलित थीं तथापि उनमें आज के जैसे विस्तृत आयामों का अभाव था। इण्टरनेट के आविष्कार के द्वारा व्यापारिक संस्थाओं ने तकनीक के क्षेत्र में उच्चता की अभिप्राप्ति की है तथा कार्य-व्यापार का निष्पादन भी निर्बाध रूप से सुधरा है।2. सी-टू-बी (Consumer to Business)-ई-कॉमर्स का यह प्रकार वेबसाइट व उन पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर ‘क्रेता’ के नजरिए में विभिन्न प्रकार की भुगतान विधियाँ उपलब्ध करा देने में सक्षम होता है। ई-कॉमर्स का यह प्रकार मुख्यत: टेली शॉपिंग, मेल ऑर्डर, टेलीफोन ऑर्डर इत्यादि का विस्तार-मात्र है। इस माध्यम से उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को डण्टरनेट के द्वारा विक्रेता तक पहुंचाता है तथा तदनुरूप विक्रेता कार्यवाही कर क्रेता के अनुगामा
पग उठाता है। इस समस्त प्रक्रिया में इण्टरनेट तथा उससे सम्बन्धित कम्यूटर की विशेष भमिका होती है। इस प्रकार अब यह क्रय विक्रय का सर्वाधिक उपयुक्त मापन होता जा रहा है।
3. आन्तरिक खरीद (Internal Procurement)-अधिकांश कम्पनियां अपने ‘एण्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग’ को वेबसाइट से जोड़कर वाणिज्यिक गतिविधियों का ही है। इन सभी कम्पनियों का प्रमुख उद्देश्य ई कॉमर्स द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सीमाओं से पी आन्तरिक व्यापारिक गतिविधियों को स्वचालित बनाने का है। ये हण्टरनेट पर बिक्री आर्ट। की प्रोसेसिंग/बिल्डिंग/धन का लेन देन व अन्य सम्बन्धित कारोबार अपने खचों में कटौती करने के लिए करती हैं। इण्टरनेट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना के इस अकूत और अनमोल खजाने की चाभी किसी एक आदमी या कम्पनी की मद्रीय कैट नहीं है। इस तक वह हर व्यक्ति पहुँच सकता है, जिसके पास एक कम्यूटर, एक मॉलम और एक टेलीफोन है।
ई-कॉमर्स के लाभ
(Advantages of e-commerce)
ई-कॉमर्स से अनेक लाभ हैं। इन लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला है। व्यवसाय के क्षेत्र सम्बन्धित इसके लाभ दो प्रकार के हो सकते हैं—प्रथम, उपभोक्ताओं को होने वाला लाभ तथा द्वितीय, विक्रय संस्थाओं को होने वाला लाभ। बिन्दुवार इन लाभों को निम्नलिखित क्रम में रखा जा सकता है
(क) उपभोक्ताओ को लाभ (Advantages to consumers)
(1) वांछित वस्तुओं व सेवाओं के चयन में सुविधा।
(2) विल का भुगतान स्वत: ही विक्रेता के पक्ष में हो जाना।
(3) उत्पादों की विशेषताओं व मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन।
(4) बिचौलियों की क्रियाविधि की पूर्णतः परिसमाप्ति।
(5) किसी भी समय वस्तुओं को क्रय करने की सुविधा।
(6) क्रय-विक्रय हेतु बाजार में बारम्बार आवागमन से मुक्ति।
(7) किसी भी वस्तु की खरीद में प्राप्त छूटों की जानकारी का लाभ।
(ख) विक्रेताओं/कम्पनियों को लाभ (Advantages to Vender/Companies)
(1) उत्पादकों, वितरकों तथा व्यापारिक सहयोगियों में व्यापारिक सूचनाओं का आदान-प्रदान व व्यापारिक खर्चों में कटौती।
(2) नए बाजारों व ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी।
(3) दस्तावेजों में समंकों की शुद्धत।।
(4) नए बाजारों की सम्भावनाओं के कारण नए व्यापार की सम्भावनाएँ।
(5) व्यापार चक्र की गतिविधियों में तीव्रता।
(6) कागज की खपत में कमी।
(7) विक्रेताओं के लिए नए उत्पादों की जानकारी तथा आवाजाही की सुविधा।
(8) नए उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करने में सुधार।
(9) समग्र गुणवत्ता के कारण गणितीय त्रुटि का लगभग पूर्ण अभाव।
(10) व्यापारिक आदान-प्रदान के निमित्त विक्रेता को अधिक समय मिलना।
भारत में ‘ई-कॉमर्स’ का भविष्य
(Future of e-commerce in India)
‘ई-कॉमर्स’ ने वाणिज्य एवं व्यापार को एक नए ढंग से करने के लिए वातावरण बनाया है, जिसमें बढ़ोतरी होने की शत-प्रतिशत सम्भावना है। व्यापारिक लेन-देन व व्यापारिक गतिविधियों को कुशलता से सम्पादित करने हेतु उचित वातावरण व तालमेल व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक होगा।
आज भारत ई-कॉमर्स की अधिकांश सुविधाओं से सम्पन्न हो चुका है। इसकी सुचारुता बनी रहे, इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने 2000 ई० में एक ‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित कर दिया है। इस प्रकार के शासकीय अधिनियम अभी कुछ विकसित राष्ट्रों में ही पारित किए जा सके हैं। ई-कॉमर्स पर व्यापार सम्बन्धी अभिलेखों को न्यायालय में भी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो गई है। इन अभिलेखों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करने पर सहज रूप से ही यह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में ई-कॉमर्स का कार्य-क्षेत्र अधिक विस्तार ग्रहण करेगा तथा निश्चित रूप से भारत में इसका भविष्य सुरक्षित तथा उज्ज्वल है।
प्रश्न – प्रतिवेदन क्या है? इसके प्रकार व गुणों का विवरण दीजिए। प्रतिवेदन तैयार करने की विधि को स्पष्ट कीजिए।
What is a Report Give its kinds and characteristics. Explain the procedure of making a report.
उत्तर – प्रतिवेदन से आशय
(Meaning of Report) ___
संचार माध्यमों में आए चहुंमुखी विकास के कारण आज देश-विदेश में कार्यक्रम आदि की तथ्यात्मक जानकारी पाने और भेजने के लिए प्रतिवेदन’ का सहारा लिया जाता है। ‘प्रतिवेदन’ को अंग्रेजी में रिपोर्ट’ या ‘रिपोर्टिंग’ कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है, जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, सरकारी, गैर-सरकारी, सामान्य अथवा विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इसका उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, परिणाम, जाँच या प्रगति की सही-सही तथा पूरी जानकारी देना होता है।
प्रतिवेदन के प्रकार
(Kinds of Reports)
प्रतिवेदन कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए हम इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में रख सकते हैं-
(1) सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन।
(2) संस्था (सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक) आदि का मासिक अथवा वार्षिक तिवेदन।
(3) व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन।
(4) जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन।
एक श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण
(Characteristics of a Perfect Report)
एक श्रेष्ठ प्रतिवेदन में निम्नलिखित गुण होते हैं-
(1) प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए।
(2) प्रतिवेदन की भाषा-शैली तथ्यात्मक होनी चाहिए। इसकी भाषा आलंकारिक और हावरेदार नहीं होनी चाहिए और न ही वाक्य अनेकार्थक शब्दों से युक्त होने चाहिए।
(3) इसकी भाषा निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। प्रथम पुरुष (मैं या हम) का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण
“बैठक में मैंने यह निर्णय लिया कि …….’ के स्थान पर यह लिखना उपयुक्त होगाबैठक में यह निर्णय लिया गया कि ……”
(4) प्रतिवेदन के तथ्य सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए।
(5) प्रतिवेदन में केवल महत्त्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए। प्रतिवेदन में क्षिप्तता का ध्यान बराबर रखना चाहिए। ___
(6) तथ्यों की प्रस्तुति क्रमवार एवं तर्कसंगत रूप में ही की जानी चाहिए, जिससे कि पूरी जानकारी स्पष्ट होती चले।
(7) कभी-कभी प्रतिवेदन में शीर्षक देना अनुकूल रहता है। शीर्षक मुख्य विषय को खांकित करने वाला होना चाहिए।
(8) प्रतिवेदन में प्रत्येक नए तथ्य को अलग अनुच्छेद में देना चाहिए। यदि कोई विषय स्तृत हो तो उसे अनेक अनुच्छेदों में विभक्त करके लिखना चाहिए।
(9) प्रतिवेदन के अन्त में प्रतिवेदन लिखने वाले को अपने हस्ताक्षर करने चाहिए या सके स्थान पर सम्बन्धित सभा, दल या संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।
प्रतिवेदन लिखने की विधि
(Way of Writing a Report)
प्रतिवेदन लिखने से पहले सारे तथ्यों को एकत्र कर लेना चाहिए। निम्नलिखित तथ्य तिवेदन में अवश्य दिए जाने चाहिए
(1) संस्था का नाम।
(2) बैठक/सम्मेलन/सभा का नाम और उद्देश्य।
(3) आयोजन स्थल का नाम।
(4) आयोजन के दिनांक और समय की सूचना।
प्रश्न -प्रतिपुष्टि से क्या आशय है? इसकी प्रक्रिया, विधियाँ बताइए तथा तिपुष्टि को प्रभावशाली बनाने के लिए मार्गदर्शन कीजिए।
What is Feedback ? Explain its process, methods and guidelines To make feedback effeptiye. उत्तर – प्रतिपुष्टि का आशय
Meaning of Feedback)
प्रतिपुष्टि एक प्रत्यार्पित सन्देश होता है, जो सन्देश प्राप्तकर्ता सम्प्रेषक को देता है। जब सम्प्रेषक सूचनाग्राही अथवा प्राप्तकर्ता को सन्देश भेजता है तो सम्प्रेषक उस भेजे गए सन्देश की तिक्रिया चाहता है। सन्देश प्राप्त कर लेने के बाद सन्देश प्राप्तकर्ता द्वारा उस सन्देश को उचित कार से समझा जाता है, तत्पश्चात् सन्देश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। इस प्रतिक्रिया का स्वरूप अनुकूल भी हो सकता है अथवा प्रतिकूल भी हो सकता है। यही प्रतिक्रिया तिपुष्टि कहलाती है। प्रतिपुष्टि सन्देश प्रक्रिया का अन्तिम महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। प्रतिपुष्टि के प्रभाव में कोई भी सम्प्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। प्रतिपुष्टि के आधार पर ही सम्प्रेषक हारा पूर्व सन्देश में परिवर्तन, सुधार अथवा संशोधन कर प्रभावी स्वरूप प्रदान किया जाता है।
प्रतिपुष्टि प्रकिया
(Feedback Process)
क सन्देश प्राप्तकर्ता उचित प्रतिपुष्टि उसी स्थिति में कर सकता है जब वह सम्प्रेषक “रा भेजे गए सन्देश को ठीक से समझे अथवा सुने तथा उस सन्देश को उसी दृष्टिकोण से मझे, जिस दृष्टिकोण से सम्प्रेषक उसे समझाना चाहता है। जब सन्देश प्राप्तकर्ता सन्देश की ई प्रतिक्रिया देता है, तभी सम्प्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि प्रक्रिया की उपस्थिति मानी जाएगी। पुष्टि अग्रांकित चित्र द्वारा समझी जा सकती है–

प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया में जब सम्प्रेषक सन्देश प्राप्तकर्ता को सन्देश भेजता है तो वह सत्रा मौखिक, लिखित, शाब्दिक अथवा अशाब्दिक हो सकता है। सम्प्रेषण प्रक्रिया में सम्प्रेषण । लिए वह बात जाननी आवश्यक है कि जब सम्प्रेषक सन्देश प्राप्तकर्ता को सन्देश भेजता है। सन्देश प्राप्तकर्ता उस सन्देश के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।
लीलेण्ड ब्राउन के अनुसार, “सम्प्रेषण व प्राप्तकर्ता दोनों की प्रभावशीलता के नि प्रतिपुष्टि की एक वांछित मात्रा अत्यन्त आवश्यक होती है।”
प्रतिपुष्टि के प्रभाव
(Effects of Feedback) –
प्रतिपुष्टि के प्रभाव निम्नलिखित हैं
(1) एक सम्प्रेषण प्रक्रिया के अन्तर्गत जिस प्रकार सम्प्रेषक की प्रत्येक क्रिया प्राप्तका की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है, ठीक उसी प्रकार प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रियाएँ भी सम्रा की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं।
(2) एक सम्प्रेषण प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता सम्प्रेषक को अपने द्वारा प्रतिक्रिया के स्वरूप के आधार पर नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता है।
(3) यदि सन्देश प्राप्तकर्ता द्वारा कोई प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो पूर्व भेजे गए स को बदल देते हैं।
(4) एक सम्प्रेषण प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रियाएँ ही प्रा कहलाती हैं, जो सम्प्रेषक को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलता प्रदान करती है।
प्रतिपुष्टि की विधियाँ
(Methods of Feedback)
प्रतिपुष्टि की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित हैं
1. लिखित सम्प्रेषण (Written Communication)-इस विधि में पाठकों के चेहरे के भावों को समझना अथवा पढ़ना असम्भव होता है तथा शीघ्र ही कोई प्रतिक्रिया भी प्राप्त नहीं होती। लिखित सम्प्रेषण सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें सम्प्रेषक जो भी सन्देश भेजना चाहता है वह सरल तथा स्पष्ट होता है एवं उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होता।
2. आमने-सामने सम्प्रेषण (Face to Face Communication)-इस विधि में प्रतिपुष्टि शीघ्र तथा लगातार मिलती रहती है। जब सम्प्रेषक सन्देश प्राप्तकर्ता को कोई सन्देश देता है तो उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है वह तुरन्त ही समझ जाता है। _
3. मौखिक सम्प्रेषण (Oral Communication)—इस विधि में जब सम्प्रेषक सन्देश प्राप्तकर्ता को कोई मौखिक सन्देश देता है और उसकी कोई प्रतिक्रिया जानना चाहता है तो सन्देश प्राप्तकर्ता सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तालियाँ अथवा डेस्क बजा सकता है और नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए उबासी ले सकता है अथवा सन्देश की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है।
प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने हेतु दिशा-निर्देश
(Guidelines to make Feedback Effective)
प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं
(1) प्रतिपुष्टि की प्रकृति वर्णनात्मक होती है।
(2) प्रतिपुष्टि सन्देश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को जानने अथवा समझने में सहायता करती है।
(3) प्रतिपुष्टि किसी आचरण विशेष से सम्बन्धित होनी चाहिए।
(4) प्रतिपुष्टि उचित समय पर होनी आवश्यक है।
(5) प्रतिपुष्टि उसी स्थिति में सम्भव है जब सन्देश प्राप्तकर्ता किसी सन्देश को सुनना अथवा समझना चाहता है।
(6) प्रतिपुष्टि का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से सन्देश के लक्ष्य से होना चाहिए।
(7) प्रतिपुष्टि में विशिष्टता का गुण होना आवश्यक है।
प्रतिपुष्टि का महत्त्व
(Importance of Feedback)
प्रतिपुष्टि का महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट किया जा सकता है
(1) प्रतिपुष्टि के बिना कोई भी प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण असम्भव है।
(2) प्रतिपुष्टि किसी सम्प्रेषण की प्रभावशीलता का मापदण्ड है।
(3) प्रतिपुष्टि सन्देश प्रक्रिया का अन्तिम महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
(4) प्रतिपुष्टि सम्प्रेषण का वास्तविक बोध है।
(5) प्रतिपुष्टि के अभाव में कोई भी सम्प्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ___
(6) प्रतिपुष्टि एक संगठन अथवा व्यवसाय के प्रबन्धन के लिए अत्यन्त होती है।
(7) सम्प्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि एक उत्प्रेरक तत्त्व के रूप में कार्य करती है
(8) उचित प्रतिपुष्टि के द्वारा सम्प्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। __
(9) प्रतिपुष्टि सूचना के आदान-प्रदान और सम्प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य समय पुष्टि करती है।
(10) सम्प्रेषक प्रतिपुष्टि के माध्यम से ही यह जान सकता है कि अभिव्यक्ति उसकी इच्छाओं के अनुरूप है कि नहीं।
(11) प्रतिपुष्टि किसी सन्देश को प्राप्त करने तथा उसकी ठीक व्याख्या को समझने का एक स्रोत है।
प्रश्न – तगादे का पत्र क्या है? एक तगादे का पत्र लिखते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए?
What is Dunning Letter ? What points should be kept in mind while drafting a dunning letter ? अथवा अपने एक ग्राहक के भुगतान हेतु तगादे सम्बन्धी सभी पत्रों (स्मरण पत्रों) को लिखिए।
Write the specimen dunning letters (remindes) to your customer for payment.
उत्तर- ((तगादे के पन्ने का अभिप्राय
(Meaning of Dunning Letter)
यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति नियत समय पर अथवा नियत अवधि के भीतर, खरीदी हुई वस्तु का मूल्य नहीं चुकाता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो पत्र लिखा जाता है उसे ‘तगादे का पत्र’ अथवा ‘रुपया वसूली का पत्र’ कहते हैं। ऐसे पत्र बकाया राशि या अदत्त राशि वसूल करने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों को लिखते समय काफी सावधानी की आवश्यकता होती है; अत: तगादे के पत्र का लेखन पर्याप्त चातुर्य एवं सावधानी से होना चाहिए ताक भूगतान भी प्राप्त हो जाए एवं ग्राहक भी बना रहे। सामान्यतः ऐसे व्यापारिक मामलों में पयास संयम रखा जाना चाहिए। इसमें शीघ्रता की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अत्यधिक शावता करने पर न्यायिक विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से श्रम एवं पैसे की हानि तो होती ही है, साल ही व्यापारिक साख पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
तगादे सम्बन्धी पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें
(Points to be kept in Mind while drafting a Dunning Letter)
लगाटे का पत्र लिखते समय लेखक का मूल ध्येय यह होना चाहिए कि अदत्त रुकी हई राशि भी प्राप्त हो जाए एवं ग्राहक भी बना रहे, अत: इनका लेखन करते समय महत्त्वपर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, वे अग्रलिखित हैं



भाषण का अर्थ
(Meaning of Speech) .
भाषण सम्प्रेषण का शक्तिशाली माध्यम है। व्यावसायिक सम्प्रेषण में भाषण औपना शृंखला के अन्तर्गत आता है। भाषण के अन्तर्गत वक्ता अपनी वाक् शक्ति द्वारा व्यवस्थित में समयोचित दैहिक एवं पार्श्व भाषा के साथ वक्तव्य को सम्प्रेषित करता है, जो श्रोतामे विचारों के साथ बहा ले जाता है। इस वक्तव्य या सम्बोधन को ही भाषण कहा जाता है। में कई ऐसे औपचारिक व अनौपचारिक अवसर आते हैं, जब हमें व्याख्यान या भाषण देता आवश्यकता महसूस होती है। उदाहरण के लिए, उद्घाटन समारोह, संगोष्ठियाँ, कम्पनी ही बैठकें, परिचर्चा इत्यादि ऐसे अवसर होते हैं, जब हम प्रमुख अतिथियों के स्वागतार्थ कल उद्बोधन देते हैं। अनेक अवसरों पर व्याख्यान-माला का विशिष्ट अवदान होता है। व्याख्यान आकार को निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है। यह समय व अवसर के अनुसार छोटा अथवा विस्तृत हो सकता है। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई भाषा सम्बन्धी परिभाषाएँ निम्नलिखित रूप मे हैं।
“Speech is power: Speech is to persuade, to convert, to compel.”
-प्लेटो “भाषण मानव के मस्तिष्क पर शासन करने की एक कला है।”
-सेनेका “भाषण मस्तिष्क का दर्पण है।”
“The ability to speak in a hortative way to distinction, it puts a man in the limelight, raises him head and shoulder above the crowd.”
प्रभावशाली भाषण हेतु आवश्यक तैयारी ।
(Necessary Preparations for an Effective Speech)
एक अच्छे भाषण या व्याख्यान के लिए आवश्यक है कि उसके लिए पूर्व में कुछ तैयारी कर ली जाए। इसके लिए शब्दों की जानकारी, विषय का बोध तथा वाक्चातुर्य का होना भी नितान्त आवश्यक है। एक प्रभावशाली भाषण की तैयारी के लिए निम्नलिखित बिन्दु सहायक सिद्ध हो सकते हैं
(1) Rudyard Kipling के अनुसार हमें व्याख्यान/भाषण को तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए
(i) कौन (Who)-हम किसके लिए भाषण दे रहे हैं, उनकी संख्या क्या है-एक व्यक्ति के लिए या बहुत-से व्यक्तियों के लिए और साथ-ही-साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्रोताओं की रुचि व आशाएँ क्या हैं।
(ii) क्या (What)-हम क्या सम्प्रेषित करना चाहते हैं।
(iii) क्यों (Why)-हमें व्याख्यान/भाषण का उद्देश्य ज्ञात होना चाहिए अथात् हमें क्यों सुनें और हमने उनका चयन क्यों किया है।
(iv) कैसे (How)-हम अपने सन्देश को कितनी अच्छी तरह सम्प्रेषित करें, हम अपने व्याख्यान को या भाषण को प्रभावशाली कैसे बनाएँ।
(v) कहाँ (Where) हमें अपना व्याख्यान कहाँ देना है, क्या चयनित स्थान, श्रोताओं की दृष्टि से उचित है।
(vi) कब (When)-क्या हमने अपने व्याख्यान में समय का ध्यान रखा है, आपका किस समय व कितने समय तक बोलना उचित है।
(2) व्याख्यान के समय यदि उपर्युक्त प्रश्नों का सम्यक् ध्यान रखा जाए तो व्याख्यान निश्चय ही प्रभावोत्पादक होगा। यद्यपि स्पष्टता का गुण प्रत्येक भाषण का प्राण होता है तथापि हमें सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सम्पूर्ण श्रोता शिक्षित है। मुख्यत: व्यावसायिक विश्व में प्रत्येक प्रभावशाली वक्ता “Be dear’ सिद्धान्त का अनुपालन करता है।
(3) व्याख्यान दिए जाने की अवस्था में स्वाभाविक चेष्टाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। सम्भाषण के दौरान कृत्रिमता, व्याख्यान के स्वरूप को कलुषित कर देती है। इस समय भौतिक अवरोधों को अपने अनुगामी बना लेने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए।
(4) स्पष्टता के पश्चात् एक भाषण/व्याख्यान में सरलता का गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एक प्रभावशाली वक्ता जटिल बातों को बड़े ही सरल शब्दों में स्पष्ट कर देता है।
(5) भाषण को सन्दर्भित विषय के अनुगामी होना चाहिए। तथ्यों का उचित समावेश भी अनिवार्य है। व्याख्यान सुस्पष्ट तथा जीवन को आह्लाद प्रदान करने वाला होना चाहिए। ।
(6) एक वक्ता को समस्त सूचनाओं की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह साहित्य, दर्शन आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक, तकनीकी व विज्ञान से सम्बन्धित ही क्यों न हो।
(7) हमें अपने व्याख्यान या भाषण में अशाब्दिक सम्प्रेषण विधि का प्रयोग प्रभावपूर्ण ढंग’ से करना चाहिए क्योंकि शारीरिक भाषा, भाषा प्रतिरूप इत्यादि का प्रभावशाली प्रयोग व्याख्यान को सम्मोहक या रुचिकर बनाता है।
(8) भाषण में तकनीकी शब्दावली का यथासम्भव कम प्रयोग किया जाना चाहिए तथा महत्त्वपूर्ण विषय छूटना नहीं चाहिए। भाषण पर वक्ता का पूर्ण अधिकार होना परम आवश्यक है। वक्ता जो भी कहे, उसे साधिकार कहे, यही प्रभावशाली व्याख्यान का गुण है।
प्रभावशाली भाषण के गुण/लाभ
(Advantages of an Effective Speech)
भाषण कला से वक्ता किसी समूह को प्रेरित करता है। भाषण के द्वारा श्रोताओं को प्रभावित किया जाता है। वक्ता अपने भाषण द्वारा पुरानी नीतियों का समर्थन या निषेध करता है। नवीन का प्रतिपादन या खण्डन करता है। प्रचलित नीतियों पर बल देता है या उन पर प्रहार करता है। किसी नीति या विचार के प्रति श्रोताओं को समर्थन के लिए तैयार करता है या वर्तमान विचारों का खण्डन कर दूसरा मार्ग सुझाता है।1. भोतागण पर स्पष्ट प्रभाव (Good Impression on Audience)प्रभावशाली भाषण की यह विशिष्टता होती है कि वह श्रोतागण को अपने में आत्मसात कर लेता है। श्रोता पूर्ण रूप से सम्भाषणकर्ता के साथ एकाकार हो जाते हैं। श्रोता मन्त्रमुग्ध हो भाषण की विचार-शृंखला के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। सर्वोत्तम भाषण श्रोता को कायल करता है, उसका मत बदल देता है तथा उसे किसी विशेष कार्य करने को बाध्य
करता हैं। शब्दों का मूल्य जानने वाला वक्ता सर्वप्रथम श्रोताओं की मानसिक स्थिति को लता ह, तत्पश्चात् जनसमूह की अवस्था एवं आवश्यकता के अनुरूप व्याख्यान देता है। अच्छ भाषण की विशेषता है कि वह जनसामान्य को अपने निहित विचारों में डबोल” अच्छे भाषण का प्रभाव स्थायी होता है।
2. क्रमबद्धता (Sequence)-क्रमबद्ध विचार-शैली किसी भी भाषण कार विचार, भावना, कल्पना तथा सूचना देने की प्रक्रिया तभी सफल होती है, जब वक्ता का सुव्यवस्थित रूप में विषय का प्रतिपादन करता है। भाषण के दौरान सन्दर्भित वार्ता को ही देना चाहिए। प्रसंगरहित बिन्दुओं का समावेश किया जाना अच्छे भाषण का लक्षण नहीं विषयगत क्रमबद्धता का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए।
3. अभिनेयता (Actions)-भाषण की सफलता के लिए अभिनेयता अनिवार्य हाथ, आँख, भौह, होठ, गर्दन, कन्धे सबकी अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। विषय प्रतिपादन की पापहाव सहजता के साथ अंग संचालन प्रभावकारी होता है। आत्महीनता के भाव को मिटाकर आत्मविश्वास जगाकर ही झिझक को दूर भगाया जा सकता है तथा भाषण कला में विशिष्टतामा प्राप्त की जा सकती है। __
4. सारगर्भिता (Conclusive)-एक सुव्यवस्थित भाषण का यह विशेष गुण होता है कि उसमें सारगर्भिता का लक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कम-से-कम वाक्यों में अपनी बात को सुस्पष्ट कर देना सम्भाषण कला की दक्षता का स्पष्ट सूचक माना गया है। प्रायः विस्तृत भाषणों को श्रोतागण सुनना पसन्द नहीं करते हैं। ऐसे भाषणों पर बोझिल होने का आरोप प्राय: ही लगता रहा है। छोटे तथा सारगर्भित भाषण की उपादेयता को प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार किया जा चुका है।
5. स्पष्टवादिता (Clarity)-किसी भी भाषण में तथ्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। अपने विचारों को निर्भीक ढंग से प्रस्फुटित करना वक्ता का परम धर्म है। कल्पना तथा झूठे तथ्यों का सहारा लेना अच्छे भाषण के गुण नहीं माने जाते हैं। विषय-विशेष पर निर्भीक व स्पष्ट व्याख्यान देना, कुशल व्याख्याता का एक महत्त्वपूर्ण गुण होता है। विचारों का उन्मुक्त प्रस्फुटन ही विचार-शैली की उत्तुंगता का परिचायक है।
प्रश्न – आप एक एजेन्सी प्राप्त करने जा रहे हैं। इस आशय का परिपत्र तैयार र करते समय आप किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगे? उदाहरण सहित समझाइए।
You have to obtain an agency. What points would you keep in your mind while drafting a circular letter for this purpose ? Explain with illustration
उत्तर – परिपत्र तैयार करते समय अत्यन्त सावधानी रखी जानी चाहिए क्योकि इसक माध्यम से व्यावसायिक सूचनाएं जनसाधारण को दी जाती हैं। यदि व्यवसायी परिपत्रों के बारजा भी लापरवाही करता है तो उसे न केवल प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ा। जिसके परिपत्रों का महत्त्व भी समाप्त हो जाएगा। व्यवसाय में विभिन्न परिस्थितिया – विभिन्न प्रकार के परिपत्र जारी करने की आवश्यकता पड़ती है।
एजेन्सी प्राप्त करने के सम्बन्ध में (Regarding Obtaining an Agency)-यदि व्यवसायी को कोई एजेन्सी प्राप्त होती है तो उसकी सूचना वह सभी सम्भावित कों को देना चाहता है, इसके लिए वह प्राय: परिपत्र की सहायता लेता है। यह एजेन्सी किसी वस्त के सम्बन्ध में हो सकती है; जैसे-गैस एजेन्सी, चमड़े की वस्तुओं की एजेन्सी, बन-तेल की एजेन्सी, बीड़ी-सिगरेट की एजेन्सी, कपड़े की एजेन्सी आदि। एजेन्सी प्राप्त ने की सूचना देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—
(1) यदि एजेन्सी प्राप्त करने का कोई महत्त्वपूर्ण कारण हो तो उसका उल्लेख करना हिए; जैसे-वस्तु की माँग बढ़ जाना या शहर में उस प्रकार की कोई एजेन्सी न होना आदि।
(2) ग्राहकों को सूचित कीजिए कि अब हम ग्राहकों के आदेशों को शीघ्रता से पूरा कर कते हैं तथा हमारे पास वस्तुओं की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं।
(3) एजेन्सी के क्षेत्र का उल्लेख करना चाहिए।
(4) माल की किस्म, उपयोगिता, टिकाऊपन, मूल्य, मूल्य पर लगने वाले कर तथा छूट आदि की व्याख्या कीजिए।
(5) यदि आपकी विशेष छूट देने की कोई योजना हो तो उसका उल्लेख कीजिए।
(6) इस प्रकार के स्पष्टीकरण भी देने चाहिए कि ग्राहक अपने आदेश निर्माणकर्ता को त्यक्ष रूप से न देकर केवल एजेन्सी के माध्यम से ही दें।
(7) अन्त में, ग्राहक के सहयोग की अपेक्षा कीजिए तथा उसकी सराहना कीजिए।
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण
वन्दना साड़ी ट्रेडर्स
(बनारसी एवं दाज-वरी की साड़ियों के थोक विक्रेता)
11, बाजार बजाजा, मेरठ
शाखा : शक्ति सिंह मार्केट, चित्तौड़
दिनांक : 13 जनवरी, 2014
सज्जनो एवं बहनो!
हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। आपके शहर के शक्ति सिंह मार्केट में क एजेन्सी खोली जा रही है। इस एजेन्सी पर आपको दाज एवं वरी तथा बनारसी साड़ियों की भरपूर वैरायटी मिलेंगी। यह आपके शहर में एकमात्र एजेन्सी होगी, जो केवल बनारसी साड़ियों का व्यापार करेगी। आपके शहर में बनारसी साड़ियों की माँग को देखते हुए ही यह एजेन्सी बोली जा रही है। अपने ग्राहकों की माँग व पसन्द के अनुसार हम अपने निर्माता से प्रत्यक्ष रूप माल मॅगाते हैं, अत: इस प्रकार की साड़ियाँ आपको न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगी। स एजेन्सी में आपको नए-नए डिजाइनों में साड़ियाँ उपलब्ध होंगी, जो सुन्दर होने के -साथ टिकाऊ भी होंगी। बनारसी साड़ियों के बारे में और अधिक कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस उत्पाद से. सभी भली-भाँति परिचित हैं। बनारसी साड़ियाँ कर्षक, टिकाऊ एवं महिलाओं के मन को लुभाने वाली होती हैं। –
आपके चयन के लिए हम कैटलॉग भेज रहे हैं। आप अपनी इच्छानुसार चयन कर करते हैं। आपका मूल्यवान आदेश हमें सन्तुष्टि प्रदान करेगा। हम आपके आदेश को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ₹ 5,000 से अधिक की साड़ियाँ खरीदेंगे तो हा बट्टा प्रदान करेंगे।
हमें आपके सहयोग की पूर्ण आशा है।
भवदीय
वास्ते वन्दना साड़ी ट्रेड
(भानु प्रताप)
प्रबन्धक
प्रश्न – श्रवणता से आप क्या समझते हैं ? सम्प्रेषण में प्रभावी क्या है? श्रवणता की प्रक्रिया को समझाइए।
What do you mean by Listening ? What is effective listenin communication? Describe the process of Listening.
अथवा श्रवणता से क्या अभिप्राय है? इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए।
What do you mean by Listening ? Describe various types and listening.
उत्तर – श्रवणता से अभिप्राय
(Meaning of Listening)
श्रवणता, इतनी सरल क्रिया नहीं है जितनी कि समझी जाती है। अधिकांश व्यक्ति की। बारे में अक्षम होते हैं। वे सुनने व सोचने के बारे में सावधानी नहीं रखते, अत: वे जितना सन हैं उससे कुछ कम ही याद कर पाते हैं। फ्लोड जे० जेम्स के शब्दों में-“श्रवण-क्षमता की न्यूनता प्रत्येक स्तर पर हमारे कार्य से सम्बन्धित समस्याओं की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है। व्यावसायिक क्षेत्रों में श्रवणता की महत्ता किसी भी रूप में सम्प्रेषण से कम नहीं आँको जन सकती। सुनने अर्थात् श्रवण की क्रिया को ध्यानपूर्वक सुव्यविस्थत ढंग से करने पर उसका प्रतिफल उच्च आयामों को प्राप्त होता है।
वास्तव में, “श्रवणता स्वीकार करने, ध्यान लगाने तथा कानों से सुने गए शब्दों का अप निरूपण करने की एक क्रिया है।”
श्रवणता के प्रकार
(Types of Listening) .
व्यावसायिक क्षेत्र में श्रवणता का महत्त्व अब सुस्थापित हो चुका है। परिस्थितियासअनसार इसके प्रकारों में भी कम या अधिक अन्तर आ जाता है। मुख्य रूप से श्रवणताया विभिन्न प्रकार निम्नलिखित रूप में प्रकट होते हैं
1. एकाग्र श्रवणता (Focus Listening)-इसमें एकाग्रता के तत्त्व काम अपेक्षित रूप से सर्वाधिक होता है। इसकी ग्राह्यता अन्य प्रकारों से कई गना अधिक होती हैं।2. विषयगत श्रवणता (Subjective Listening)-ग्राह्य व्यक्ति में सम्प्रेषित । की जितनी जानकारी होती है, उसी के अनुसार श्रवणता का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। सम्बन्ध व्यक्ति की समझ से होता है।
3. अन्तःप्रज्ञात्मक श्रवणता (Inter Listening)-जब सहज बोधगम्यतावश को ग्रहण किया जाता है, तब इसके समानान्तर अन्य विचार मस्तिष्क में आते रहते हैं। स्थिति सन्देश को सम्पूर्ण अर्थ में समझने में सहायता करती है।
4. समीक्षात्मक श्रवणता (Analytical Listening)-समीक्षात्मक श्रवणता में ही व्यक्ति में तुरन्त ही समीक्षात्मक तत्त्वों का आविर्भाव होने लगता है। इस प्रकार विशिष्ट बिन्दुओं के मूल्यांकन का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है।
5. तदनुभूतिक श्रवणता (Communicating Listening)-इसमें सन्देश को अन्य व्यक्तियों को बताने की सामर्थ्य होती है।
6.सक्रिय श्रवणता (Creative Listening)-इसमें अन्य व्यक्तियों के विचार व -वघटित मानसिक अन्तर्द्वन्द्व समाहित होते हैं।
7. दिखावटी या मिथ्या श्रवणता (Artificial Listening)-इसमें श्रवण की नाह्यता अत्यन्त न्यून होती है। हाव-भाव से तो प्रकट किया जाता है कि ग्राह्यता शत-प्रतिशत है, लेकिन होता इसके विपरीत है। यहाँ सन्देश को सुना तो जाता है, लेकिन ग्रहण नहीं किया जाता।
8. चयनित श्रवणता (Selective Listening)—इसमें श्रवणता के किस हिस्से का वण किया जाना है, इसका निर्धारण स्वयं ग्राही पक्ष करता है और केवल आवश्यक तत्त्व को – ग्रहण करता है।
श्रवण प्रक्रिया
(Listening Process)
श्रवणता एक ऐसी कला है, जिसे प्रक्रियाओं की सीमा में बाँधना अत्यन्त कठिन है फिर इसे निम्नलिखित प्रक्रियाओं में विभक्त किया जा सकता है
1. निर्वचन (Interpreting) 2. अनुभूति (Sensing) 3. मूल्यांकन (Evaluating) 4. अनुक्रिया (Responding) – 5. स्मरण (Remembering) V 1. निर्वचन (Interpreting)-यदि बोलने वाले का सन्दर्भ कुछ अलग है तो हमें
सका विश्लेषण कर यह जानना आवश्यक है कि सोचने वाले की बात का वास्तविक अर्थ या है। इसके लिए हमें उसकी अभाषित गतिविधियों पर ध्यान देना होगा।
2. अनुभूति (Sensing)-श्रवण करते समय सन्देश को लिख लेना चाहिए क्योंकि दिश की प्राप्ति में शोर, दुर्बल श्रवण शक्ति, असावधानी व उपेक्षा बाधा पहुंचाते हैं। इन नरोधों को दूर करके हमें सन्देश को ग्रहण करने पर ध्यान लगाना चाहिए। 3. मूल्यांकन (Evaluating)-इसका अभिप्राय सन्देश के सम्बन्ध में अपने विचार त करने से है। वक्ता द्वारा दिए गए सन्देशों में जो आवश्यक है उस पर विचार करना, जो र अप्रभावी हैं उन्हें पृथक करना। ये सब गतिविधियाँ मूल्यांकन के अन्तर्गत आती हैं।
4. अनुक्रिया (Responding)-वक्ता द्वारा दिए गए सन्देश को ग्रहण क आनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना इसमें सम्मिलित है।
5. स्मरण (Remembering)–इसमें सन्देशों को भविष्य के सन्दर्भ के लिा कर लिया जाता है। वक्ता द्वारा दिए गए मुख्य बिन्दुओं को अनिवार्य रूप से लिव उसको अपने मस्तिष्क में उतारना इसके अन्तर्गत आता है।
व्यावसायिक सम्प्रेषण में प्रभावी श्रवणता
(Effective Listening in Business Communication)
संगठन व व्यवसाय के श्रेष्ठ नीति-निर्धारण में श्रवणता सहायक होती है। प्रभावी श्रवण एक असाधारण कला है। प्रभावी श्रवणता के लाभ व उद्देश्यों को समझना आवश्यक है। प्रभारी श्रवणता के निम्नलिखित उद्देश्य व लाभ होते हैं
(1) अच्छी श्रवणता का रूप बहुआयामी होता है। अच्छी तथा सही श्रवणता , मानवीय कष्टों का सम्यक् निदान प्राप्त किया जाता है। अधोगामी प्रकार के सम्प्रेषण को श्रव के माध्यम से ही ग्राह्य बनाया जाता है।
(2) प्रभावी श्रवणता में सहकार की भावना का स्वतः ही उत्प्रेषण होता है।
(3) श्रवणता संवेदनशील क्षेत्रों, जो विस्फोटक हो सकते हैं, को नियन्त्रित करने में सहायक होती है।
(4) अच्छी श्रवणता अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती है।
(5) प्रभावी श्रवणता अन्य अनेक लोगों के हृदय में सकारात्मक भावनाओं का उन्मेष करती है।
(6) अच्छी श्रवणता अधिकारी तथा कर्मचारी दोनों वर्गों पर सकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करती है, जिस कारण समस्याओं का निदान करने की दिशा में सक्रिय होना सहज हो जाता है।
(7) एकाग्र श्रवणता संगठन के कर्मचारियों में शान्तिपूर्ण वातावरण निर्मित करने में सहायक होती है। धीरज व सहानुभूतिपूर्ण श्रवणता क्रोध व उग्रता को कम करने में सहायक होती है।
(8) उचित रीति से ग्राही श्रवणता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यक्षमता की अभिवान करती है। व्यावसायिक क्षेत्र में यह अधिक मुखर रूप में प्रकट होती है, जिससे उत्पादकता जन अनेक दूरगामी उद्देश्यों की अभिप्राप्ति होती है।
(9) सही श्रवणता अच्छे गुणों से भूषित होती है, जो वास्तविक अर्थ के सम्प्रेषण उचित रीति से ग्रहण करने की सार्थकता को चरितार्थ करती है।
प्रश्न -“आधुनिक युग सूचना-क्रान्ति का युग है।” क्या आप इस कथा सहमत हैं?
ModernAge is the Age of Information Revolution.” Do you as | with this statement ?
अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-
1. फैक्स
2. स्वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग
3, ई-मेल।
Write short note on the following:
1. Fax
2. Video Conferencing
3. e-Mail.
अथवा आधुनिक व्यावसायिक युग में सम्प्रेषण के किन-किन साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इनसे होने वाले लाभों को बताइए।
What forms of communication are being used in the modern world ? Discuss their advantages.
अथवा “आधुनिक सूचना-तन्त्र ने संसार को एक विश्व-गाँव में बदल दिया है।” व्याख्या कीजिए
“Modern Communication System has changed the world into a में World-village.” Discuss.
उत्तर – वर्तमान युग सूचना-क्रान्ति का युग है। बीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में । सम्प्रेषण के नए मशीनी यन्त्रों ने आकार ग्रहण किया। इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में हम देष इसको अधिक मुखरित होते हुए देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक तकनीक ने तो इस विधा को आकाश की ऊँचाइयों का स्पर्श करा दिया है। आज कम्प्यूटर, इण्टरनेट, उपग्रह द्वारा सम्प्रेषण जैसी क्रियाएँ अत्यन्त लोकप्रिय हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मानव ने आशातीत सफलता हो अर्जित की है। फैक्स तथा ई-मेल से सूचना के साधन अधिकाधिक जनसंख्या को सुलभ होते
जा रहे हैं। इक्कीसवीं शताब्दी में जन-संचार ने नए सोपानों का स्पर्श किया है। आधुनिक संचार – में प्रणाली ने सम्प्रेषण को नए रूपाकार में अत्यन्त सुविधाजनक व लाभकारी बना दिया है।
सम्प्रेषण के आधुनिक साधन
(Modern Means of Communication)
इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में सम्प्रेषण के साधन के रूप में विभिन्न यन्त्रों का आविष्कार हो चुका है। सम्प्रेषण के आधुनिक साधन निम्नलिखित हैं
(1) इलेक्ट्रॉनिक, मेल अथवा ई-मेल,
(2) इण्टरनेट,
(3) असेल्युलर फोन्स,
(4.) (पैजर्स,
(5) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग,
(6) फैक्स,
(7) उपग्रह सम्प्रेषण आदि।
सम्प्रेषण के प्रमुख अत्याधुनिक साधनों की विस्तृत विवेचना इस प्रकार है-
फैक्स
(Axor Fasimile)
फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ हस्तलिखित/मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रात को फोटो कॉपी के रूप में भेजा जाता है। इसके द्वारा कुछ ही सेकण्डों में टाइप किए जा हस्तलिखित सन्देश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना सम्भव होता अन्य शब्दों में, फैक्स के द्वारा मूल प्रति की छायाप्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो सकती है।
यह प्रणाली अन्य प्रणालियों की तुलना में त्वरित व सस्ती है। इसका प्रयोग उस स्थिति में अत्यन्त उपयोगी व लाभप्रद होता है, जब प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी काफी अधिक हो।
– फैक्स सेवा एक त्वरित व अत्यन्त सस्ती प्रणाली है। इस फैक्स सेवा के जरिए हम अपने लिखित/मुद्रित दस्तावेजों को फोटोकॉपी रूप में सम्बन्धित व्यक्ति तक अविलम्ब प्रेषित कर सकते हैं। आज फैक्स सेवा दैनिक कार्य-प्रणाली का एक प्रमुख अंग बन गई है, इसका प्रयोग स्वास्थ्य चिकित्सा, व्यापार, कृषि, बैंकिंग, बीमा व शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में अधिकाधिक किया जा रहा है।
2. वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग
(Video Conferencing)
आज भारत का लगभग प्रत्येक जिला वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की सुविधा से सम्पन्न है। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग मौखिक व दृश्यिक सम्प्रेषण की एक उत्तम तकनीक है, अर्थात् विभिन्न स्थानों पर उपस्थित लोग एक वास्तविक बैठक या सभा की तरह ही सम्प्रेषण करते हैं। इस तकनीक द्वारा केवल सन्देश ही सम्प्रेषित नहीं होते, बल्कि सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच सजीव वार्ता भी सम्भव होती है, जिसमें दैहिक भाषा (यथा-हाव-भाव, मुखाभिव्यक्ति, भाव-भंगिमा) का सम्प्रेषण भी होता है।
वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग आमने-सामने (Face-to-Face) दो प्रकार से सम्पन्न होती है
(1) कम्प्यूटर के उपयोग द्वारा एवं (2) बिना कम्प्यूटर के उपयोग द्वारा।
कम्प्यूटर के प्रयोग से सम्पन्न कॉन्फ्रेन्सिंग को ‘कम्प्यूटर कॉन्फ्रेन्सिंग’ भी कहा जाता है। इसमें कम्प्यूटर, वैब कैमरा, टेलीफोन कनेक्शन व इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जबकि बिना कम्प्यूटर के प्रयोग के सम्पन्न कॉन्फ्रेन्सिंग के लिए डिजिटल वैब कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग मशीन, टेलीफोन, सेटेलाइट कनेक्शन व प्रोजेक्टर आवश्यक होता है।
लाभ (Advantages)
(1) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में अलग-अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति लगभग आमने-सामन की तरह ही सम्प्रेषण करते हैं।
(2) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में दृश्य तथा श्रव्य दोनों ही प्रकार के सन्देशों का सम्प्रेषण सम्भव होता है।
(3) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के द्वारा बिना लम्बी यात्रा किए, समय की बचत द्वारा, किसी बैठक/सभा/सम्मेलन में सहभागिता सम्भव होती है।
लिए दोनों व्यक्तियों अर्थात् सम्प्रेषणकर्त्ता व सम्प्रेषणग्राही के पास एक ही ‘Website’ का पता होना आवश्यक है। इण्टरनेट पर g.mail yahoo तथा hotmail प्रमुख वेबसाइट हैं।
2. ई-कॉमर्स (e-Commerce)-व्यावसायिक क्षेत्रों में ई-कॉमर्स का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जाने लगा है। यदि आपके पास इससे सम्बन्धित क्रेडिट कार्ड है तो आप विश्व के किसी भी स्थान से माल का क्रय कर सकते हैं।
3. ई-बैंकिंग (e-Banking)-इसके अन्तर्गत बैंकिंग क्षेत्र से सम्बन्धित क्रिया-कलापों को समाहित किया जाता है। पी० सी० बैंकिंग, टेली-सेविंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी विधाएँ ई-बैंकिंग के अन्तर्गत ही समाहित हैं।
4. वर्ल्डवाइड वेब (World Wide Web)-इण्टरनेट पर लोकप्रियता में ई-मेल के पश्चात् इसी वेब का स्थान है। विश्व में इसकी ख्याति ‘थ्री डब्ल्यू’ www अर्थात् वर्ल्डवाइड वेब) के रूप में हो चुकी है। सूचनाओं का आदान-प्रदान इसके द्वारा बेहतर ढंग से होता है।
5. चैट रूम (Chat Room)-इण्टरनेट के इस माध्यम ने दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया है। इसमें असीमित बातचीत करने के अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति को ‘Web Camera’ के द्वारा अपने कम्प्यूटर की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और वह भी आपको देख्न सकता है।
6. इण्ट्रानेट (Intranet)-इण्ट्रानेट का प्रयोग अत्यन्त सीमित है। सामान्यत: बड़ी कम्पनियाँ इसका प्रयोग अपने मुख्यालय व शाखाओं में परस्पर सम्पर्क बनाने के लिए करती हैं।
7. पुशनेट (Push Net)–इसकी सहायता से सन्देश को इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जाता है, जहाँ इसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
8. यूजनेट (Usenet)-इसकी सहायता से नेटवर्क में समाहित सूचनाओं को किसी विशिष्ट विषय के आधार पर समूहों में बाँटा जा सकता है। इसमें किसी एक विषय में रुचि रखने वाले तमाम व्यक्ति सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। आज यूजनेट अत्यन्त लोकप्रिय है क्योंकि वह एक से अधिक विषयों में बँट सकता है।
9. टेलनेट (Telnet)-इसके द्वारा इण्टरनेट के माध्यम से जुड़े विश्व के किसी भी कम्प्यूटर पर ‘Log in’ करके उस पर इस प्रकार कार्य कर सकते हैं जैसे कि वह कम्प्यूटर आपके नियन्त्रण में हो। इसे ‘दूरस्थ लॉग इन’ कहा जाता है। इसमें एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर पर आवश्यक नई एवं उपयोगी सूचनाओं को उतारा अर्थात् ‘Download’ किया जाता है।
10. सर्च इंजन (Search Engine)-सर्च इंजन के रूप में ‘Google’ की ख्याति चरम सीमा पर है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप वेबसाइट का . सुगमतापूर्वक पता लगा सकता है। सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित हर तरह की जानकारी इसके द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाती है।
इण्टरनेट के प्रयोग से उत्पन्न समस्याएँ
(Problems created due to Use of Internet)
इण्टरनेट वर्तमान में बहुत लोकप्रिय है, परन्तु इसके प्रयोग से कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं जो अग्रलिखित हैं
(1) साइबर अपराधियों द्वारा कम्प्यूटरों में वाइरस प्रवाहित कर उनकी कार्यप्रणाली को पंगु बना दिया जाता है, जो कम्प्यूटर की क्षमता को अवरोधित कर देते हैं।
(2) अश्लीलता विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। इण्टरनेट के द्वारा इस अश्लीलता कर प्रदशन काफी आसान हो गया है। इस समस्या का अभी तक कोई उचित निदान नहीं हो पायाॉ
(3) बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों में भी इण्टरनेट प्रणाली समस्याग्रस्त हो चुकी है। इसमें आपका पासवर्ड चुराकर आपके आँकड़ों व फाइलों का दुरुपयोग हो सकता है।
(4) इण्टरनेट पर असीमित ज्ञान व जानकारियाँ उपलब्ध हैं। लेकिन तकनीक के कल पायदान आज भी पिछड़े हुए तथा अविकसित अवस्था में हैं। इण्टरनेट की सूचनाओं के आदान-प्रदान का मार्ग अत्यन्त व्यस्त व संघनित होता है। केबिल, जो सूचना के प्रेषण का मार्ग प्रदान करता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं आया है। अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है।
5. सेल्युलर फोन्स
(Cellular Phones)
‘सेल्युलर’ शब्द अंग्रेजी के ‘सेल’ शब्द से बना है। ‘सेल’ (cell) का अर्थ है ‘कोशिका’। इन्हीं सेल या कोशिकाओं के माध्यम से सेल्युलर फोन्स कार्य करते हैं। इसे मोबाइल फोन (Mobile Phone) भी कहा जाता है क्योंकि यह एक छोटा-सा यन्त्र है, जिसे जेब में रखकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। 4 सेल्युलर फोन पद्धति मुख्यतः मौखिक सम्प्रेषण का एक प्रारूप है। इसका प्रयोग बड़ी आसानी से वाहनों में व देश के किसी भी हिस्से में, जहाँ इस संचार प्रणाली की सुविधा है, आसानी से किया जा सकता है। यह ‘समय-प्रबन्धन’ (Time Management) का एक प्रमुख यन्त्र है क्योंकि इसके माध्यम से एक व्यवसायी अपने कीमती समय को अधिक उत्पादक बना सकता है। जब संचार की सामान्य सम्प्रेषण प्रणालियाँ खराब हो जाती हैं, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा (बाढ़, भूकम्प के समय) की स्थिति में होती हैं, तो सेल्युलर फोन पद्धति एक वरदान के रूप में कार्य करती है।
सेल्युलर फोन के लाभ
(Advantages of Cellular Phone)
(1) सेल्युलर फोन प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, जब भूकम्प या बाढ के कारण हमारी तारों पर आधारित सामान्य संचार प्रणाली खराब हो जाती है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है।
(2) सेल्युलर फोन का प्रयोग यात्रा करते समय वाहन में या सुदर क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है।
(3) सेल्युलर फोन ‘समय-प्रबन्धन’ हेतु महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा समय-प्रबन्धन कर अपनी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
सेल्युलर फोन से हानियाँ/सीमाएँ
(Disadvantages/Limitations of Cellular Phones)
(1) सेल्युलर फोन के नम्बर अत्यधिक लम्बे होते हैं, विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेल्युलर फोन का नम्बर कम से कम 10 अंकों का होता है, अत: इन्हें या असुविधा महसूस होती है।
(2) सेल्युलर फोन पर सम्प्रेषक व सम्प्रेषणग्राही दोनों को ही शुल्क देना होता है। इस कारण यह एक महँगा यन्त्र है। यद्यपि अब इस दिशा में कुछ नए परिवर्तन किए जा रहे हैं।
(3) सेल्युलर फोन का गलत प्रयोग (विशेष तौर पर वाहन चलाते समय) किसी बड़ी दर्घटना या अन्य असुविधाओं को जन्म देता है।
(4) सेल्युलर फोन अत्यन्त छोटा होता है, अत: इसके खो जाने का भय सदैव बना रहता है।
प्रश्न – निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
(I) सामीप्य भाषा
(II) भाषा प्रतिरूप,
(II) संकेत भाषा या दृश्य-श्रव्य उपकरण।
Write short note on the following:
(I) Proximics
(II) Para Language
(III) Sign Language or Audio-visual Instruments.
उत्तर – (I) सामीप्य भाषा
(Proximics)
सामीप्य भाषा में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति अपने आस-पास की विषय-वस्तु व स्थान के अन्तर को किस प्रकार व्यवस्थित कर सम्प्रेषण क्रिया सम्पन्न करता है। अन्य शब्दों में, सामीप्य भाषा (Proximics) के अन्तर्गत हम अपने आस-पास के स्थान, जगह, दूरी, अन्तर व आस-पास की विषय-वस्तु के माध्यम से किस प्रकार सम्प्रेषण प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं—समाहित होता है। यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो यह पाएँगे या इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारे आस-पास की स्थिति, जगह, दूरी, अन्तर व आस-पास की विषय-वस्तु सम्प्रेषण क्रिया करती हैं। यह हमारे मस्तिष्क या अन्य के मस्तिष्क में अपने एक अर्थ को स्पष्ट करती है।
सामीप्य भाषा के प्रकार (Types of Proximics)
सामीप्य भाषा को व्यक्तिगत अन्तर भाषा (Personal Space Language), समय भाषा (Time Language) व परिवेश (Surrounding) के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात् सामीप्य भाषा के निम्नलिखित तीन प्रारूप या प्रकार होते हैं
(1) अन्तर (स्थान, दूरी, जगह) भाषा (Space Language)
(2) समय भाषा (Time Language)
(3) परिवेश, वातावरण, माहौल (Surrounding)।
1. स्थान अन्तर भाषा (Space Language)-एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से दूरी उनके मध्य सम्बन्ध व सम्प्रेषण की प्रकृति को स्पष्ट करती है। एडवर्ड टी० हॉल ने इस क्षेत्र में अत्यन्त ही रुचिकर एवं उपयोगी कार्य किया है। एक व्यक्ति अपने को स्थान के केन्द्र में स्थित कर अपने आस-पास के क्षेत्र, स्थान, जगह को एक प्रकार के संकेन्द्रित चक्रीय रूप में पाता है।
अन्तर भाषा निम्नलिखित दो रूपों में सम्प्रेषित की जाती है-
(i) सामीप्यता (Proximity)
(ii) उन्मुखीकरण (Orientation)।
सामीप्यता में सम्प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य एक विश्रामग्रह में लगभग 5.5 फट र दूरी होती है, जबकि उन्मुखीकरण व्यक्तियों के बैठने व खड़े रहने की स्थिति को दर्शाता है। व्यक्तियों का आमने-सामने बैठना. बाज में बैठना आदि ये स्थितियाँ व्यक्तियों के मध्य सम्ब को स्पष्ट करती हैं जैसे सहयोगी व्यक्ति सदैव टेबिल के सामने या बाजू में बैठता है, अर्थात व्यक्ति एक-दूसरे के बीच दूरी के आधार पर विभिन्न चार प्रकार की अन्तर भाषाओं का निर्माण करता है-
(i) प्रगाढ़ अन्तर भाषा (Intimate Space Language)
(ii) व्यक्तिगत अन्तर भाषा (Personal Space Language)
(iii) सामाजिक अन्तर भाषा (Social Space Language) (iv) सार्वजनिक अन्तर भाषा (Public Space Language)।
(i) प्रगाढ़ अन्तर भाषा में सम्प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच लगभग 18 इंच की दूरी होती है, अर्थात् व्यक्ति (सम्प्रेषक) की समस्त शारीरिक गतिविधियाँ 18 इंच के घेरे में सम्पन्न की जाएँगी। भाषा का यह प्रकार, शारीरिक स्पर्श की सम्भावना को व्यक्त करता है। सामान्यतः इस घेरे में परिवार के सदस्य, नजदीकी दोस्त व विशिष्ट व्यक्ति ही आते हैं।
(ii) व्यक्तिगत अन्तर भाषा में सम्प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच लगभग 18 इंच से 4 फुट की दूरी होती है। सम्प्रेषण के इस घेरे में सामान्यत: स्वैच्छिक/स्वाभाविक एवं अनियोजित सम्प्रेषण तथा मित्रवत् वार्तालाप सम्मिलित होते हैं।
(iii) सामाजिक अन्तर भाषा में सम्प्रेषक व प्राप्तकर्ता में 4 फुट से 12 फुट तक का अन्तर होता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रायः औपचारिक उद्देश्य के लिए होता है। यह राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करता है। इसका प्रयोग प्राय: व्यावसायिक वार्तालापों में होता है।
(iv) सार्वजनिक अन्तर भाषा में सम्प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच 12 फुट से अधिक दूरी होती है। यह दूरी सम्प्रेषक/ग्राही के देखने व सुनने की सीमा में होती है। यह सम्प्रेषण की औपचारिकता को व्यक्त करती है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः तेज आवाज के रूप में होता है।
2.समय भाषा (Time Language)-समय मानव जीवन के व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन की महत्त्वपूर्ण विषय-वस्तु, समयबद्धता, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं प्रचलित संस्कृति पर निर्भर है। समय-पालन व्यक्ति का सापेक्ष गुण है। भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति के व्यक्तियों की समय के प्रति गम्भीरता अलग-अलग होती है। भारतीय परिवेश के संगठन चाहे वे व्यावसायिक हों, सरकारी हों या अशासकीय हों समय का प्रयोग कैलेण्डर व घड़ी के माध्यम से करते हैं। व्यावसायिक समुदाय में हमेशा एक कथन का प्रयोग किया जाता हैTime is Money.” यह समय की महत्ता व उपयोगिता को दर्शाता या स्पष्ट करता है।
3. परिवेश (Surrounding)-परिवेश से अभिप्राय आसपास के भौतिक वातावरण से है। यह स्वयं अपनी भाषा संजोता है, अर्थात् इसकी अपनी एक भाषा होती है। परिवेश के कई संघटक होते हैं। यहा हम दो प्रकार के संघटकों का वर्णन कर
(a) रंग (Colour) एवं
(b) रूपरेखा व रूपाकन/आभकल्पना (Layout and Designing)
रंग मानवीय भावनाओ, इन्द्रियों तथा सोचनक यि भावनाओ, इन्द्रियों तथा सोचने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। प्रिय रगा से न केवल सजावट बढ़ती है बल्कि ये मनुष्य के मनोविज्ञान पर
र बढ़ता है बल्कि ये मनष्य के मनोविज्ञान पर भी प्रभाव डालते हैं। अमेरिका म मातम के समय काले वस्त्र धारण किए जाते हैं तथा नववध सफेद रंग के वस्त्र धारण
भी करते हैं। गग सावभामिक रूप में सफेद रंग शान्ति का प्रतीक है। इसे हम रंगों की भाषा कहते हा रंग औपचारिक सम्प्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
रूपरेखा व रूपांकन स्वयं एक महत्त्वपर्ण व्यवसाय है। इसका उद्देश्य द्रव्य को प्रदशित करना होता है। स्थान की अधिकता वक्ता की आवाज को बढ़ाती है। स्थान की कमी स्वर का नीचा होना दर्शाती है तथा शारीरिक भाषा की सरलता स्थान को सरलतापूर्वक मौखिक सम्प्रेषण से जोड़ती है।
निकषतः स्थान अन्तर, जगह, समय और भौतिक वातावरण सभी अभाषिक सम्प्रेषण के मुख्य तत्त्व हैं। समय व अन्तर/स्थान की उपलब्धता मौखिक सम्प्रेषण की पूरक होती है। इसी प्रकार से ‘समय भाषा’ या एक सम्प्रेषक द्वारा समय को दिया गया महत्त्व अभाषित सम्प्रेषण को उपयुक्त व अर्थपूर्ण बनाता है। रूपरेखा व रूपांकन तथा रंग वर्तमान फैशन की दिशा का स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं।
भाषा प्रतिरूप
Para Language)
‘Para Language’ में ‘Para’ शब्द का आशय ‘समान’ (Like) तथा ‘Language’ शब्द का आशय ‘भाषा’ से है। दोनों के संयुक्त अर्थ को हिन्दी में ‘पार्श्व भाषा’ कहते हैं। मौखिक सम्प्रेषण में वक्ता का यदि गहन अवलोकन करें तो पता चलता है कि वह अपने सम्प्रेषण में अनेक संकेतों, स्वर का उतार-चढ़ाव, धाराप्रवाह अथवा अप्रवाह, जगह-जगह वाणी को अल्प विराम, ऊँची अथवा धीमी आवाज जाने-अनजाने में प्रयोग करता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को ही मिश्रित रूप में ‘पार्श्व भाषा’ कहा जाता है।
‘Para Language’ अभाषित सम्प्रेषण का ही एक प्रकार है, परन्तु अन्य अभाषित सम्प्रेषणों (Non-verbal Communications) की अपेक्षा यह शब्द-संकेतों के अत्यन्त निकट है क्योंकि इसमें एक वक्ता अपने शब्दों को किस प्रकार ‘स्वर-ध्वनि’ के साथ कैसे उद्घोषित करता है, इस बात का इशारा या संकेत प्राप्त होता है। आवाज या स्वरों में यह गुण या विशेषता होनी चाहिए कि उनके स्वराघात, लय, गति व मात्रा अथवा आयाम के द्वारा सन्देश के अर्थ को समझा जा सके जैसे उच्च स्वराघात/लय वाली आवाज स्नेह, प्रेम, अनुराग, लगाव, चाह की परिचायक है।
भाषा प्रतिरूप के मुख्य तत्त्व
(Main Factors of Para Language).
भाषा प्रतिरूप के निम्नलिखित मुख्य तत्त्व हैं11. अन्तराल या विराम (Pause)-किसी भी वक्तव्य या सन्देश को बिना अन्तराल या विराम के सम्प्रेषित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी होगी कि अन्तराल या विराम सही समय पर होना चाहिए। अन्तराल का गलत प्रयोग सन्देश को बदल देता है।
पूर्ण हो जाती हैं। एक श्रोता एवं वक्ता के व्यवसाय, भौतिक बोधगम्यता, आयु, व्यक्तित्व का भी प्रभाव सम्पूर्ण सम्प्रेषण प्रक्रिया पर पड़ता है।
भाषा प्रतिरूप के लाभ
(Advantages of Para Language)
(1) भाषा प्रतिरूप के द्वारा किसी व्यक्ति की किसी व्यवसाय या संगठन में स्थिति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है।
(2) भाषा प्रतिरूप किसी समय-विशेष के शैक्षणिक परिवेश को स्पष्ट करता है।
(3) भाषा प्रतिरूप का उपभोग शैक्षिक मूल्य है। एक सतर्क/सचेत श्रोता एक कुशल वक्ता से बहुत कुछ सीखता है।
(4) भाषा प्रतिरूप किसी वक्ता की मानसिक दशा को स्पष्ट करने में सहायक है। उसकी स्वर-गणवत्ता. बोलने की गति एक श्रोता के सन्देश ग्रहण करने में सहायक हाता है।
(5) भाषा प्रतिरूप, भाषा से संलग्न है, अतः कोई भी मौखिक सन्देश बिना इसके पर्ण नहीं होता
भाषा प्रतिरूप की सीमाएँ
(Limitations of Para Language)
(1) चूँकि वक्ता विभिन्न समुदायों के होते हैं, अत: मौखिक सम्प्रेषण प्रक्रिया में सन्देश की एकरूपता समाप्त हो जाती है।
(2) वक्ता की स्वर-गुणवत्ता व पिच, प्राप्तकर्ता या श्रोता को भ्रमित करती है क्योंकि सदैव इस पर ध्यान रखना श्रोता के लिए कठिन व जटिल होता है। इस कारण से भाषा प्रतिरूप कभी-कभी श्रोता को भ्रमित करता है।
(3) भाषा प्रतिरूप एक भाषा के समान है, परन्तु भाषा नहीं है। यह सम्प्रेषण का एक अशाब्दिक/अभाव्येतर अंश है। इस पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता है।
संकेत भाषा या दृश्य-श्रव्य उपकरण
(Sign Language or Audio-visual Instruments)
सम्प्रेषण प्रक्रिया में सन्देश को प्रेषित व ग्रहण करने के लिए सम्प्रेषक व प्राप्तकर्ता पारस्परिक रूप से कुछ संकेतों, चिह्नों, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। भाषा स्वयं चिह्नों, संकेतों, प्रतीकों का एक क्रमबद्ध समूह है। प्राचीनकाल से मनुष्य अपनी अनुभूतियों, विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेतों, प्रतीकों का प्रयोग करता आया है। इन चिह्नों प्रतीकों का प्रयोग कम-सेकम दो व्यक्तियों या समूहों के लिए, विशेषकर आदिम जातियों के बीच होता रहा है।
ये चिह्न, संकेत, प्रतीक मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं
1. चाक्षुष संकेत एवं
2. ध्वनि संकेत।1. चाक्षुष संकेत (Visual Sign)-इस श्रेणी में ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें देखकर सूचना प्राप्त की जाती है। इन संकेतों के माध्यम से या चेहरे के बदलते भावों से सन्देश ग्रहण किया जाता है जैसे जलती हुई सिगरेट पर क्रॉस का चिह्न इस बात का संकेत है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। विद्युत प्रदाय स्थानों पर लाल रंग से Danger लिखा का अर्थ है कि उस स्थान के समीप नहीं जाना चाहिए। इसमें बोलना, हस्ताक्षर कर हा लिखना आवश्यक नहीं होता है। केवल दृश्य-प्रदर्शन से ही सम्प्रेषण हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी पुस्तक (यथा–भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र या इतिहास विषय) में मानचित चित्र मात्र एक विशेष वर्ग तक के लिए सीमित होते हैं। परन्तु ऐसे बहुत-से चाक्षष संकेत प्रतीक हैं, जो सार्वभौमिक होते हैं और इन्हें सभी वर्ग के व्यक्ति समझ सकते हैं, अर्थात संकेत भाषा सार्वभौमिक होती है; जैसे-लाल व हरे रंग का प्रकाश (Light) ट्रैफिक, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर तथा लाल रंग का बल्ब ऑपरेशन थियेटर के बाहर इत्यादि सार्वभौमिक संकेत/प्रतीक हैं। एम्बुलेन्स व वी०आई०पी० गाड़ियाँ बगैर शब्दों के केवल चाक्षुष संकेत से ही अत्यन्त प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्य को सम्प्रेषित करती हैं।
विभिन्न प्रकार के रंगों की सहायता से व्यक्तियों के स्वभाव को इंगित किया जाता है.

लाल और पीला रंग अत्यधिक ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि लाल रंग आक्रमणशीलता व पीला रंग स्पष्टता या दृश्यता का प्रतीक है।
इसी प्रकार झण्डे का रंग, चाहे वह सफेद हो या काला एवं फूलों के रंग भी सम्प्रेषक की अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं।2. ध्वनि संकेत (Audio/Sound Signals)-प्राचीनकाल में जो मनुष्य जंगलों में रहते थे, वे विभिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों; यथा-ढोल की विभिन्न प्रकार की आवाजों (Drumbeats) का प्रयोग करते थे। आज भी जब शिकार के लिए जंगल में प्रवेश किया जाता है तो ढोल की थाप (Drumbeating) के द्वारा ध्वनि संकेत के रूप में सन्देश प्रेषित किया जाता है। आज भी विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए ढोलक का विभिन्न प्रकार का आवाजो के माध्यम से सम्प्रेषण किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है।
कि ध्वनि संकेत आज भी हमारी प्राचीन सभ्यता से ही चाक्षष संकेतों के साथ-साथ प्रयुक्त किए जाते हैं और व्यावसायिक क्षेत्र ने इन्हें बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया है।
वर्तमान समय में विभिन्न कार्यालयों में अलार्म संकेतों का प्रयोग किया जाता है; जैसेFire Alarms, Accident/Casualty Alarms इत्यादि। इसके लिए विभिन्न प्रकार क सायरन, सीटियों, हूटर्स (भोपुओं) का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रोता को सावधान करना व सही स्थिति में लाना होता है। घड़ी का अलार्म समय के प्रति व अपनी प्रोग्राम सूची के प्रति सचेत करता है।
आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दफ्तर बर्जर, प्रेस बटन, घण्टी, विद्युत घण्टी के बगैर अपूर्ण है क्योकि इनके संकेत इनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके कार्य के प्रति सचेत करते हैं।
संकेत भाषा के लाभ (Advantages of Sign Language)
(1) रंगीन पेण्टिग्स, फोटोग्राफ्स, पोस्टर इत्यादि सम्प्रेषण को रुचिकर बनाते हैं और सम्प्रेषणग्राही को प्रेरित करते हैं।
(2) ये सम्प्रेषक की मानसिक स्थिति, बुद्धिमत्ता स्तर, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रतिबिम्बित करते हैं।
(3) चाक्षुष संकेत; यथा—चित्र, पोस्टर, फोटोग्राफ इत्यादि शाब्दिक सम्प्रेषण से बचाते हैं क्योंकि इनके द्वारा अनेक शब्दों को चाक्षुष रूप में सम्प्रेषित किया जाता है।
(4) पोस्टर विज्ञापन का एक प्रभावी माध्यम है। ये लोगों का ध्यान तुरन्त अपनी ओर आकर्षित करता है।
(5) ‘समय प्रबन्धन’ के लिए ध्वनि संकेत अत्यन्त उपयोगी हैं। समय संकेतों के आधार पर एक दिन की योजना का निर्माण किया जाता है।
(6) ध्वनि संकेत विभिन्न सन्देशों को तीव्रतापूर्वक सम्प्रेषित करते हैं; जैसे—घण्टी या सायरन का बजना कर्मचारियों को उनके कार्यों के प्रति सचेत करता है।
संकेत भाषा की सीमाएँ (Limitations of Sign Language)
(1) सदैव प्रभावशाली चित्र या पोस्टर बनाना आसान नहीं होता। यह कलाकार की कशलता पर निर्भर करता है कि उसने सम्बन्धित धारणा या विचार को सही रूप से समझ लिया है या नहीं, तभी वह उसका प्रभावशाली चित्रांकन कर सकता है।
(2) संकेत भाषा में चाक्षुष या ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा केवल सरल व प्रारम्भिक अनिवार्य सूचनाओं को सम्प्रेषित करना ही सम्भव होता है। यदि सन्देश या विचारों में कोई जटिलता है तो पोस्टर या चित्रों के माध्यम से इसका सम्प्रेषण अत्यन्त कठिन होता है।
(3) संकेत भाषा सन्देश प्राप्तकर्ता की समझ पर निर्भर करती है, अत: संकेत को सही रूप में न समझने पर वह भ्रमित भी हो सकता है।
(4) संकेत भाषा को दुहराना या उसमें तुरन्त सुधार सम्भव नहीं होता, जबकि शाब्दिक सम्प्रेषण में तात्कालिक सुधार अत्यन्त ही आसान होता है।
(5) संकेत भाषा शाब्दिक सम्प्रेषण के साथ अत्यधिक प्रभावशाली हो जाती है। .
Follow Me
B.Com Ist Year Foreign Trade And Economic Growth Question Answer Notes
[PDF] B.Com 1st Year All Subject Notes Study Material PDF Download In English
B.Com 2nd Year Books Notes & PDF Download For Free English To Hindi
B.Com 1st Year Notes Books & PDF Free Download Hindi To English
B.Com 1st 2nd 3rd Year Notes Books English To Hindi Download Free PDF
B.Com Ist Year Unemployment Short Study Notes Question Answer

Leave a Reply